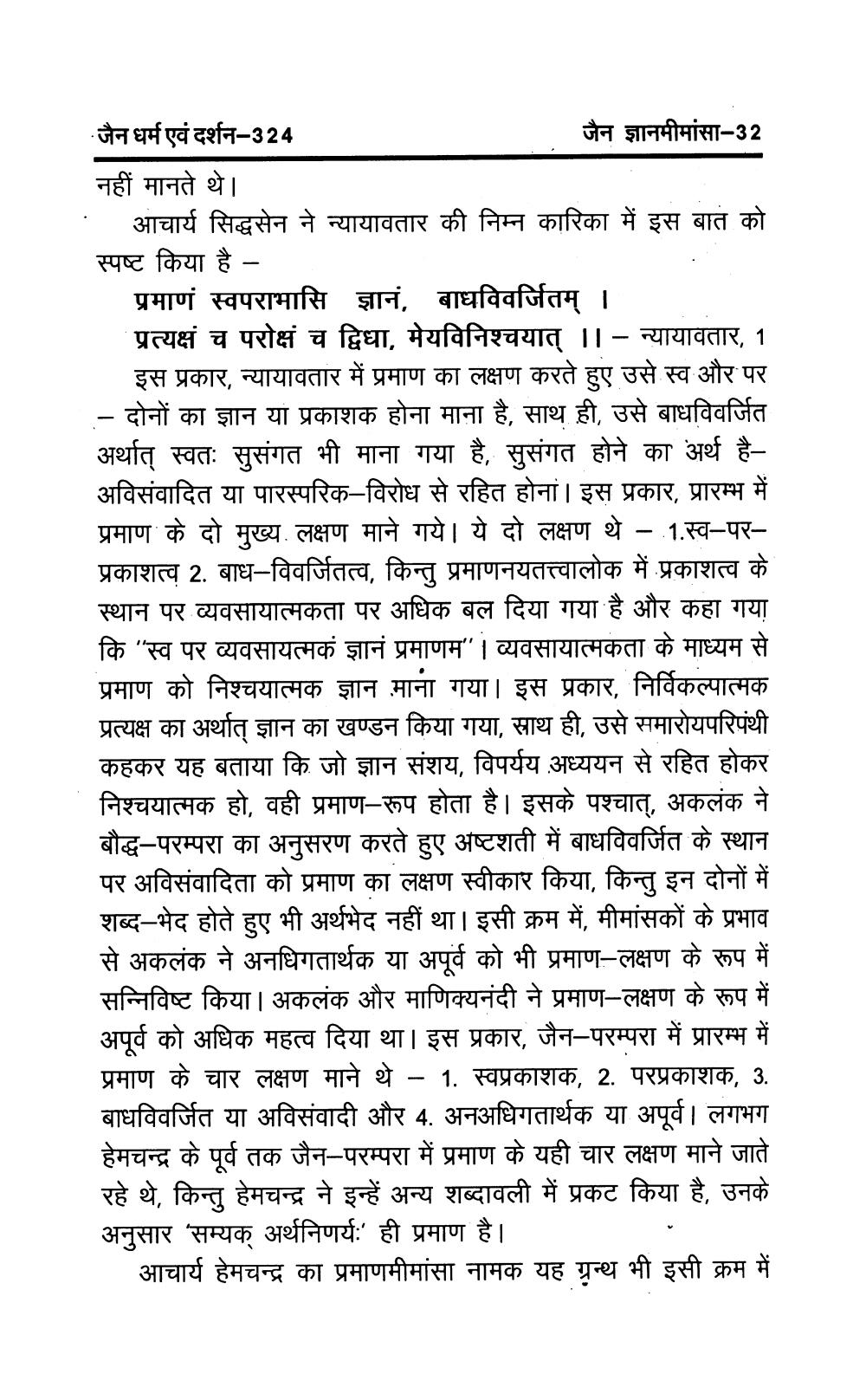________________ जैन धर्म एवं दर्शन-324 जैन ज्ञानमीमांसा-32 नहीं मानते थे। - आचार्य सिद्धसेन ने न्यायावतार की निम्न कारिका में इस बात को स्पष्ट किया है - प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं, बाधविवर्जितम् / प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्विधा, मेयविनिश्चयात् || - न्यायावतार, 1 इस प्रकार, न्यायावतार में प्रमाण का लक्षण करते हुए उसे स्व और पर - दोनों का ज्ञान या प्रकाशक होना माना है, साथ ही, उसे बाधविवर्जित अर्थात् स्वतः सुसंगत भी माना गया है, सुसंगत होने का अर्थ हैअविसंवादित या पारस्परिक-विरोध से रहित होनां / इस प्रकार, प्रारम्भ में प्रमाण के दो मुख्य लक्षण माने गये। ये दो लक्षण थे - 1.स्व-परप्रकाशत्व 2. बाध-विवर्जितत्व, किन्तु प्रमाणनयतत्त्वालोक में प्रकाशत्व के स्थान पर व्यवसायात्मकता पर अधिक बल दिया गया है और कहा गया कि "स्व पर व्यवसायत्मकं ज्ञानं प्रमाणम" | व्यवसायात्मकता के माध्यम से प्रमाण को निश्चयात्मक ज्ञान माना गया। इस प्रकार, निर्विकल्पात्मक प्रत्यक्ष का अर्थात् ज्ञान का खण्डन किया गया, साथ ही, उसे समारोयपरिपंथी कहकर यह बताया कि जो ज्ञान संशय, विपर्यय अध्ययन से रहित होकर निश्चयात्मक हो, वही प्रमाण-रूप होता है। इसके पश्चात्, अकलंक ने बौद्ध-परम्परा का अनुसरण करते हुए अष्टशती में बाधविवर्जित के स्थान पर अविसंवादिता को प्रमाण का लक्षण स्वीकार किया, किन्तु इन दोनों में शब्द-भेद होते हुए भी अर्थभेद नहीं था। इसी क्रम में, मीमांसकों के प्रभाव से अकलंक ने अनधिगतार्थक या अपूर्व को भी प्रमाण-लक्षण के रूप में सन्निविष्ट किया। अकलंक और माणिक्यनंदी ने प्रमाण-लक्षण के रूप में अपूर्व को अधिक महत्व दिया था। इस प्रकार, जैन-परम्परा में प्रारम्भ में प्रमाण के चार लक्षण माने थे - 1. स्वप्रकाशक, 2. परप्रकाशक, 3. बाधविवर्जित या अविसंवादी और 4. अनअधिगतार्थक या अपूर्व / लगभग हेमचन्द्र के पूर्व तक जैन-परम्परा में प्रमाण के यही चार लक्षण माने जाते रहे थे, किन्तु हेमचन्द्र ने इन्हें अन्य शब्दावली में प्रकट किया है, उनके अनुसार 'सम्यक् अर्थनिणर्यः' ही प्रमाण है। आचार्य हेमचन्द्र का प्रमाणमीमांसा नामक यह ग्रन्थ भी इसी क्रम में