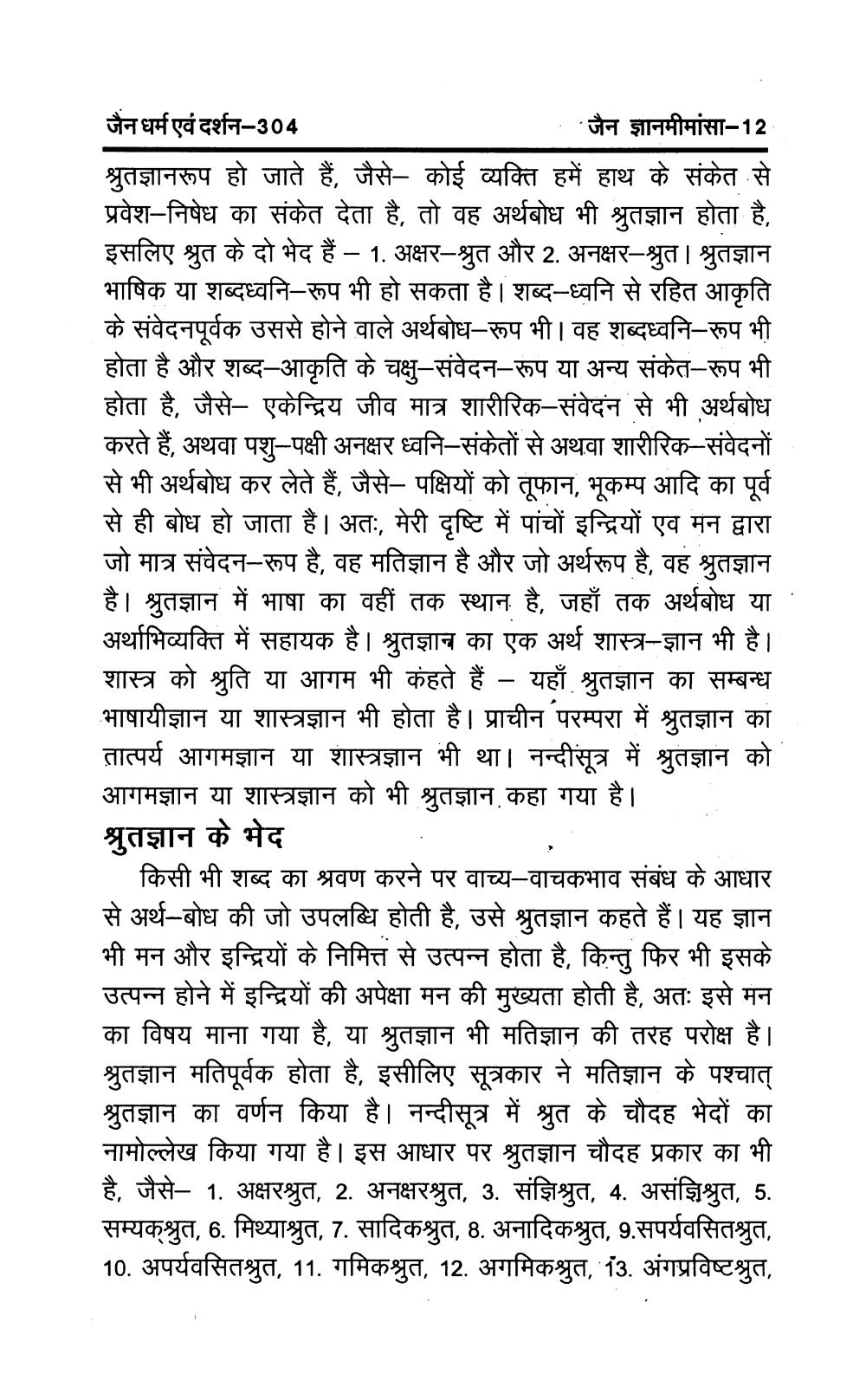________________ जैन धर्म एवं दर्शन-304 .. 'जैन ज्ञानमीमांसा-12 श्रुतज्ञानरूप हो जाते हैं, जैसे- कोई व्यक्ति हमें हाथ के संकेत से प्रवेश निषेध का संकेत देता है, तो वह अर्थबोध भी श्रुतज्ञान होता है, इसलिए श्रुत के दो भेद हैं - 1. अक्षर-श्रुत और 2. अनक्षर-श्रुत / श्रुतज्ञान भाषिक या शब्दध्वनि-रूप भी हो सकता है। शब्द-ध्वनि से रहित आकृति के संवेदनपूर्वक उससे होने वाले अर्थबोध-रूप भी / वह शब्दध्वनि-रूप भी होता है और शब्द-आकृति के चक्षु-संवेदन-रूप या अन्य संकेत-रूप भी होता है, जैसे- एकेन्द्रिय जीव मात्र शारीरिक-संवेदन से भी अर्थबोध करते हैं, अथवा पशु-पक्षी अनक्षर ध्वनि-संकेतों से अथवा शारीरिक-संवेदनों से भी अर्थबोध कर लेते हैं, जैसे- पक्षियों को तूफान, भूकम्प आदि का पूर्व से ही बोध हो जाता है। अतः, मेरी दृष्टि में पांचों इन्द्रियों एव मन द्वारा जो मात्र संवेदन-रूप है, वह मतिज्ञान है और जो अर्थरूप है, वह श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान में भाषा का वहीं तक स्थान है, जहाँ तक अर्थबोध या अर्थाभिव्यक्ति में सहायक है। श्रुतज्ञान का एक अर्थ शास्त्र-ज्ञान भी है। शास्त्र को श्रुति या आगम भी कहते हैं - यहाँ श्रुतज्ञान का सम्बन्ध भाषायीज्ञान या शास्त्रज्ञान भी होता है। प्राचीन परम्परा में श्रुतज्ञान का तात्पर्य आगमज्ञान या शास्त्रज्ञान भी था। नन्दीसूत्र में श्रुतज्ञान को आगमज्ञान या शास्त्रज्ञान को भी श्रुतज्ञान कहा गया है। श्रुतज्ञान के भेद किसी भी शब्द का श्रवण करने पर वाच्य-वाचकभाव संबंध के आधार से अर्थ-बोध की जो उपलब्धि होती है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान भी मन और इन्द्रियों के निमित्त से उत्पन्न होता है, किन्तु फिर भी इसके उत्पन्न होने में इन्द्रियों की अपेक्षा मन की मुख्यता होती है, अतः इसे मन का विषय माना गया है, या श्रुतज्ञान भी मतिज्ञान की तरह परोक्ष है। श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है, इसीलिए सूत्रकार ने मतिज्ञान के पश्चात् श्रुतज्ञान का वर्णन किया है। नन्दीसूत्र में श्रुत के चौदह भेदों का नामोल्लेख किया गया है। इस आधार पर श्रुतज्ञान चौदह प्रकार का भी है, जैसे- 1. अक्षरश्रुत, 2. अनक्षरश्रुत, 3. संज्ञिश्रुत, 4. असंज्ञिश्रुत, 5. सम्यकश्रुत, 6. मिथ्याश्रुत, 7. सादिकश्रुत, 8. अनादिकश्रुत, 9.सपर्यवसितश्रुत, 10. अपर्यवसितश्रुत, 11. गमिकश्रुत, 12. अगमिकश्रुत, 13. अंगप्रविष्टश्रुत,