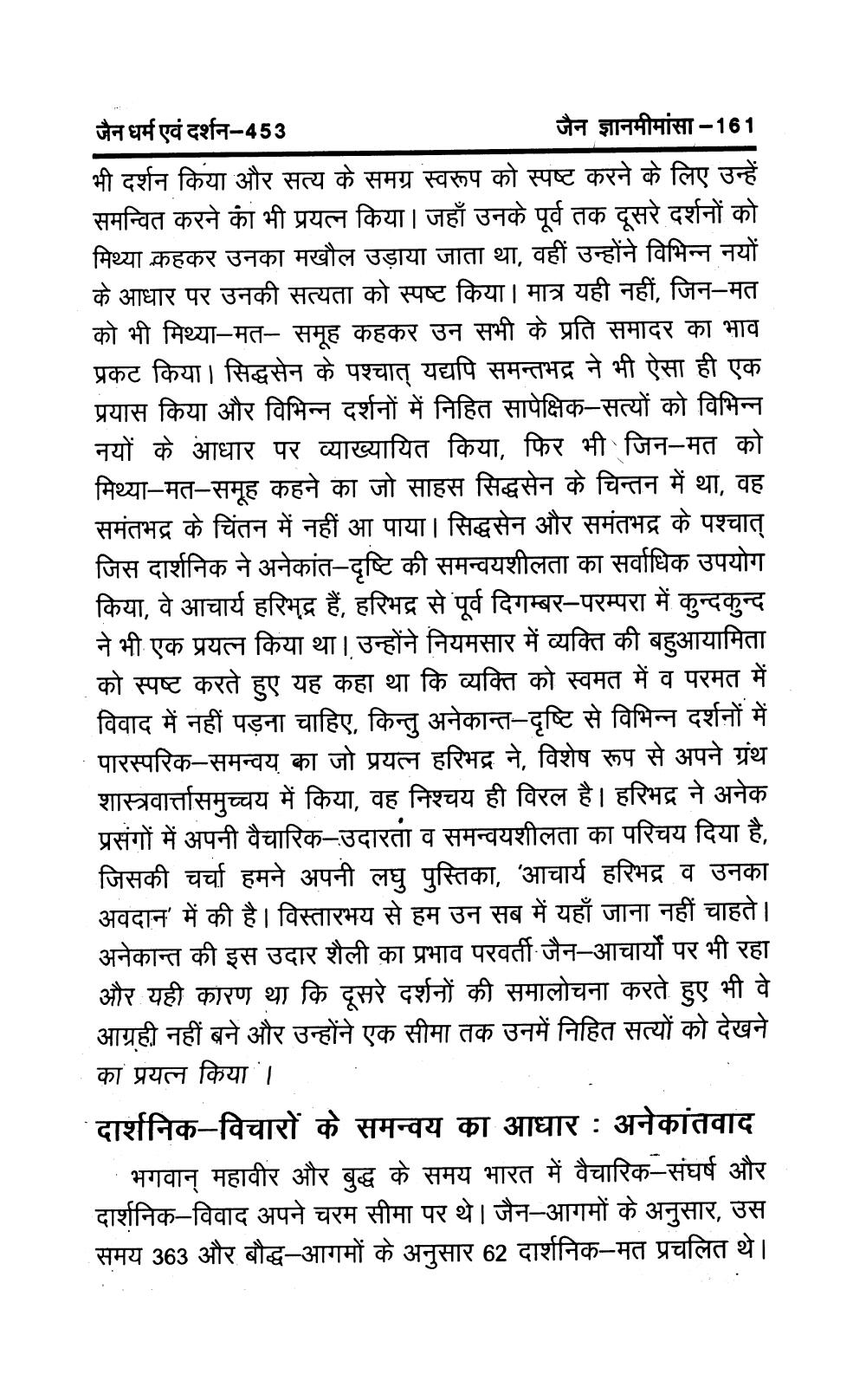________________ जैन धर्म एवं दर्शन-453 जैन ज्ञानमीमांसा -161 भी दर्शन किया और सत्य के समग्र स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उन्हें समन्वित करने का भी प्रयत्न किया / जहाँ उनके पूर्व तक दूसरे दर्शनों को मिथ्या कहकर उनका मखौल उड़ाया जाता था, वहीं उन्होंने विभिन्न नयों के आधार पर उनकी सत्यता को स्पष्ट किया। मात्र यही नहीं, जिन-मत को भी मिथ्या-मत- समूह कहकर उन सभी के प्रति समादर का भाव प्रकट किया। सिद्धसेन के पश्चात् यद्यपि समन्तभद्र ने भी ऐसा ही एक प्रयास किया और विभिन्न दर्शनों में निहित सापेक्षिक सत्यों को विभिन्न नयों के आधार पर व्याख्यायित किया, फिर भी जिन-मत को मिथ्या-मत-समूह कहने का जो साहस सिद्धसेन के चिन्तन में था, वह समंतभद्र के चिंतन में नहीं आ पाया। सिद्धसेन और समंतभद्र के पश्चात् जिस दार्शनिक ने अनेकांत-दृष्टि की समन्वयशीलता का सर्वाधिक उपयोग किया, वे आचार्य हरिभद्र हैं, हरिभद्र से पूर्व दिगम्बर-परम्परा में कुन्दकुन्द ने भी एक प्रयत्न किया था। उन्होंने नियमसार में व्यक्ति की बहुआयामिता को स्पष्ट करते हुए यह कहा था कि व्यक्ति को स्वमत में व परमत में विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, किन्तु अनेकान्त-दृष्टि से विभिन्न दर्शनों में पारस्परिक-समन्वय का जो प्रयत्न हरिभद्र ने, विशेष रूप से अपने ग्रंथ शास्त्रवार्तासमुच्चय में किया, वह निश्चय ही विरल है। हरिभद्र ने अनेक प्रसंगों में अपनी वैचारिक-उदारता व समन्वयशीलता का परिचय दिया है, जिसकी चर्चा हमने अपनी लघु पुस्तिका, 'आचार्य हरिभद्र व उनका अवदान' में की है। विस्तारभय से हम उन सब में यहाँ जाना नहीं चाहते। अनेकान्त की इस उदार शैली का प्रभाव परवर्ती जैन-आचार्यों पर भी रहा और यही कारण था कि दूसरे दर्शनों की समालोचना करते हुए भी वे आग्रही नहीं बने और उन्होंने एक सीमा तक उनमें निहित सत्यों को देखने का प्रयत्न किया / दार्शनिक-विचारों के समन्वय का आधार : अनेकांतवाद * भगवान् महावीर और बुद्ध के समय भारत में वैचारिक-संघर्ष और दार्शनिक-विवाद अपने चरम सीमा पर थे। जैन-आगमों के अनुसार, उस समय 363 और बौद्ध-आगमों के अनुसार 62 दार्शनिक-मत प्रचलित थे।