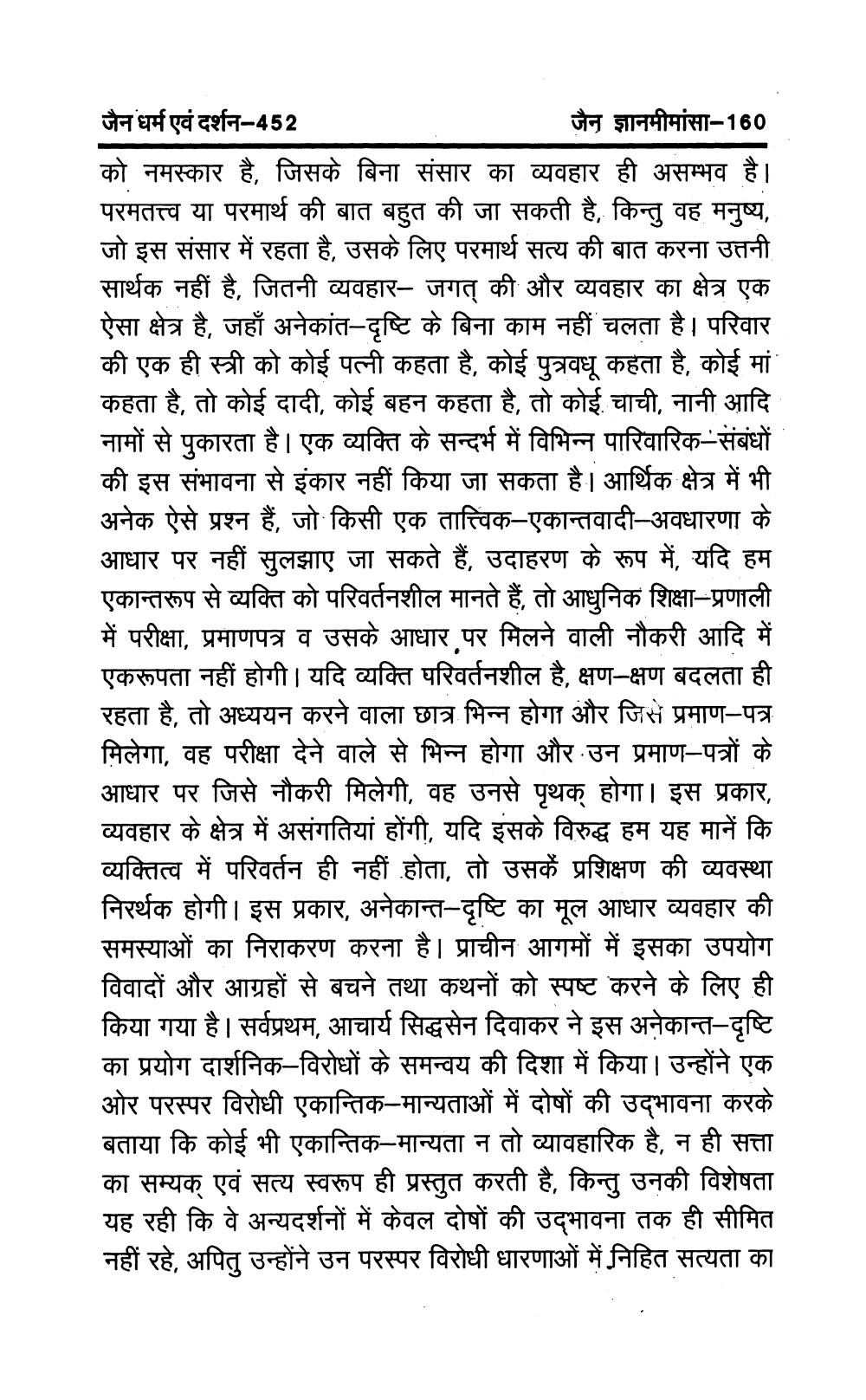________________ जैन धर्म एवं दर्शन-452 जैन ज्ञानमीमांसा-160 को नमस्कार है, जिसके बिना संसार का व्यवहार ही असम्भव है। परमतत्त्व या परमार्थ की बात बहुत की जा सकती है, किन्तु वह मनुष्य, जो इस संसार में रहता है, उसके लिए परमार्थ सत्य की बात करना उत्तनी सार्थक नहीं है, जितनी व्यवहार- जगत् की और व्यवहार का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ अनेकांत-दृष्टि के बिना काम नहीं चलता है। परिवार की एक ही स्त्री को कोई पत्नी कहता है, कोई पुत्रवधू कहता है, कोई मां कहता है, तो कोई दादी, कोई बहन कहता है, तो कोई. चाची, नानी आदि नामों से पुकारता है। एक व्यक्ति के सन्दर्भ में विभिन्न पारिवारिक संबंधों की इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में भी अनेक ऐसे प्रश्न हैं, जो किसी एक तात्त्विक-एकान्तवादी-अवधारणा के आधार पर नहीं सुलझाए जा सकते हैं, उदाहरण के रूप में, यदि हम एकान्तरूप से व्यक्ति को परिवर्तनशील मानते हैं, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा, प्रमाणपत्र व उसके आधार पर मिलने वाली नौकरी आदि में एकरूपता नहीं होगी। यदि व्यक्ति परिवर्तनशील है, क्षण-क्षण बदलता ही रहता है, तो अध्ययन करने वाला छात्र भिन्न होगा और जिसे प्रमाण-पत्र मिलेगा, वह परीक्षा देने वाले से भिन्न होगा और उन प्रमाण-पत्रों के आधार पर जिसे नौकरी मिलेगी, वह उनसे पृथक होगा। इस प्रकार, व्यवहार के क्षेत्र में असंगतियां होंगी, यदि इसके विरुद्ध हम यह मानें कि व्यक्तित्व में परिवर्तन ही नहीं होता, तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था निरर्थक होगी। इस प्रकार, अनेकान्त-दृष्टि का मूल आधार व्यवहार की समस्याओं का निराकरण करना है। प्राचीन आगमों में इसका उपयोग विवादों और आग्रहों से बचने तथा कथनों को स्पष्ट करने के लिए ही किया गया है। सर्वप्रथम, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने इस अनेकान्त-दृष्टि का प्रयोग दार्शनिक-विरोधों के समन्वय की दिशा में किया। उन्होंने एक ओर परस्पर विरोधी एकान्तिक-मान्यताओं में दोषों की उद्भावना करके बताया कि कोई भी एकान्तिक-मान्यता न तो व्यावहारिक है, न ही सत्ता का सम्यक एवं सत्य स्वरूप ही प्रस्तुत करती है, किन्तु उनकी विशेषता यह रही कि वे अन्यदर्शनों में केवल दोषों की उदभावना तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु उन्होंने उन परस्पर विरोधी धारणाओं में निहित सत्यता का