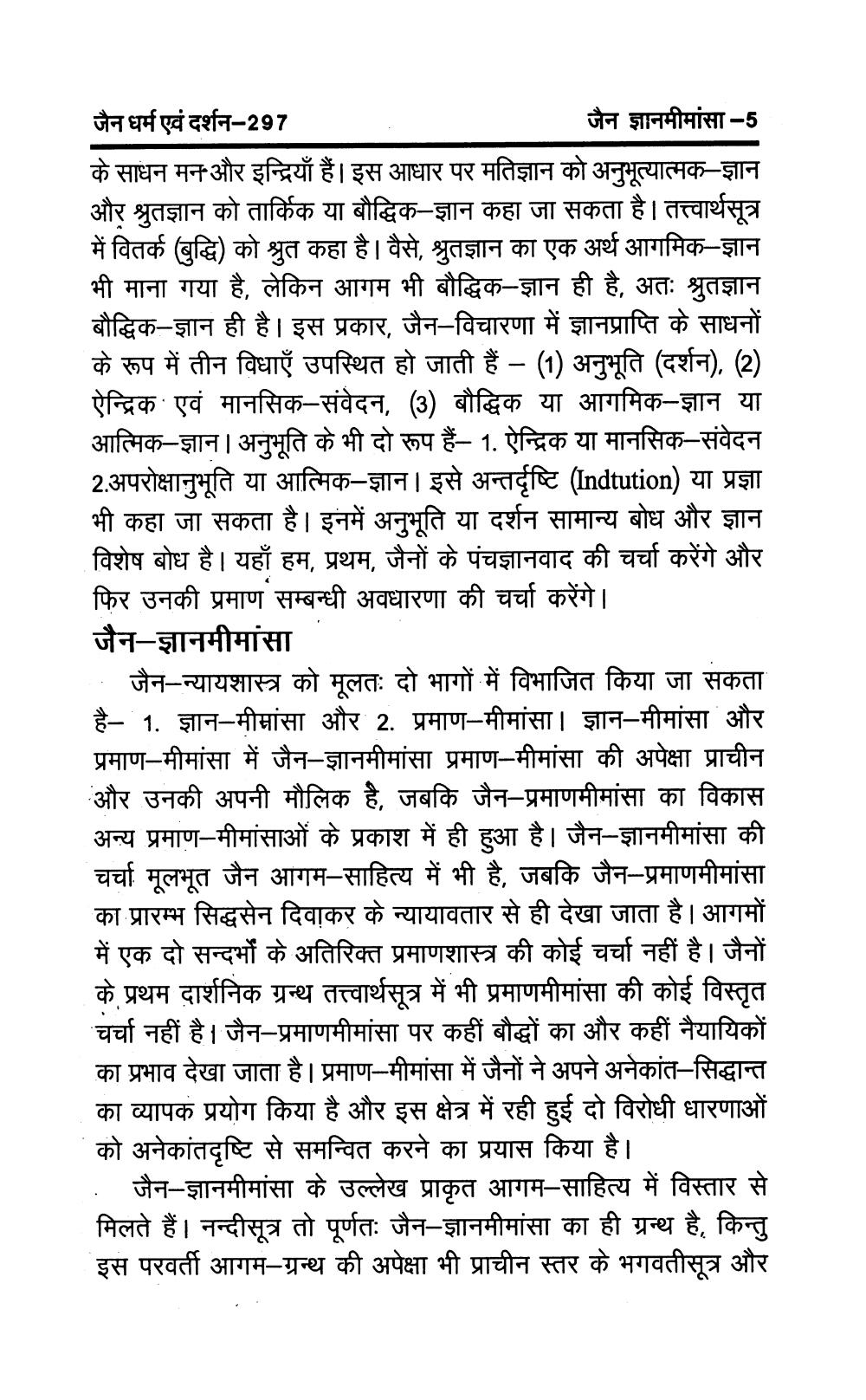________________ जैन धर्म एवं दर्शन-297 जैन ज्ञानमीमांसा-5 के साधन मन और इन्द्रियाँ हैं। इस आधार पर मतिज्ञान को अनुभूत्यात्मक ज्ञान और श्रुतज्ञान को तार्किक या बौद्धिक-ज्ञान कहा जा सकता है। तत्त्वार्थसूत्र में वितर्क (बुद्धि) को श्रुत कहा है। वैसे, श्रुतज्ञान का एक अर्थ आगमिक-ज्ञान भी माना गया है, लेकिन आगम भी बौद्धिक-ज्ञान ही है, अतः श्रुतज्ञान बौद्धिक ज्ञान ही है। इस प्रकार, जैन-विचारणा में ज्ञानप्राप्ति के साधनों के रूप में तीन विधाएँ उपस्थित हो जाती हैं - (1) अनुभूति (दर्शन), (2) ऐन्द्रिक एवं मानसिक-संवेदन, (3) बौद्धिक या आगमिक-ज्ञान या आत्मिक ज्ञान / अनुभूति के भी दो रूप हैं- 1. ऐन्द्रिक या मानसिक-संवेदन 2.अपरोक्षानुभूति या आत्मिक-ज्ञान / इसे अन्तर्दृष्टि (Indtution) या प्रज्ञा भी कहा जा सकता है। इनमें अनुभूति या दर्शन सामान्य बोध और ज्ञान विशेष बोध है। यहाँ हम, प्रथम, जैनों के पंचज्ञानवाद की चर्चा करेंगे और फिर उनकी प्रमाण सम्बन्धी अवधारणा की चर्चा करेंगे। जैन-ज्ञानमीमांसा - जैन-न्यायशास्त्र को मूलतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- 1. ज्ञान-मीमांसा और 2. प्रमाण-मीमांसा। ज्ञान-मीमांसा और प्रमाण-मीमांसा में जैन-ज्ञानमीमांसा प्रमाण-मीमांसा की अपेक्षा प्राचीन और उनकी अपनी मौलिक है, जबकि जैन-प्रमाणमीमांसा का विकास अन्य प्रमाण-मीमांसाओं के प्रकाश में ही हुआ है। जैन-ज्ञानमीमांसा की चर्चा मूलभूत जैन आगम-साहित्य में भी है, जबकि जैन-प्रमाणमीमांसा का प्रारम्भ सिद्धसेन दिवाकर के न्यायावतार से ही देखा जाता है। आगमों में एक दो सन्दर्भो के अतिरिक्त प्रमाणशास्त्र की कोई चर्चा नहीं है। जैनों के प्रथम दार्शनिक ग्रन्थ तत्त्वार्थसूत्र में भी प्रमाणमीमांसा की कोई विस्तृत चर्चा नहीं है। जैन-प्रमाणमीमांसा पर कहीं बौद्धों का और कहीं नैयायिकों का प्रभाव देखा जाता है। प्रमाण-मीमांसा में जैनों ने अपने अनेकांत-सिद्धान्त का व्यापक प्रयोग किया है और इस क्षेत्र में रही हुई दो विरोधी धारणाओं को अनेकांतदृष्टि से समन्वित करने का प्रयास किया है। . जैन-ज्ञानमीमांसा के उल्लेख प्राकृत आगम-साहित्य में विस्तार से मिलते हैं। नन्दीसूत्र तो पूर्णतः जैन-ज्ञानमीमांसा का ही ग्रन्थ है, किन्तु इस परवर्ती आगम-ग्रन्थ की अपेक्षा भी प्राचीन स्तर के भगवतीसूत्र और