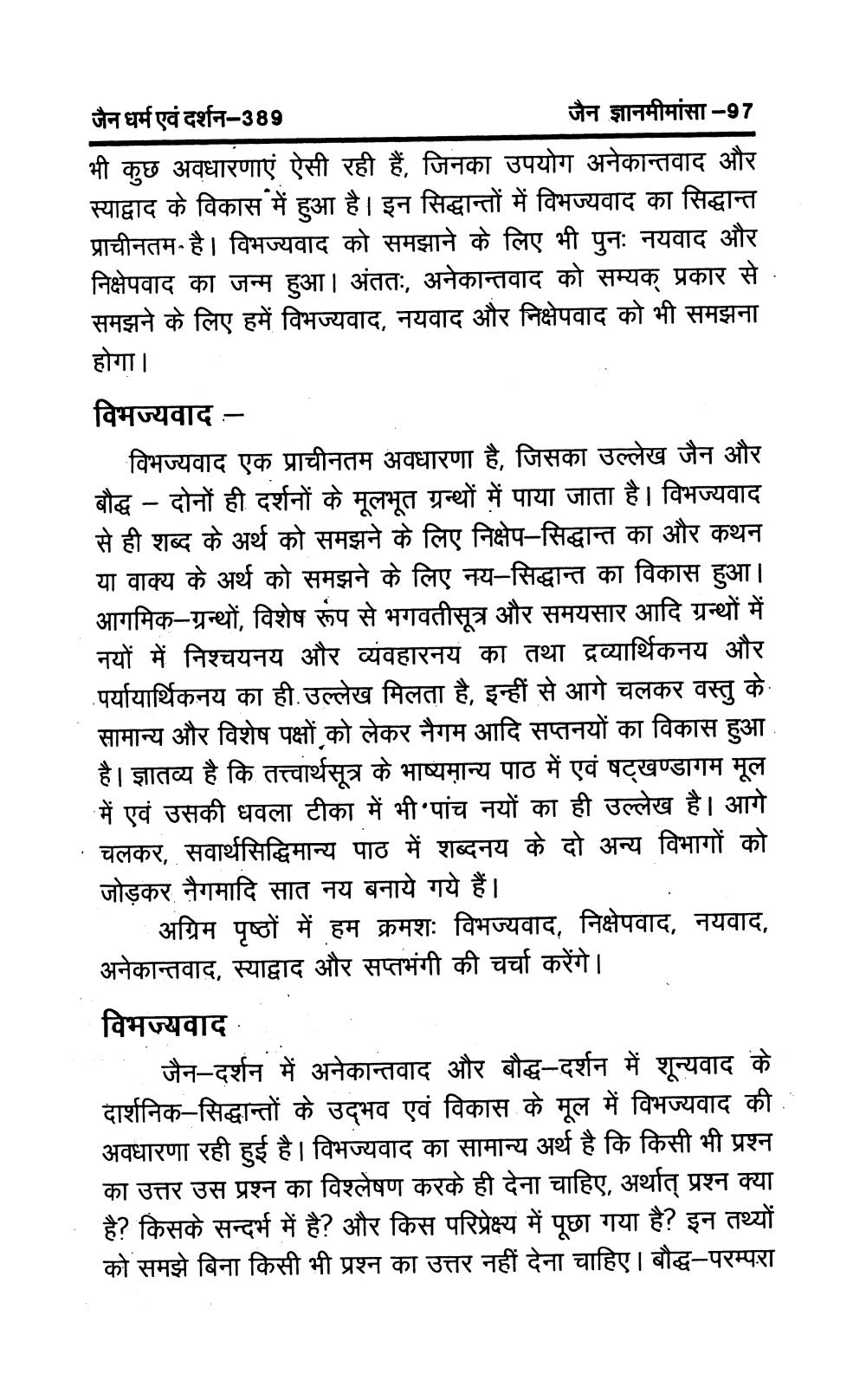________________ जैन धर्म एवं दर्शन-389 जैन ज्ञानमीमांसा-97 भी कुछ अवधारणाएं ऐसी रही हैं, जिनका उपयोग अनेकान्तवाद और स्याद्वाद के विकास में हुआ है। इन सिद्धान्तों में विभज्यवाद का सिद्धान्त प्राचीनतम है। विभज्यवाद को समझाने के लिए भी पुनः नयवाद और निक्षेपवाद का जन्म हुआ। अंततः, अनेकान्तवाद को सम्यक् प्रकार से . समझने के लिए हमें विभज्यवाद, नयवाद और निक्षेपवाद को भी समझना होगा। विभज्यवाद - विभज्यवाद एक प्राचीनतम अवधारणा है, जिसका उल्लेख जैन और बौद्ध - दोनों ही दर्शनों के मूलभूत ग्रन्थों में पाया जाता है। विभज्यवाद से ही शब्द के अर्थ को समझने के लिए निक्षेप-सिद्धान्त का और कथन या वाक्य के अर्थ को समझने के लिए नय-सिद्धान्त का विकास हुआ। आगमिक-ग्रन्थों, विशेष रूप से भगवतीसूत्र और समयसार आदि ग्रन्थों में नयों में निश्चयनय और व्यवहारनय का तथा द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनय का ही. उल्लेख मिलता है, इन्हीं से आगे चलकर वस्तु के सामान्य और विशेष पक्षों को लेकर नैगम आदि सप्तनयों का विकास हुआ है। ज्ञातव्य है कि तत्त्वार्थसूत्र के भाष्यमान्य पाठ में एवं षट्खण्डागम मूल में एवं उसकी धवला टीका में भी पांच नयों का ही उल्लेख है। आगे चलकर, सवार्थसिद्धिमान्य पाठ में शब्दनय के दो अन्य विभागों को जोड़कर नैगमादि सात नय बनाये गये हैं। अग्रिम पृष्ठों में हम क्रमशः विभज्यवाद, निक्षेपवाद, नयवाद, अनेकान्तवाद, स्याद्वाद और सप्तभंगी की चर्चा करेंगे। विभज्यवाद __ जैन-दर्शन में अनेकान्तवाद और बौद्ध-दर्शन में शून्यवाद के दार्शनिक-सिद्धान्तों के उद्भव एवं विकास के मूल में विभज्यवाद की . अवधारणा रही हुई है। विभज्यवाद का सामान्य अर्थ है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न का विश्लेषण करके ही देना चाहिए, अर्थात् प्रश्न क्या है? किसके सन्दर्भ में है? और किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है? इन तथ्यों को समझे बिना किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। बौद्ध-परम्परा