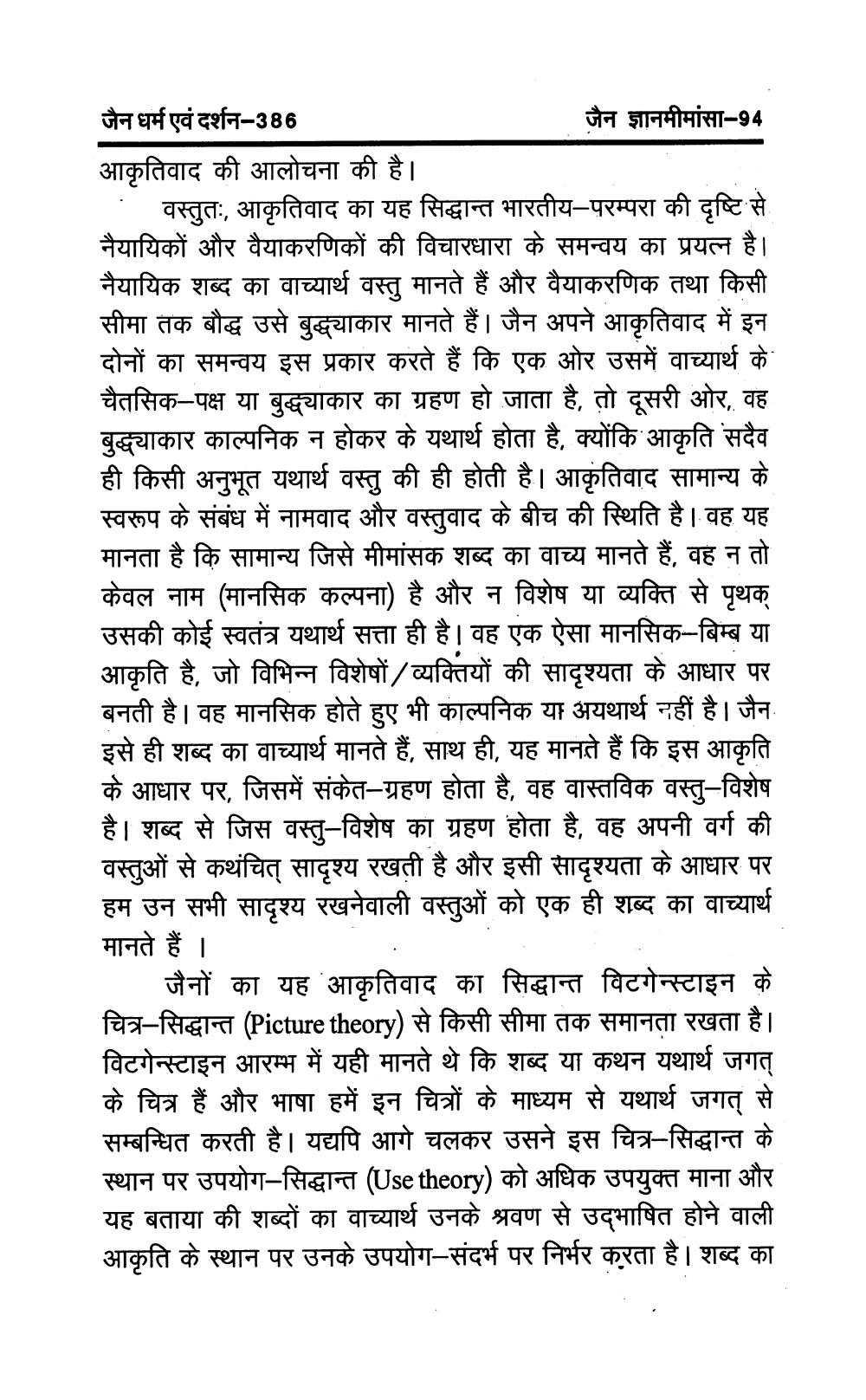________________ जैन धर्म एवं दर्शन-386 जैन ज्ञानमीमांसा-94 आकृतिवाद की आलोचना की है। . वस्तुतः, आकृतिवाद का यह सिद्धान्त भारतीय-परम्परा की दृष्टि से नैयायिकों और वैयाकरणिकों की विचारधारा के समन्वय का प्रयत्न है। नैयायिक शब्द का वाच्यार्थ वस्तु मानते हैं और वैयाकरणिक तथा किसी सीमा तक बौद्ध उसे बुद्ध्याकार मानते हैं। जैन अपने आकृतिवाद में इन दोनों का समन्वय इस प्रकार करते हैं कि एक ओर उसमें वाच्यार्थ के चैतसिक-पक्ष या बुद्ध्याकार का ग्रहण हो जाता है, तो दूसरी ओर, वह बुद्ध्याकार काल्पनिक न होकर के यथार्थ होता है, क्योंकि आकृति सदैव ही किसी अनुभूत यथार्थ वस्तु की ही होती है। आकृतिवाद सामान्य के स्वरूप के संबंध में नामवाद और वस्तुवाद के बीच की स्थिति है। वह यह मानता है कि सामान्य जिसे मीमांसक शब्द का वाच्य मानते हैं, वह न तो केवल नाम (मानसिक कल्पना) है और न विशेष या व्यक्ति से पृथक उसकी कोई स्वतंत्र यथार्थ सत्ता ही है। वह एक ऐसा मानसिक-बिम्ब या आकति है, जो विभिन्न विशेषों/व्यक्तियों की सादृश्यता के आधार पर बनती है। वह मानसिक होते हुए भी काल्पनिक या अयथार्थ नहीं है। जैन इसे ही शब्द का वाच्यार्थ मानते हैं, साथ ही, यह मानते हैं कि इस आकृति के आधार पर, जिसमें संकेत-ग्रहण होता है, वह वास्तविक वस्तु-विशेष है। शब्द से जिस वस्तु-विशेष का ग्रहण होता है, वह अपनी वर्ग की वस्तुओं से कथंचित् सादृश्य रखती है और इसी सादृश्यता के आधार पर हम उन सभी सादृश्य रखनेवाली वस्तुओं को एक ही शब्द का वाच्यार्थ मानते हैं / जैनों का यह आकृतिवाद का सिद्धान्त विटगेन्स्टाइन के चित्र-सिद्धान्त (Picture theory) से किसी सीमा तक समानता रखता है। विटगेन्स्टाइन आरम्भ में यही मानते थे कि शब्द या कथन यथार्थ जगत् के चित्र हैं और भाषा हमें इन चित्रों के माध्यम से यथार्थ जगत् से सम्बन्धित करती है। यद्यपि आगे चलकर उसने इस चित्र-सिद्धान्त के स्थान पर उपयोग-सिद्धान्त (Use theory) को अधिक उपयुक्त माना और यह बताया की शब्दों का वाच्यार्थ उनके श्रवण से उद्भाषित होने वाली आकृति के स्थान पर उनके उपयोग-संदर्भ पर निर्भर करता है। शब्द का