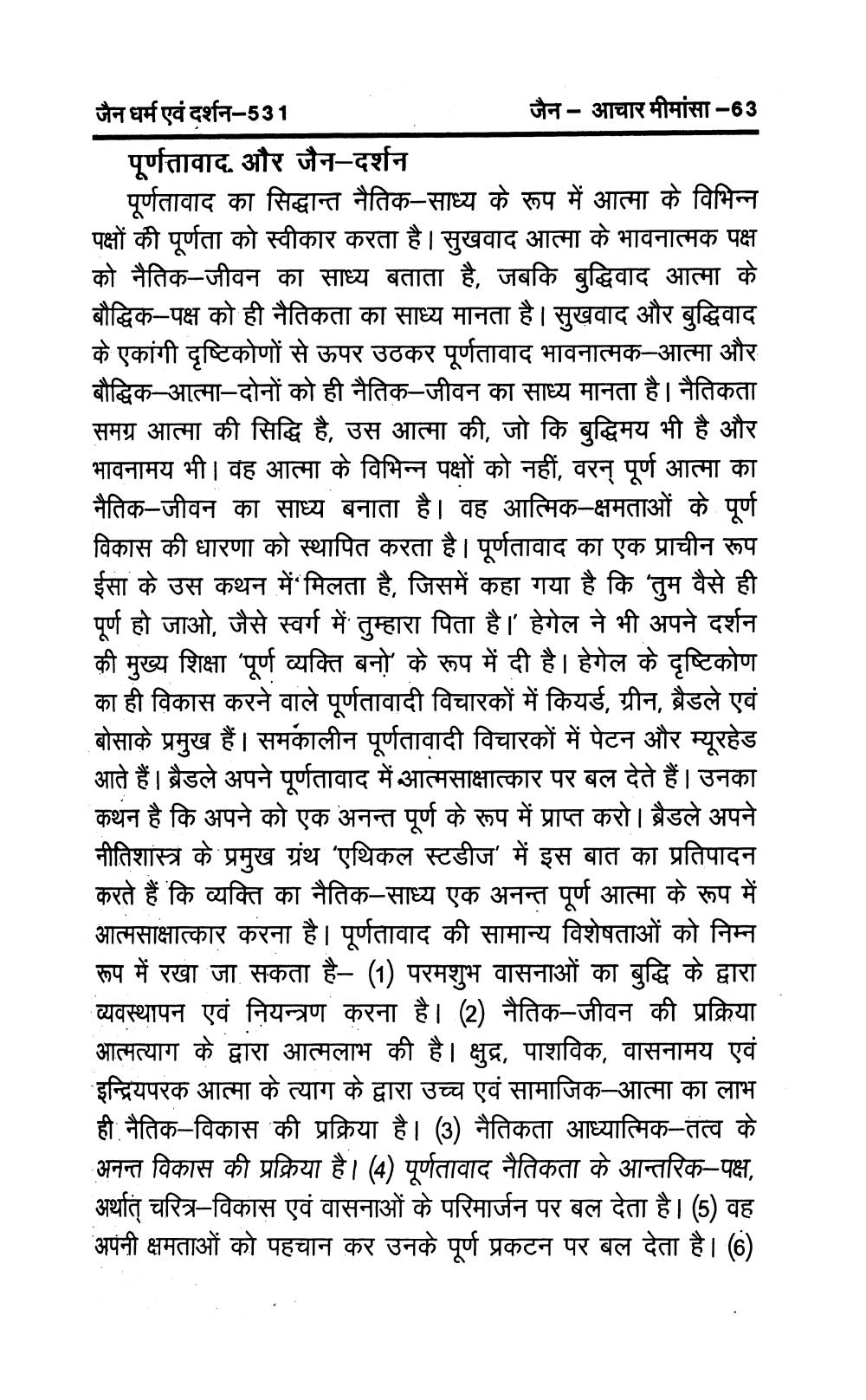________________ जैन धर्म एवं दर्शन-531 जैन- आचार मीमांसा-63 पूर्णतावाद, और जैन-दर्शन पूर्णतावाद का सिद्धान्त नैतिक-साध्य के रूप में आत्मा के विभिन्न पक्षों की पूर्णता को स्वीकार करता है। सुखवाद आत्मा के भावनात्मक पक्ष को नैतिक-जीवन का साध्य बताता है, जबकि बुद्धिवाद आत्मा के बौद्धिक-पक्ष को ही नैतिकता का साध्य मानता है। सुखवाद और बुद्धिवाद के एकांगी दृष्टिकोणों से ऊपर उठकर पूर्णतावाद भावनात्मक-आत्मा और बौद्धिक आत्मा दोनों को ही नैतिक-जीवन का साध्य मानता है। नैतिकता समग्र आत्मा की सिद्धि है, उस आत्मा की, जो कि बुद्धिमय भी है और भावनामय भी। वह आत्मा के विभिन्न पक्षों को नहीं, वरन् पूर्ण आत्मा का नैतिक-जीवन का साध्य बनाता है। वह आत्मिक क्षमताओं के पूर्ण विकास की धारणा को स्थापित करता है। पूर्णतावाद का एक प्राचीन रूप ईसा के उस कथन में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि 'तुम वैसे ही पूर्ण हो जाओ, जैसे स्वर्ग में तुम्हारा पिता है।' हेगेल ने भी अपने दर्शन की मुख्य शिक्षा 'पूर्ण व्यक्ति बनो' के रूप में दी है। हेगेल के दृष्टिकोण का ही विकास करने वाले पूर्णतावादी विचारकों में कियर्ड, ग्रीन, ब्रैडले एवं बोसाके प्रमुख हैं। समकालीन पूर्णतावादी विचारकों में पेटन और म्यूरहेड आते हैं। ब्रैडले अपने पूर्णतावाद में आत्मसाक्षात्कार पर बल देते हैं। उनका कथन है कि अपने को एक अनन्त पूर्ण के रूप में प्राप्त करो। ब्रैडले अपने नीतिशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ ‘एथिकल स्टडीज' में इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति का नैतिक-साध्य एक अनन्त पूर्ण आत्मा के रूप में आत्मसाक्षात्कार करना है। पूर्णतावाद की सामान्य विशेषताओं को निम्न रूप में रखा जा सकता है- (1) परमशुभ वासनाओं का बुद्धि के द्वारा व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण करना है। (2) नैतिक-जीवन की प्रक्रिया आत्मत्याग के द्वारा आत्मलाभ की है। क्षुद्र, पाशविक, वासनामय एवं इन्द्रियपरक आत्मा के त्याग के द्वारा उच्च एवं सामाजिक-आत्मा का लाभ ही नैतिक-विकास की प्रक्रिया है। (3) नैतिकता आध्यात्मिक-तत्व के अनन्त विकास की प्रक्रिया है। (4) पूर्णतावाद नैतिकता के आन्तरिक-पक्ष, अर्थात् चरित्र-विकास एवं वासनाओं के परिमार्जन पर बल देता है। (5) वह अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनके पूर्ण प्रकटन पर बल देता है। (6)