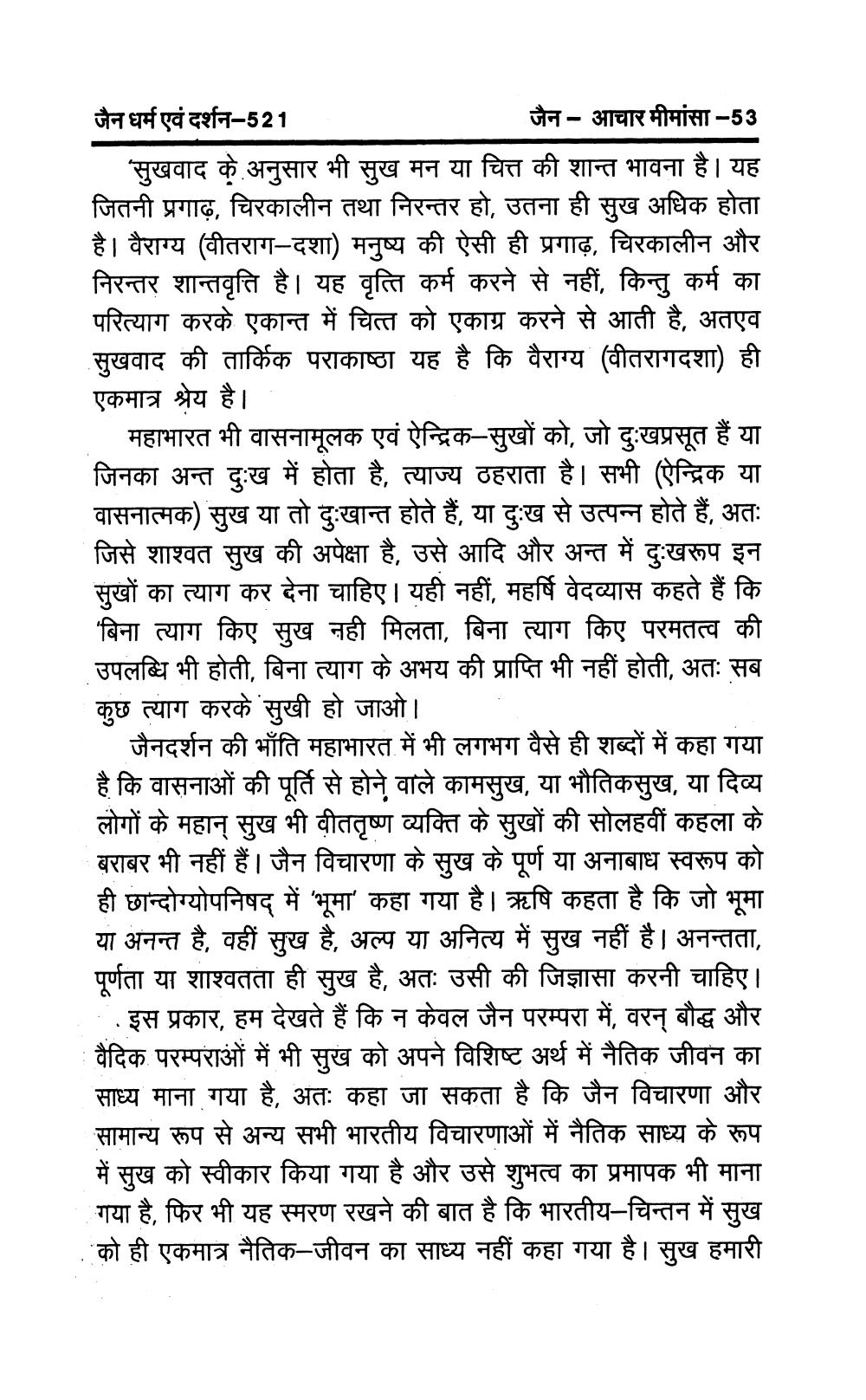________________ जैन धर्म एवं दर्शन-521 जैन- आचार मीमांसा-53 'सुखवाद के अनुसार भी सुख मन या चित्त की शान्त भावना है। यह जितनी प्रगाढ़, चिरकालीन तथा निरन्तर हो, उतना ही सुख अधिक होता है। वैराग्य (वीतराग-दशा) मनुष्य की ऐसी ही प्रगाढ़, चिरकालीन और निरन्तर शान्तवृति है। यह वृत्ति कर्म करने से नहीं, किन्तु कर्म का परित्याग करके एकान्त में चित्त को एकाग्र करने से आती है, अतएव सुखवाद की तार्किक पराकाष्ठा यह है कि वैराग्य (वीतरागदशा) ही एकमात्र श्रेय है। महाभारत भी वासनामूलक एवं ऐन्द्रिक-सुखों को, जो दुःखप्रसूत हैं या जिनका अन्त दुःख में होता है, त्याज्य ठहराता है। सभी (ऐन्द्रिक या वासनात्मक) सुख या तो दुःखान्त होते हैं, या दुःख से उत्पन्न होते हैं, अतः जिसे शाश्वत सुख की अपेक्षा है, उसे आदि और अन्त में दुःखरूप इन सुखों का त्याग कर देना चाहिए। यही नहीं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि 'बिना त्याग किए सुख नही मिलता, बिना त्याग किए परमतत्व की उपलब्धि भी होती, बिना त्याग के अभय की प्राप्ति भी नहीं होती, अतः सब कुछ त्याग करके सुखी हो जाओ। जैनदर्शन की भाँति महाभारत में भी लगभग वैसे ही शब्दों में कहा गया है कि वासनाओं की पूर्ति से होने वाले कामसुख, या भौतिकसुख, या दिव्य लोगों के महान् सुख भी वीततृष्ण व्यक्ति के सुखों की सोलहवीं कहला के बराबर भी नहीं हैं। जैन विचारणा के सुख के पूर्ण या अनाबाध स्वरूप को ही छान्दोग्योपनिषद् में 'भूमा' कहा गया है। ऋषि कहता है कि जो भूमा या अनन्त है, वहीं सुख है, अल्प या अनित्य में सुख नहीं है। अनन्तता, पूर्णता या शाश्वतता ही सुख है, अतः उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। - . इस प्रकार, हम देखते हैं कि न केवल जैन परम्परा में, वरन् बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में भी सुख को अपने विशिष्ट अर्थ में नैतिक जीवन का साध्य माना गया है, अतः कहा जा सकता है कि जैन विचारणा और सामान्य रूप से अन्य सभी भारतीय विचारणाओं में नैतिक साध्य के रूप में सुख को स्वीकार किया गया है और उसे शुभत्व का प्रमापक भी माना गया है, फिर भी यह स्मरण रखने की बात है कि भारतीय-चिन्तन में सुख . को ही एकमात्र नैतिक-जीवन का साध्य नहीं कहा गया है। सुख हमारी