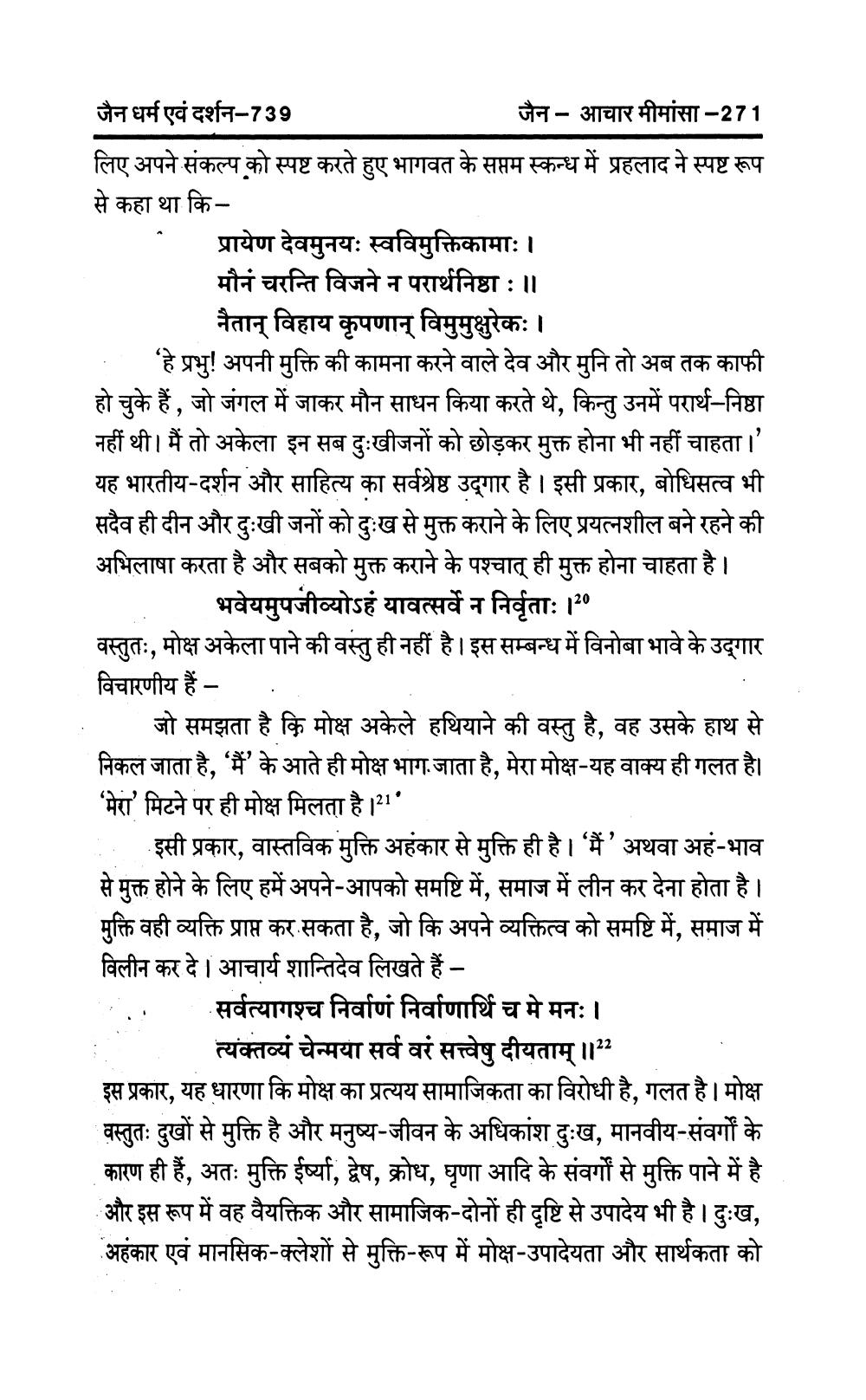________________ जैन धर्म एवं दर्शन-739 जैन- आचार मीमांसा-271 लिए अपने संकल्प को स्पष्ट करते हुए भागवत के सप्तम स्कन्ध में प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामाः। मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा : // नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षुरेकः / - हे प्रभु! अपनी मुक्ति की कामना करने वाले देव और मुनि तो अब तक काफी हो चुके हैं, जो जंगल में जाकर मौन साधन किया करते थे, किन्तु उनमें परार्थ-निष्ठा नहीं थी। मैं तो अकेला इन सब दुःखीजनों को छोड़कर मुक्त होना भी नहीं चाहता।' यह भारतीय-दर्शन और साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उद्गार है। इसी प्रकार, बोधिसत्व भी सदैव ही दीन और दुःखी जनों को दुःख से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील बने रहने की अभिलाषा करता है और सबको मुक्त कराने के पश्चात् ही मुक्त होना चाहता है। . भवेयमुपजीव्योऽहं यावत्सर्वे न निर्वृताः / वस्तुतः, मोक्ष अकेला पाने की वस्तु ही नहीं है। इस सम्बन्ध में विनोबा भावे के उद्गार विचारणीय हैं - .. जो समझता है कि मोक्ष अकेले हथियाने की वस्तु है, वह उसके हाथ से निकल जाता है, 'मैं' के आते ही मोक्ष भाग जाता है, मेरा मोक्ष-यह वाक्य ही गलत है। 'मेरा' मिटने पर ही मोक्ष मिलता है। - इसी प्रकार, वास्तविक मुक्ति अहंकार से मुक्ति ही है। मैं' अथवा अहं-भाव से मुक्त होने के लिए हमें अपने-आपको समष्टि में, समाज में लीन कर देना होता है। मुक्ति वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जो कि अपने व्यक्तित्व को समष्टि में, समाज में विलीन कर दे। आचार्य शान्तिदेव लिखते हैं - ... सर्वत्यागश्च निर्वाणं निर्वाणार्थि च मे मनः। त्यक्तव्यं चेन्मया सर्व वरं सत्त्वेषु दीयताम् // 2 इस प्रकार, यह धारणा कि मोक्ष का प्रत्यय सामाजिकता का विरोधी है, गलत है। मोक्ष वस्तुतः दुखों से मुक्ति है और मनुष्य-जीवन के अधिकांश दुःख, मानवीय-संवर्गों के कारण ही हैं, अतः मुक्ति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा आदि के संवर्गों से मुक्ति पाने में है और इस रूप में वह वैयक्तिक और सामाजिक-दोनों ही दृष्टि से उपादेय भी है। दुःख, अहंकार एवं मानसिक-क्लेशों से मुक्ति-रूप में मोक्ष-उपादेयता और सार्थकता को