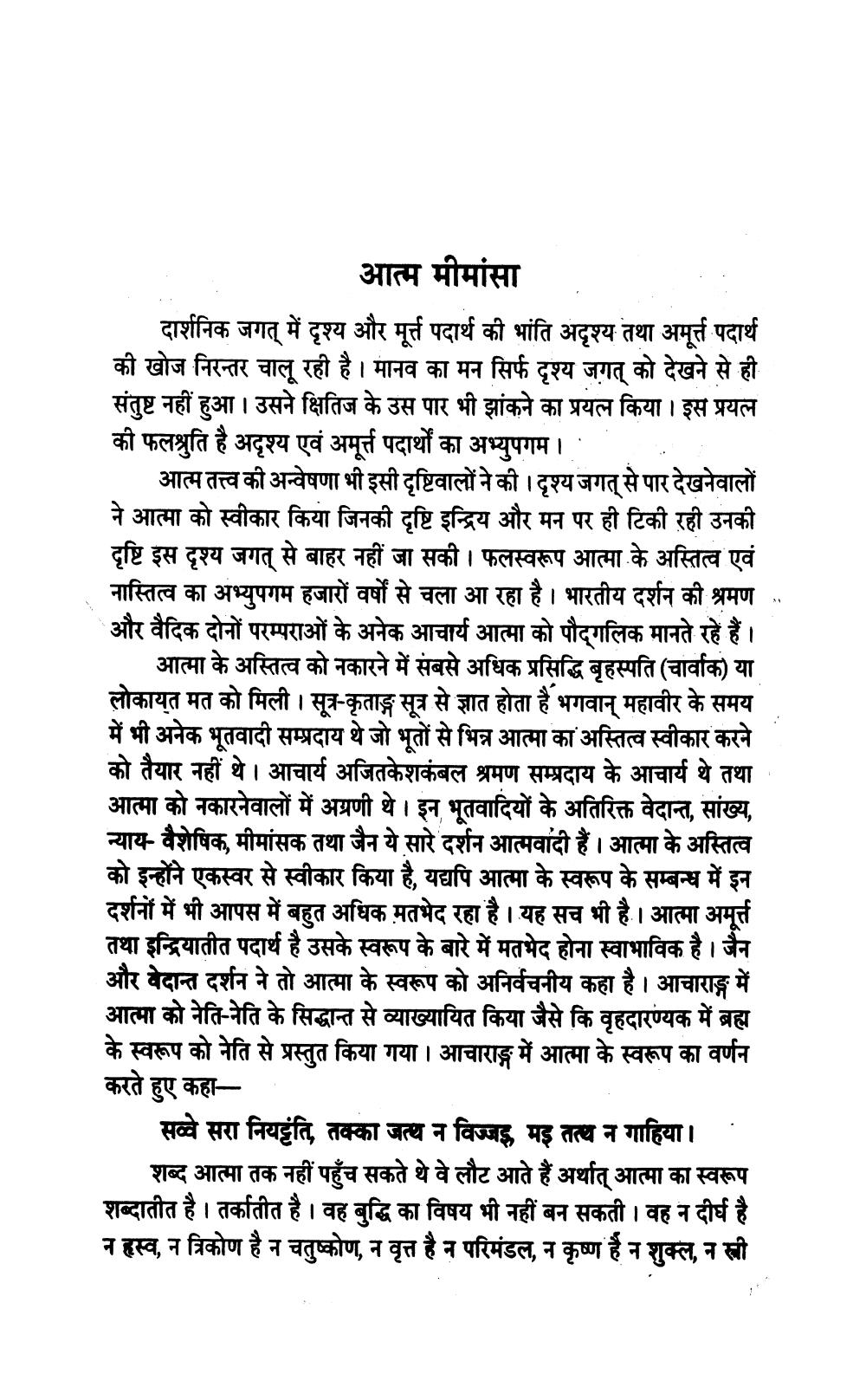________________ आत्म मीमांसा दार्शनिक जगत् में दृश्य और मूर्त पदार्थ की भांति अदृश्य तथा अमूर्त पदार्थ की खोज निरन्तर चालू रही है। मानव का मन सिर्फ दृश्य जगत् को देखने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने क्षितिज के उस पार भी झांकने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न की फलश्रुति है अदृश्य एवं अमूर्त पदार्थों का अभ्युपगम। ___आत्म तत्त्व की अन्वेषणा भी इसी दृष्टिवालों ने की / दृश्य जगत् से पार देखनेवालों ने आत्मा को स्वीकार किया जिनकी दृष्टि इन्द्रिय और मन पर ही टिकी रही उनकी दृष्टि इस दृश्य जगत् से बाहर नहीं जा सकी। फलस्वरूप आत्मा के अस्तित्व एवं नास्तित्व का अभ्युपगम हजारों वर्षों से चला आ रहा है। भारतीय दर्शन की श्रमण .. और वैदिक दोनों परम्पराओं के अनेक आचार्य आत्मा को पौदगलिक मानते रहे हैं। आत्मा के अस्तित्व को नकारने में सबसे अधिक प्रसिद्धि बृहस्पति (चार्वाक) या लोकायत मत को मिली। सूत्र-कृताङ्ग सूत्र से ज्ञात होता है भगवान् महावीर के समय में भी अनेक भूतवादी सम्प्रदाय थे जो भूतों से भिन्न आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। आचार्य अजितकेशकंबल श्रमण सम्प्रदाय के आचार्य थे तथा आत्मा को नकारनेवालों में अग्रणी थे। इन भूतवादियों के अतिरिक्त वेदान्त, सांख्य, न्याय-वैशेषिक, मीमांसक तथा जैन ये सारे दर्शन आत्मवादी हैं / आत्मा के अस्तित्व को इन्होंने एकस्वर से स्वीकार किया है, यद्यपि आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में इन दर्शनों में भी आपस में बहुत अधिक मतभेद रहा है / यह सच भी है। आत्मा अमूर्त तथा इन्द्रियातीत पदार्थ है उसके स्वरूप के बारे में मतभेद होना स्वाभाविक है / जैन और वेदान्त दर्शन ने तो आत्मा के स्वरूप को अनिर्वचनीय कहा है। आचाराङ्ग में आत्मा को नेति-नेति के सिद्धान्त से व्याख्यायित किया जैसे कि वृहदारण्यक में ब्रह्म के स्वरूप को नेति से प्रस्तुत किया गया। आचाराङ्ग में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा सव्वे सरा नियटृति, तक्का जत्थ न विज्जइ मइ तत्थ न गाहिया। शब्द आत्मा तक नहीं पहुँच सकते थे वे लौट आते हैं अर्थात् आत्मा का स्वरूप शब्दातीत है। तर्कातीत है / वह बुद्धि का विषय भी नहीं बन सकती। वह न दीर्घ है न हस्व, न त्रिकोण है न चतुष्कोण, न वृत्त है न परिमंडल, न कृष्ण है न शुक्ल, न स्त्री