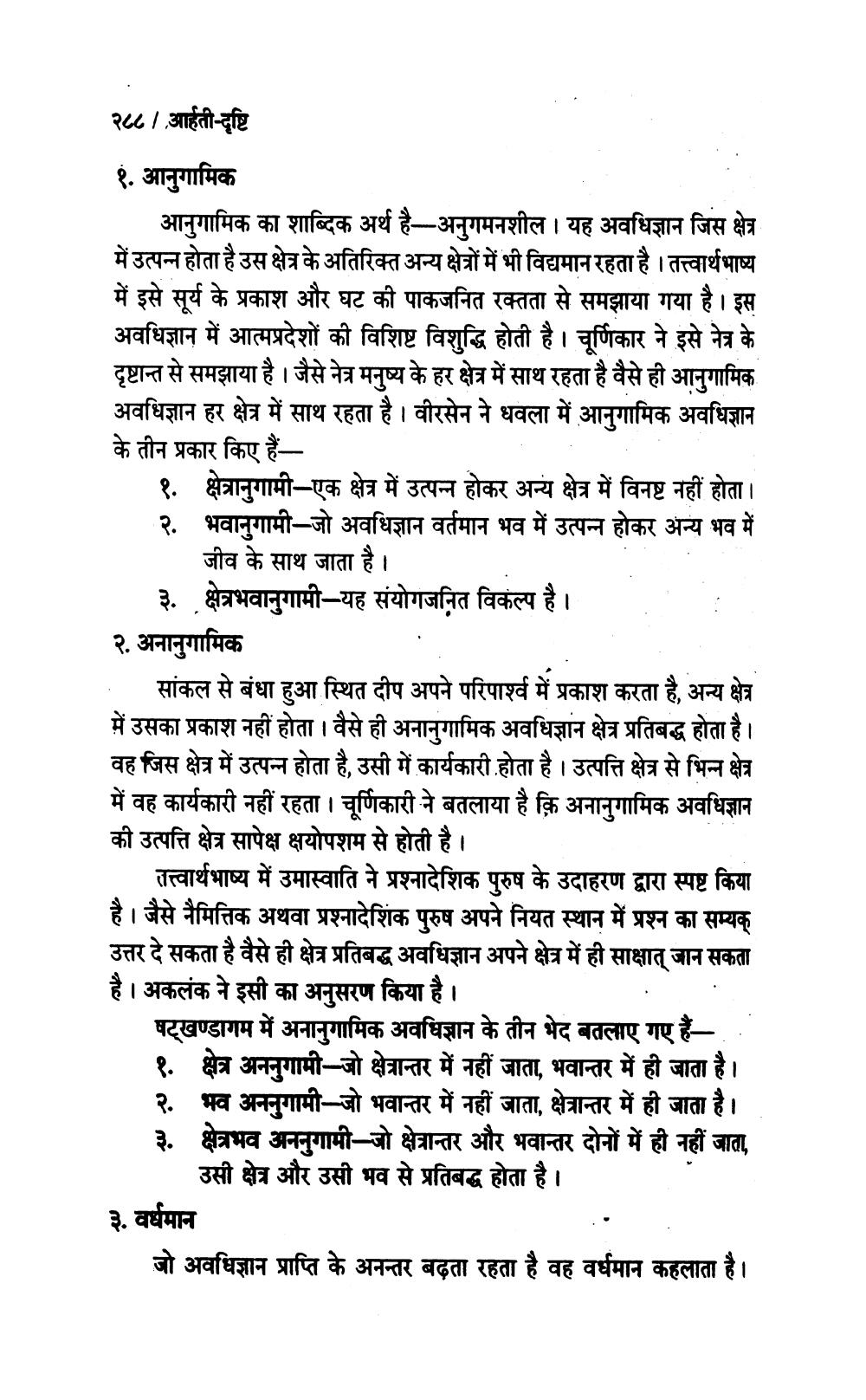________________ 288 / आर्हती-दृष्टि 1. आनुगामिक आनुगामिक का शाब्दिक अर्थ है-अनुगमनशील। यह अवधिज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है उस क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यमान रहता है / तत्त्वार्थभाष्य में इसे सूर्य के प्रकाश और घट की पाकजनित रक्तता से समझाया गया है। इस अवधिज्ञान में आत्मप्रदेशों की विशिष्ट विशुद्धि होती है। चूर्णिकार ने इसे नेत्र के दृष्टान्त से समझाया है / जैसे नेत्र मनुष्य के हर क्षेत्र में साथ रहता है वैसे ही आनुगामिक अवधिज्ञान हर क्षेत्र में साथ रहता है / वीरसेन ने धवला में आनुगामिक अवधिज्ञान के तीन प्रकार किए हैं 1. क्षेत्रानुगामी-एक क्षेत्र में उत्पन्न होकर अन्य क्षेत्र में विनष्ट नहीं होता। 2. भवानुगामी-जो अवधिज्ञान वर्तमान भव में उत्पन्न होकर अन्य भव में जीव के साथ जाता है। 3. क्षेत्रभवानुगामी-यह संयोगजनित विकल्प है। 2. अनानुगामिक . सांकल से बंधा हुआ स्थित दीप अपने परिपार्श्व में प्रकाश करता है, अन्य क्षेत्र में उसका प्रकाश नहीं होता। वैसे ही अनानुगामिक अवधिज्ञान क्षेत्र प्रतिबद्ध होता है। वह जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है, उसी में कार्यकारी होता है / उत्पत्ति क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में वह कार्यकारी नहीं रहता। चूर्णिकारी ने बतलाया है कि अनानुगामिक अवधिज्ञान की उत्पत्ति क्षेत्र सापेक्ष क्षयोपशम से होती है। तत्त्वार्थभाष्य में उमास्वाति ने प्रश्नादेशिक पुरुष के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। जैसे नैमित्तिक अथवा प्रश्नादेशिक पुरुष अपने नियत स्थान में प्रश्न का सम्यक् उत्तर दे सकता है वैसे ही क्षेत्र प्रतिबद्ध अवधिज्ञान अपने क्षेत्र में ही साक्षात् जान सकता है। अकलंक ने इसी का अनुसरण किया है। षट्खण्डागम में अनानुगामिक अवधिज्ञान के तीन भेद बतलाए गए हैं- . 1. क्षेत्र अननुगामी-जो क्षेत्रान्तर में नहीं जाता, भवान्तर में ही जाता है। 2. भव अननुगामी-जो भवान्तर में नहीं जाता, क्षेत्रान्तर में ही जाता है। 3. क्षेत्रभव अननुगामी-जो क्षेत्रान्तर और भवान्तर दोनों में ही नहीं जाता, उसी क्षेत्र और उसी भव से प्रतिबद्ध होता है। 3. वर्धमान जो अवधिज्ञान प्राप्ति के अनन्तर बढ़ता रहता है वह वर्धमान कहलाता है।