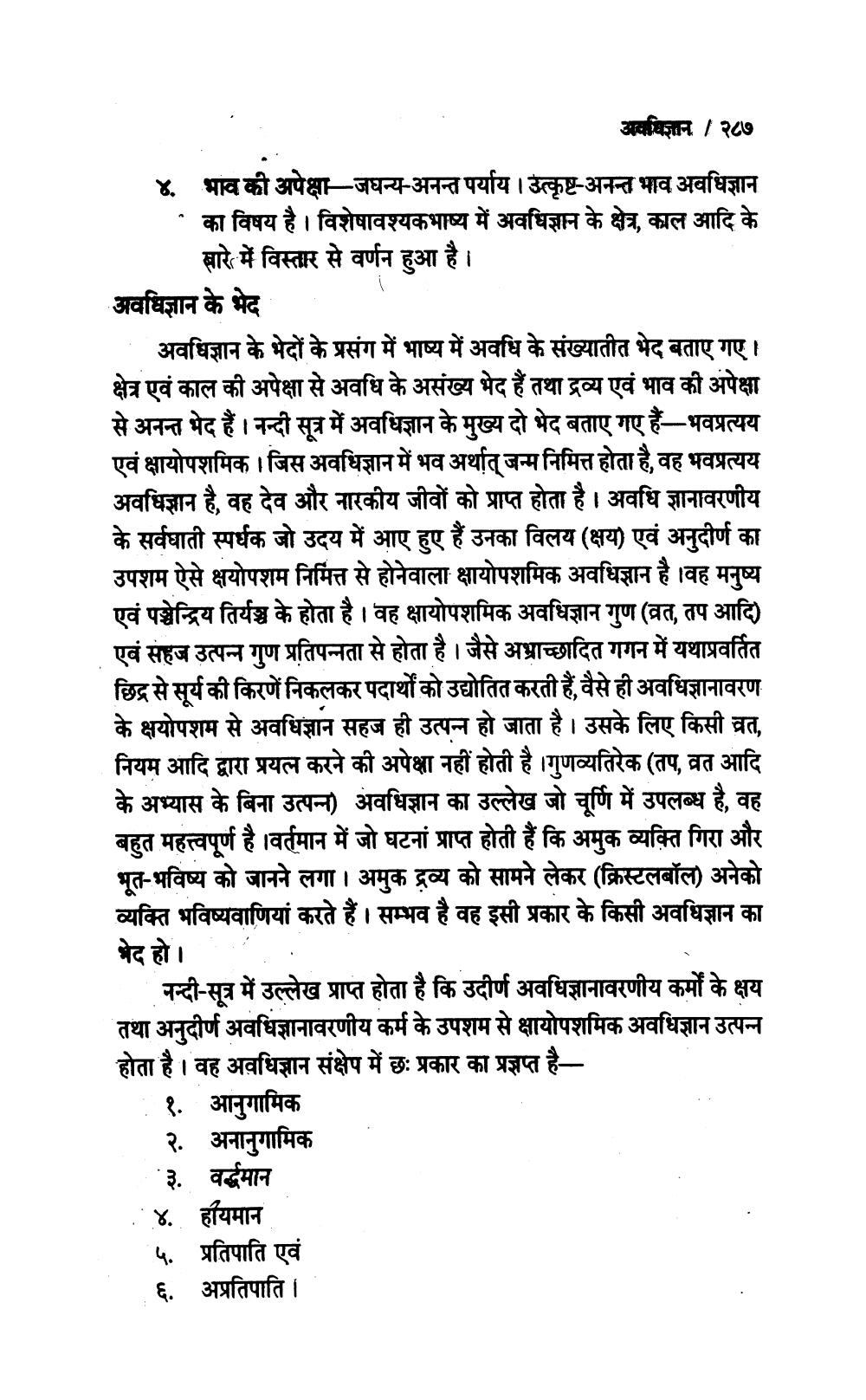________________ अविज्ञान / 287 4. भाव की अपेक्षा जघन्य-अनन्त पर्याय / उत्कृष्ट-अनन्त भाव अवधिज्ञान ' का विषय है। विशेषावश्यकभाष्य में अवधिज्ञान के क्षेत्र, काल आदि के खारे में विस्तार से वर्णन हआ है। अवधिज्ञान के भेद ___ अवधिज्ञान के भेदों के प्रसंग में भाष्य में अवधि के संख्यातीत भेद बताए गए। क्षेत्र एवं काल की अपेक्षा से अवधि के असंख्य भेद हैं तथा द्रव्य एवं भाव की अपेक्षा से अनन्त भेद हैं / नन्दी सूत्र में अवधिज्ञान के मुख्य दो भेद बताए गए है—भवप्रत्यय एवं क्षायोपशमिक / जिस अवधिज्ञान में भव अर्थात् जन्म निमित्त होता है, वह भवप्रत्यय अवधिज्ञान है, वह देव और नारकीय जीवों को प्राप्त होता है / अवधि ज्ञानावरणीय के सर्वघाती स्पर्धक जो उदय में आए हुए हैं उनका विलय (क्षय) एवं अनुदीर्ण का उपशम ऐसे क्षयोपशम निमित्त से होनेवाला क्षायोपशमिक अवधिज्ञान है ।वह मनुष्य एवं पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च के होता है / वह क्षायोपशमिक अवधिज्ञान गुण (व्रत, तप आदि) एवं सहज उत्पन्न गुण प्रतिपन्नता से होता है / जैसे अभ्राच्छादित गगन में यथाप्रवर्तित छिद्र से सूर्य की किरणें निकलकर पदार्थों को उद्योतित करती हैं, वैसे ही अवधिज्ञानावरण के क्षयोपशम से अवधिज्ञान सहज ही उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए किसी व्रत, नियम आदि द्वारा प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं होती है ।गुणव्यतिरेक (तप, व्रत आदि के अभ्यास के बिना उत्पन्न) अवधिज्ञान का उल्लेख जो चूर्णि में उपलब्ध है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है ।वर्तमान में जो घटनां प्राप्त होती हैं कि अमुक व्यक्ति गिरा और भूत-भविष्य को जानने लगा। अमुक द्रव्य को सामने लेकर (क्रिस्टलबॉल) अनेको व्यक्ति भविष्यवाणियां करते हैं। सम्भव है वह इसी प्रकार के किसी अवधिज्ञान का भेद हो। नन्दी-सूत्र में उल्लेख प्राप्त होता है कि उदीर्ण अवधिज्ञानावरणीय कर्मों के क्षय तथा अनुदीर्ण अवधिज्ञानावरणीय कर्म के उपशम से क्षायोपशमिक अवधिज्ञान उत्पन्न होता है। वह अवधिज्ञान संक्षेप में छः प्रकार का प्रज्ञप्त है 1. आनुगामिक 2. अनानुगामिक 3. वर्द्धमान .. 4. हायमान 5. प्रतिपाति एवं 6. अप्रतिपाति /