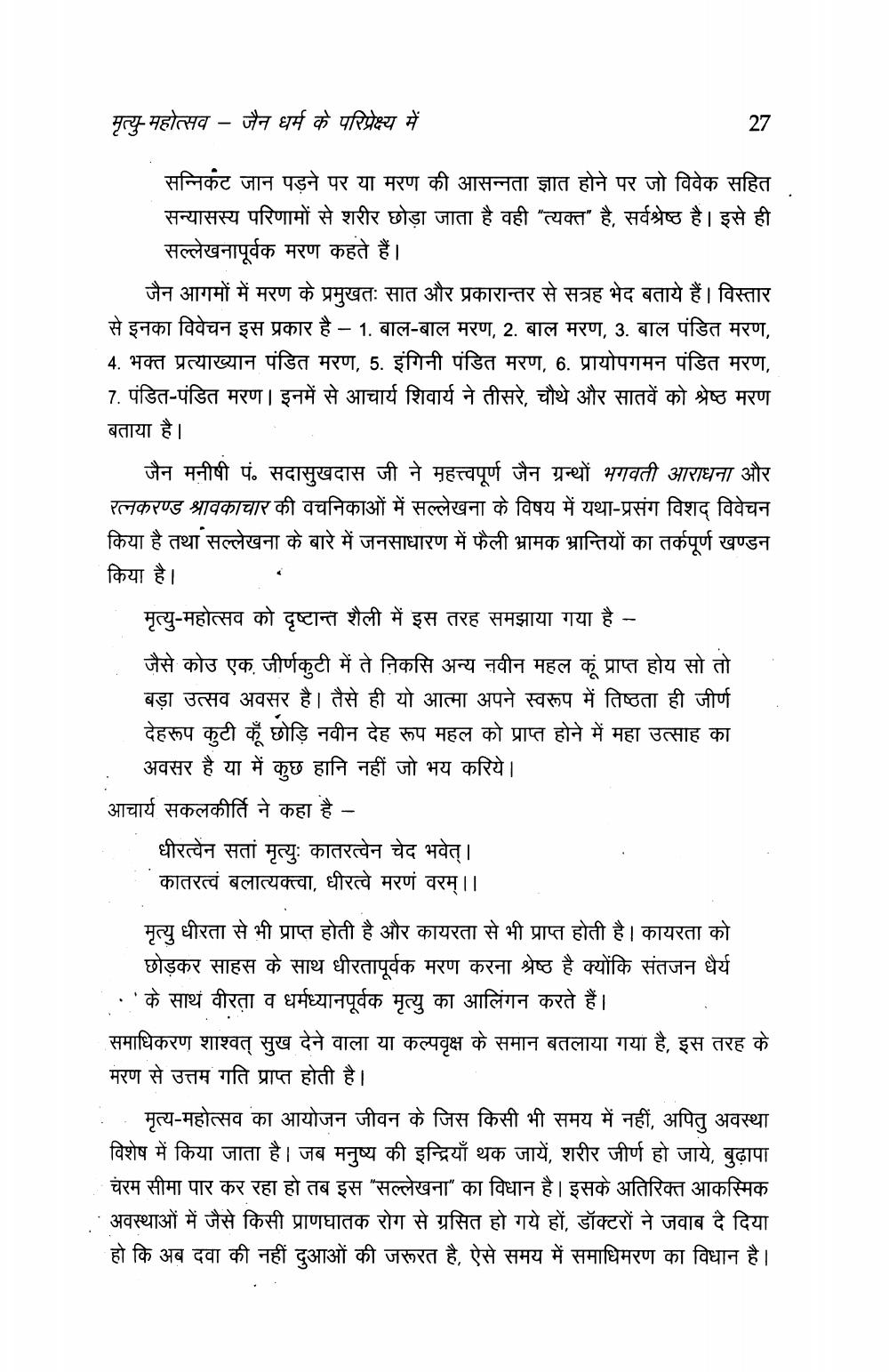________________ मृत्यु- महोत्सव - जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में 27 सन्निकट जान पड़ने पर या मरण की आसन्नता ज्ञात होने पर जो विवेक सहित सन्यासस्य परिणामों से शरीर छोड़ा जाता है वही “त्यक्त” है, सर्वश्रेष्ठ है। इसे ही सल्लेखनापूर्वक मरण कहते हैं। जैन आगमों में मरण के प्रमुखतः सात और प्रकारान्तर से सत्रह भेद बताये हैं। विस्तार से इनका विवेचन इस प्रकार है - 1. बाल-बाल मरण, 2. बाल मरण, 3. बाल पंडित मरण, 4. भक्त प्रत्याख्यान पंडित मरण, 5. इंगिनी पंडित मरण, 6. प्रायोपगमन पंडित मरण, 7. पंडित-पंडित मरण / इनमें से आचार्य शिवार्य ने तीसरे, चौथे और सातवें को श्रेष्ठ मरण बताया है। जैन मनीषी पं. सदासुखदास जी ने महत्त्वपूर्ण जैन ग्रन्थों भगवती आराधना और रत्नकरण्ड श्रावकाचार की वचनिकाओं में सल्लेखना के विषय में यथा-प्रसंग विशद् विवेचन किया है तथा सल्लेखना के बारे में जनसाधारण में फैली भ्रामक भ्रान्तियों का तर्कपूर्ण खण्डन किया है। मृत्यु-महोत्सव को दृष्टान्त शैली में इस तरह समझाया गया है - जैसे कोउ एक जीर्णकुटी में ते निकसि अन्य नवीन महल कू प्राप्त होय सो तो बड़ा उत्सव अवसर है। तैसे ही यो आत्मा अपने स्वरूप में तिष्ठता ही जीर्ण देहरूप कुटी 1 छोड़ि नवीन देह रूप महल को प्राप्त होने में महा उत्साह का अवसर है या में कुछ हानि नहीं जो भय करिये। आचार्य सकलकीर्ति ने कहा है - धीरत्वेन सतां मृत्युः कातरत्वेन चेद भवेत् / कातरत्वं बलात्यक्त्वा, धीरत्वे मरणं वरम्।। मृत्यु धीरता से भी प्राप्त होती है और कायरता से भी प्राप्त होती है। कायरता को छोड़कर साहस के साथ धीरतापूर्वक मरण करना श्रेष्ठ है क्योंकि संतजन धैर्य . ' के साथं वीरता व धर्मध्यानपूर्वक मृत्यु का आलिंगन करते हैं। समाधिकरण शाश्वत् सुख देने वाला या कल्पवृक्ष के समान बतलाया गया है, इस तरह के मरण से उत्तम गति प्राप्त होती है। - मृत्य-महोत्सव का आयोजन जीवन के जिस किसी भी समय में नहीं, अपितु अवस्था विशेष में किया जाता है। जब मनुष्य की इन्द्रियाँ थक जायें, शरीर जीर्ण हो जाये, बुढ़ापा चरम सीमा पार कर रहा हो तब इस “सल्लेखना” का विधान है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक .' अवस्थाओं में जैसे किसी प्राणघातक रोग से ग्रसित हो गये हों, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो कि अब दवा की नहीं दुआओं की जरूरत है, ऐसे समय में समाधिमरण का विधान है।