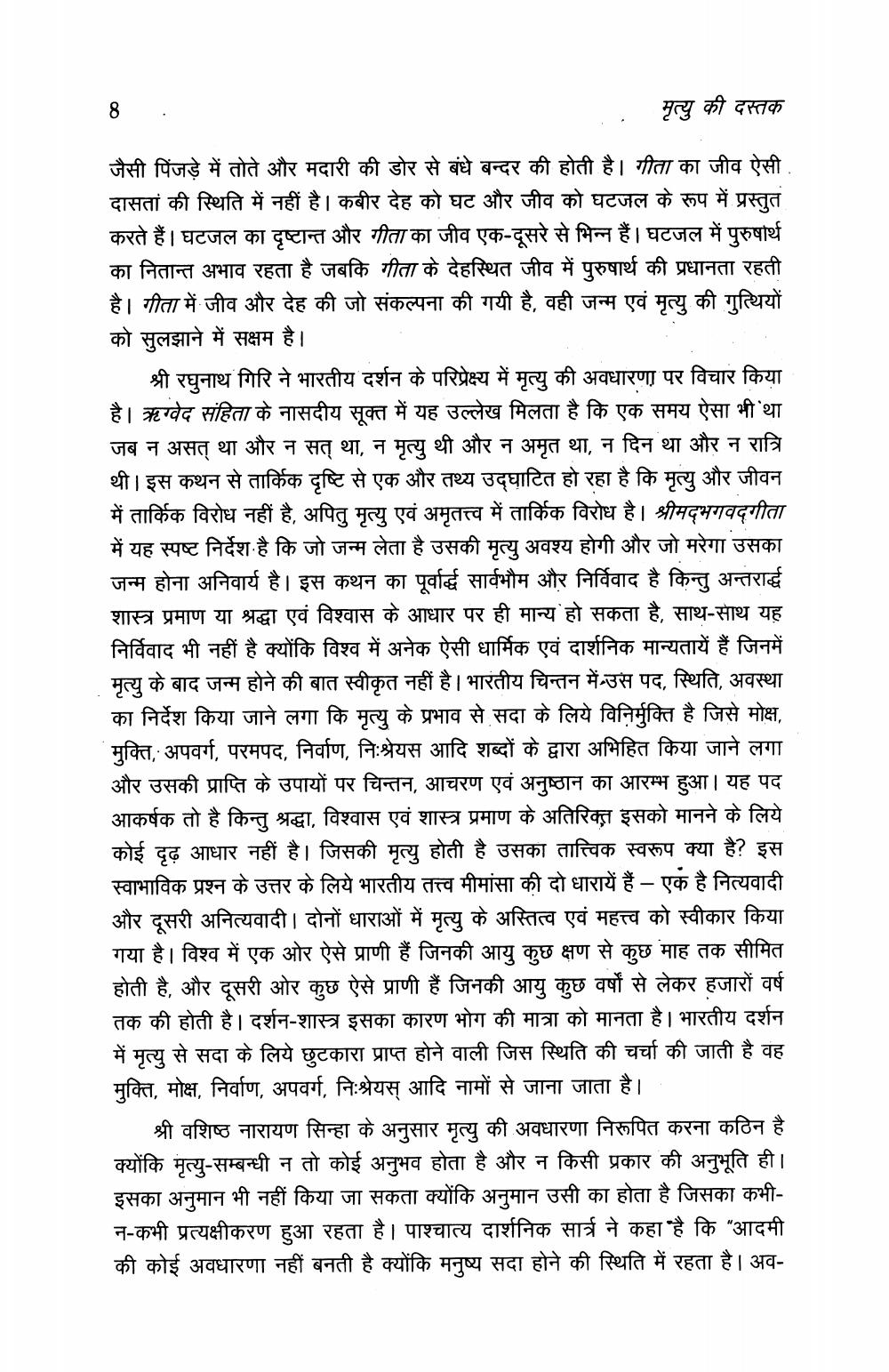________________ 8 . मृत्यु की दस्तक जैसी पिंजड़े में तोते और मदारी की डोर से बंधे बन्दर की होती है। गीता का जीव ऐसी. दासतां की स्थिति में नहीं है। कबीर देह को घट और जीव को घटजल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। घटजल का दृष्टान्त और गीता का जीव एक-दूसरे से भिन्न हैं। घटजल में पुरुषार्थ का नितान्त अभाव रहता है जबकि गीता के देहस्थित जीव में पुरुषार्थ की प्रधानता रहती है। गीता में जीव और देह की जो संकल्पना की गयी है, वही जन्म एवं मृत्यु की गुत्थियों को सुलझाने में सक्षम है। __ श्री रघुनाथ गिरि ने भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में मृत्यु की अवधारणा पर विचार किया है। ऋग्वेद संहिता के नासदीय सूक्त में यह उल्लेख मिलता है कि एक समय ऐसा भी था जब न असत् था और न सत् था, न मृत्यु थी और न अमृत था, न दिन था और न रात्रि थी। इस कथन से तार्किक दृष्टि से एक और तथ्य उद्घाटित हो रहा है कि मृत्यु और जीवन में तार्किक विरोध नहीं है, अपितु मृत्यु एवं अमृतत्त्व में तार्किक विरोध है। श्रीमद्भगवद्गीता में यह स्पष्ट निर्देश है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होगी और जो मरेगा उसका जन्म होना अनिवार्य है। इस कथन का पूर्वार्द्ध सार्वभौम और निर्विवाद है किन्तु अन्तरार्द्ध शास्त्र प्रमाण या श्रद्धा एवं विश्वास के आधार पर ही मान्य हो सकता है, साथ-साथ यह निर्विवाद भी नहीं है क्योंकि विश्व में अनेक ऐसी धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यतायें हैं जिनमें मृत्यु के बाद जन्म होने की बात स्वीकृत नहीं है। भारतीय चिन्तन में उस पद, स्थिति, अवस्था का निर्देश किया जाने लगा कि मृत्यु के प्रभाव से सदा के लिये विनिर्मुक्ति है जिसे मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग, परमपद, निर्वाण, निःश्रेयस आदि शब्दों के द्वारा अभिहित किया जाने लगा और उसकी प्राप्ति के उपायों पर चिन्तन, आचरण एवं अनुष्ठान का आरम्भ हुआ। यह पद आकर्षक तो है किन्तु श्रद्धा, विश्वास एवं शास्त्र प्रमाण के अतिरिक्त इसको मानने के लिये कोई दृढ़ आधार नहीं है। जिसकी मृत्यु होती है उसका तात्त्विक स्वरूप क्या है? इस स्वाभाविक प्रश्न के उत्तर के लिये भारतीय तत्त्व मीमांसा की दो धारायें हैं - एक है नित्यवादी और दूसरी अनित्यवादी। दोनों धाराओं में मत्य के अस्तित्व एवं महत्त्व को स्वीकार किया गया है। विश्व में एक ओर ऐसे प्राणी हैं जिनकी आयु कुछ क्षण से कुछ माह तक सीमित होती है, और दूसरी ओर कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनकी आयु कुछ वर्षों से लेकर हजारों वर्ष तक की होती है। दर्शन-शास्त्र इसका कारण भोग की मात्रा को मानता है। भारतीय दर्शन में मृत्यु से सदा के लिये छुटकारा प्राप्त होने वाली जिस स्थिति की चर्चा की जाती है वह मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, अपवर्ग, निःश्रेयस् आदि नामों से जाना जाता है। श्री वशिष्ठ नारायण सिन्हा के अनुसार मृत्यु की अवधारणा निरूपित करना कठिन है क्योंकि मृत्यु-सम्बन्धी न तो कोई अनुभव होता है और न किसी प्रकार की अनुभूति ही। इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुमान उसी का होता है जिसका कभीन-कभी प्रत्यक्षीकरण हुआ रहता है। पाश्चात्य दार्शनिक सात्र ने कहा है कि “आदमी की कोई अवधारणा नहीं बनती है क्योंकि मनुष्य सदा होने की स्थिति में रहता है। अव