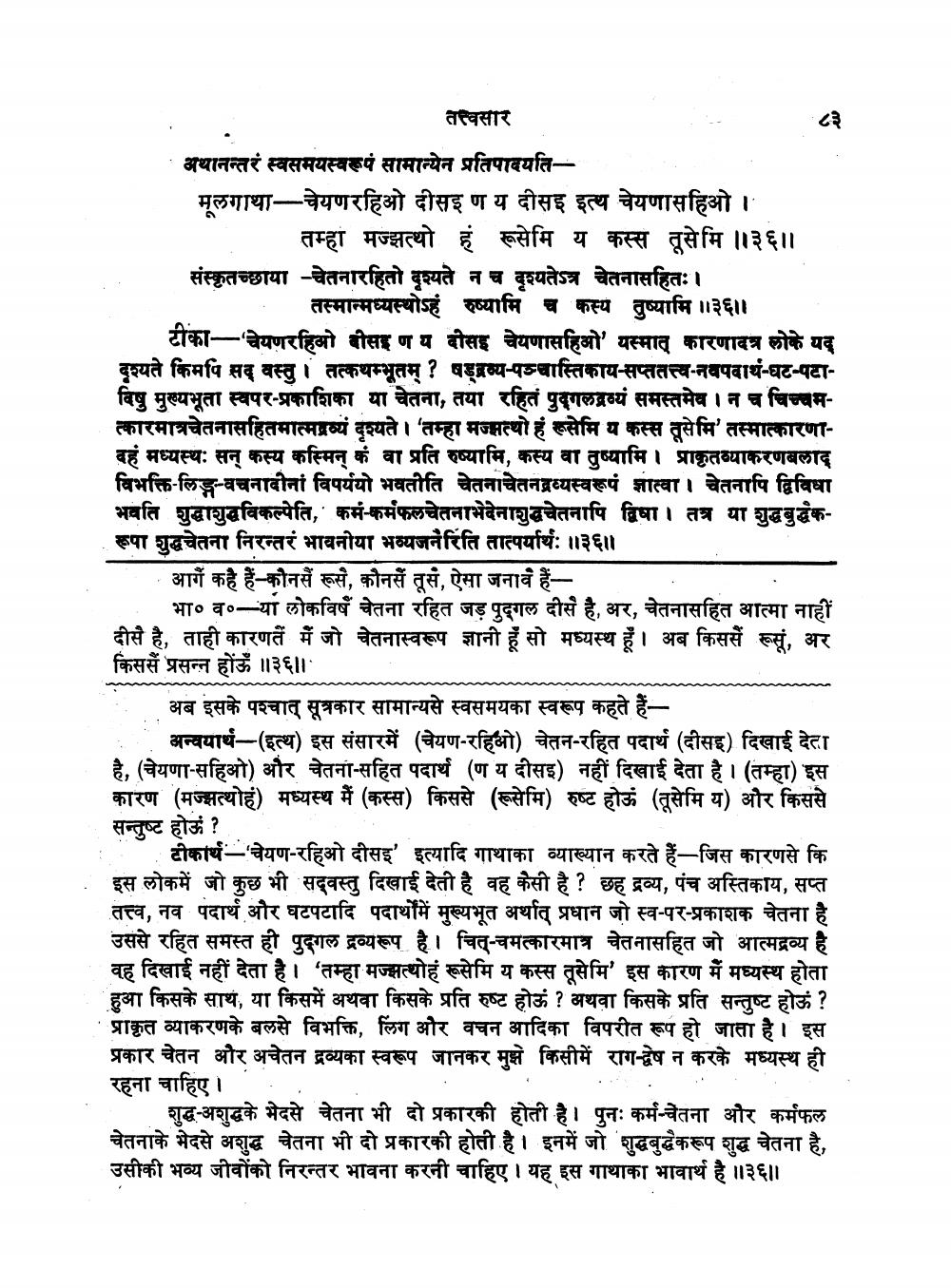________________ तत्त्वसार अथानन्तरं स्वसमयस्वरूपं सामान्येन प्रतिपादयतिमूलगाथा-चेयणरहिओ दीसइ ण य दीसइ इत्थ चेयणासहिओ। तम्हा मज्झत्थो हं रूसेमि य कस्स तूसे मि // 36 // संस्कृतच्छाया -चेतनारहितो दृश्यते न च वृश्यतेऽत्र चेतनासहितः। - तस्मान्मध्यस्थोऽहं रुष्यामि च कस्य तुष्यामि // 36 // टीका-'चेयणरहिओ बीसइण य दोसइ चेयणासहिओ' यस्मात् कारणावत्र लोके यद दृश्यते किमपि सद वस्तु / तत्कथम्भूतम् ? षड्ब्रव्य-पञ्चास्तिकाय-सप्ततत्त्व-नवपदार्थ-घट-पटाविषु मुख्यभूता स्वपर-प्रकाशिका या चेतना, तया रहितं पुद्गलद्रव्यं समस्तमेव / न च चिच्चमकारमात्रचेतनासहितमात्मद्रव्यं दृश्यते। 'तम्हा ममत्थो हं रूसेमि य कस्स तूसेमि' तस्मात्कारणावहं मध्यस्थः सन् कस्य कस्मिन् कं वा प्रति रुष्यामि, कस्य वा तुष्यामि। प्राकृतव्याकरणबलाद् विभक्ति-लिङ्ग-वचनादीनां विपर्ययो भवतीति चेतनाचेतनद्रव्यस्वरूपं ज्ञात्वा। चेतनापि द्विविधा भवति शुद्धाशुद्धविकल्पेति, कर्म-कर्मफलचेतनाभेदेनाशुद्धचेतनापि विषा। तत्र या शुद्धबुद्धकरूपा शुद्धचेतना निरन्तरं भावनोया भव्यजनैरिति तात्पर्यार्थः // 36 // आगें कहै हैं-कौनसैं रूस, कौनसें तूस, ऐसा जनाव हैं___ भा० व०-या लोकविर्षे चेतना रहित जड़ पुद्गल दीसे है, अर, चेतनासहित आत्मा नाहीं दीसै है, ताही कारणते में जो चेतनास्वरूप ज्ञानी हूँ सो मध्यस्थ हूँ। अब किससे रूसूं, अर किससे प्रसन्न होंऊँ // 36 // अब इसके पश्चात् सूत्रकार सामान्यसे स्वसमयका स्वरूप कहते हैं अन्वयार्थ-(इत्थ) इस संसारमें (चेयण-रहिओ) चेतन-रहित पदार्थ (दीसइ) दिखाई देता है, (चेयणा-सहिओ) और चेतना-सहित पदार्थ (ण य दीसइ) नहीं दिखाई देता है / (तम्हा) इस कारण (मज्झत्थोह) मध्यस्थ मैं (कस्स) किससे (रूसेमि) रुष्ट होऊ (तूसेमि य) और किससे सन्तुष्ट होऊ ? टीकार्य-'चेयण-रहिओ दीसइ' इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते हैं जिस कारणसे कि इस लोकमें जो कुछ भी सद्वस्तु दिखाई देती है वह कैसी है ? छह द्रव्य, पंच अस्तिकाय, सप्त तत्त्व, नव पदार्थ और घटपटादि पदार्थोंमें मुख्यभूत अर्थात् प्रधान जो स्व-पर-प्रकाशक चेतना है उससे रहित समस्त ही पुद्गल द्रव्यरूप है। चित्-चमत्कारमात्र चेतनासहित जो आत्मद्रव्य है वह दिखाई नहीं देता है। 'तम्हा मज्झत्योहं रूसेमि य कस्स तूसेमि' इस कारण में मध्यस्थ होता हुआ किसके साथ, या किसमें अथवा किसके प्रति रुष्ट होऊ ? अथवा किसके प्रति सन्तुष्ट होऊ ? प्राकृत व्याकरणके बलसे विभक्ति, लिंग और वचन आदिका विपरीत रूप हो जाता है। इस प्रकार चेतन और अचेतन द्रव्यका स्वरूप जानकर मुझे किसीमें राग-द्वेष न करके मध्यस्थ ही रहना चाहिए। शुद्ध-अशुद्धके भेदसे चेतना भी दो प्रकारकी होती है। पुनः कर्म-चेतना और कर्मफल चेतनाके भेदसे अशुद्ध चेतना भी दो प्रकारकी होती है। इनमें जो शुद्धबुद्धकरूप शुद्ध चेतना है, उसीकी भव्य जीवोंको निरन्तर भावना करनी चाहिए। यह इस गाथाका भावार्थ है // 36 //