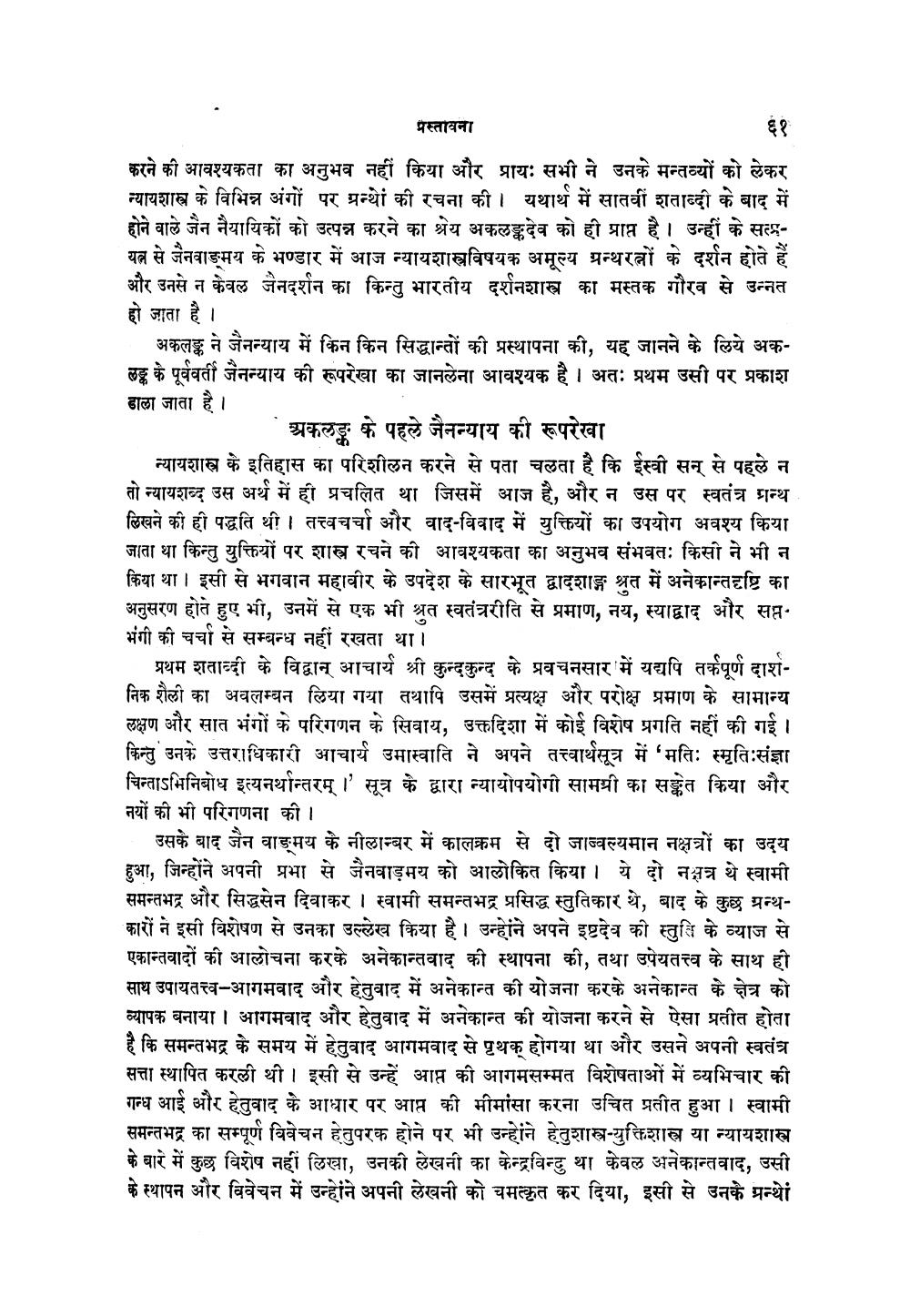________________ प्रस्तावना 61 करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया और प्रायः सभी ने उनके मन्तव्यों को लेकर न्यायशास्त्र के विभिन्न अंगों पर ग्रन्थों की रचना की। यथार्थ में सातवीं शताब्दी के बाद में होने वाले जैन नैयायिकों को उत्पन्न करने का श्रेय अकलङ्कदेव को ही प्राप्त है। उन्हीं के सत्मयत्न से जैनवाङ्मय के भण्डार में आज न्यायशास्त्रविषयक अमूल्य ग्रन्थरत्नों के दर्शन होते हैं और उनसे न केवल जैनदर्शन का किन्तु भारतीय दर्शनशास्त्र का मस्तक गौरव से उन्नत हो जाता है / ___ अकलङ्क ने जैनन्याय में किन किन सिद्धान्तों की प्रस्थापना की, यह जानने के लिये अकलङ्क के पूर्ववर्ती जैनन्याय की रूपरेखा का जानलेना आवश्यक है / अतः प्रथम उसी पर प्रकाश डाला जाता है। अकल के पहले जैनन्याय की रूपरेखा न्यायशास्त्र के इतिहास का परिशीलन करने से पता चलता है कि ईस्वी सन् से पहले न तो न्यायशब्द उस अर्थ में ही प्रचलित था जिसमें आज है, और न उस पर स्वतंत्र ग्रन्थ लिखने की ही पद्धति थी। तत्त्वचर्चा और वाद-विवाद में युक्तियों का उपयोग अवश्य किया जाता था किन्तु युक्तियों पर शास्त्र रचने की आवश्यकता का अनुभव संभवतः किसी ने भी न किया था। इसी से भगवान महावीर के उपदेश के सारभूत द्वादशाङ्ग श्रुत में अनेकान्तदृष्टि का अनुसरण होते हुए भी, उनमें से एक भी श्रुत स्वतंत्ररीति से प्रमाण, नय, स्याद्वाद और सप्त. भंगी की चर्चा से सम्बन्ध नहीं रखता था। प्रथम शताब्दी के विद्वान् आचार्य श्री कुन्दकुन्द के प्रवचनसार में यद्यपि तर्कपूर्ण दार्शनिक शैली का अवलम्बन लिया गया तथापि उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के सामान्य लक्षण और सात भंगों के परिगणन के सिवाय, उक्तदिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की गई / किन्तु उनके उत्तराधिकारी आचार्य उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थसूत्र में 'मतिः स्मृतिःसंज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनान्तरम् / ' सूत्र के द्वारा न्यायोपयोगी सामग्री का सङ्केत किया और नयों की भी परिगणना की। उसके बाद जैन वाङ्मय के नीलान्बर में कालक्रम से दो जाज्वल्यमान नक्षत्रों का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी प्रभा से जैनवाड़मय को आलोकित किया। ये दो नक्षत्र थे स्वामी समन्तभद्र और सिद्धसेन दिवाकर / स्वामी समन्तभद्र प्रसिद्ध स्तुतिकार थे, बाद के कुछ ग्रन्थकारों ने इसी विशेषण से उनका उल्लेख किया है। उन्होंने अपने इष्टदेव की स्तुति के व्याज से एकान्तवादों की आलोचना करके अनेकान्तवाद की स्थापना की, तथा उपेयतत्त्व के साथ ही साथ उपायतत्त्व-आगमवाद और हेतुवाद में अनेकान्त की योजना करके अनेकान्त के क्षेत्र को व्यापक बनाया। आगमवाद और हेतुवाद में अनेकान्त की योजना करने से ऐसा प्रतीत होता है कि समन्तभद्र के समय में हेतुवाद आगमवाद से पृथक् होगया था और उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करली थी। इसी से उन्हें आप्त की आगमसम्मत विशेषताओं में व्यभिचार की गन्ध आई और हेतुवाद के आधार पर आप्त की मीमांसा करना उचित प्रतीत हुआ। स्वामी समन्तभद्र का सम्पूर्ण विवेचन हेतुपरक होने पर भी उन्होंने हेतुशास्त्र-युक्तिशास्त्र या न्यायशास्त्र के बारे में कुछ विशेष नहीं लिखा, उनकी लेखनी का केन्द्रविन्दु था केवल अनेकान्तवाद, उसी के स्थापन और विवेचन में उन्होंने अपनी लेखनी को चमत्कृत कर दिया, इसी से उनके ग्रन्थों