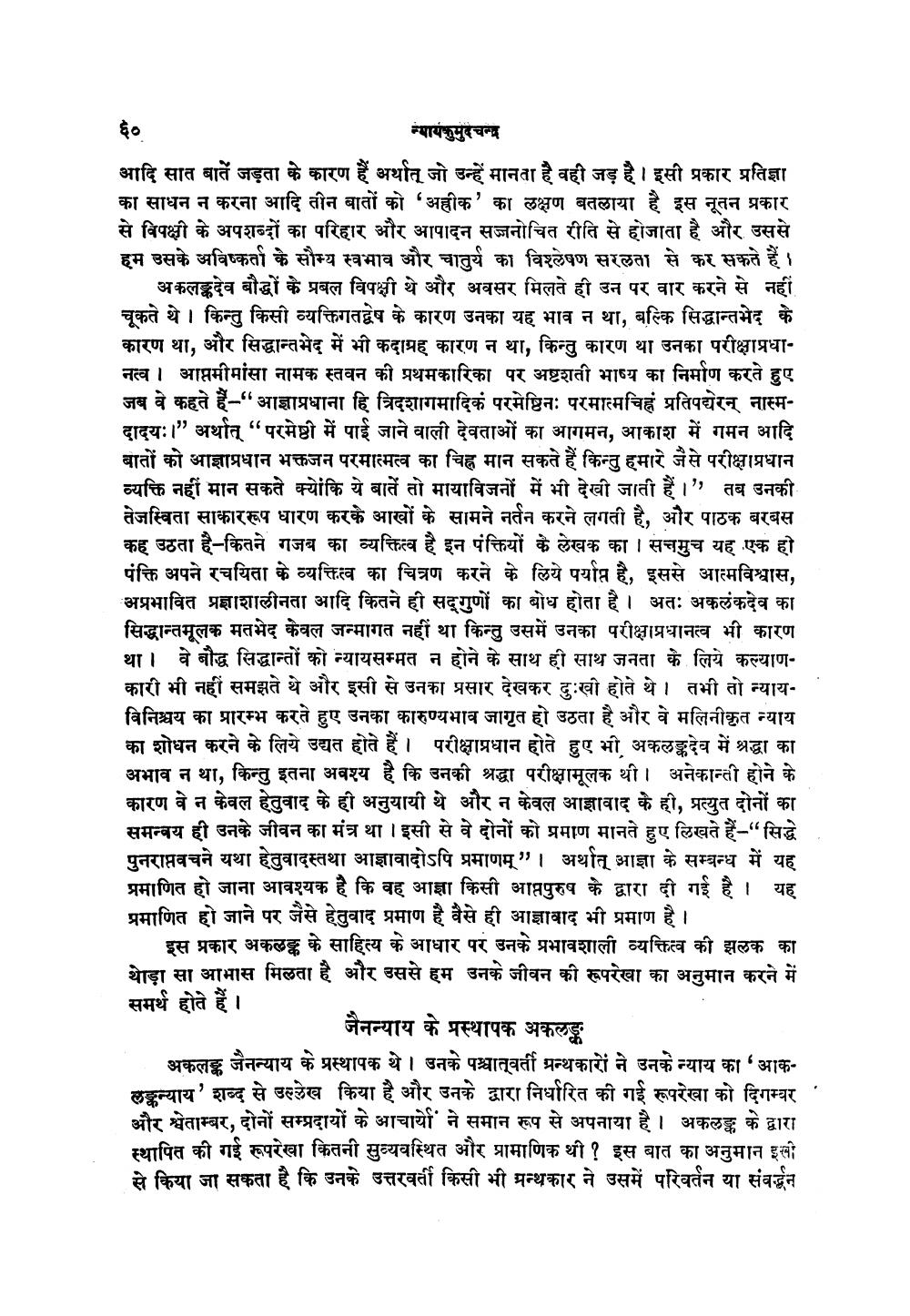________________ 60 न्यायकुमुदचन्द्र आदि सात बातें जड़ता के कारण हैं अर्थात् जो उन्हें मानता है वही जड़ है। इसी प्रकार प्रतिज्ञा का साधन न करना आदि तीन बातों को 'अत्रीक' का लक्षण बतलाया है इस नूतन प्रकार से विपक्षी के अपशब्दों का परिहार और आपादन सज्जनोचित रीति से होजाता है और उससे हम उसके अविष्कर्ता के सौम्य स्वभाव और चातुर्य का विश्लेषण सरलता से कर सकते हैं। अकलङ्कदेव बौद्धों के प्रबल विपक्षी थे और अवसर मिलते ही उन पर वार करने से नहीं चूकते थे। किन्तु किसी व्यक्तिगतद्वेष के कारण उनका यह भाव न था, बल्कि सिद्धान्तभेद के कारण था, और सिद्धान्तभेद में भी कदाग्रह कारण न था, किन्तु कारण था उनका परीक्षाप्रधानत्व / आप्तमीमांसा नामक स्तवन की प्रथमकारिका पर अष्टशती भाष्य का निर्माण करते हुए जब वे कहते हैं-"आज्ञाप्रधाना हि त्रिदशागमादिकं परमेष्ठिनः परमात्मचिह्न प्रतिपद्यरन् नास्मदादयः।" अर्थात् “परमेष्ठी में पाई जाने वाली देवताओं का आगमन, आकाश में गमन आदि बातों को आज्ञाप्रधान भक्तजन परमात्मत्व का चिह्न मान सकते हैं किन्तु हमारे जैसे परीक्षाप्रधान व्यक्ति नहीं मान सकते क्योंकि ये बातें तो मायाविजनों में भी देखी जाती हैं।' तब उनकी तेजस्विता साकाररूप धारण करके आखों के सामने नर्तन करने लगती है, और पाठक बरबस कह उठता है-कितने गजब का व्यक्तित्व है इन पंक्तियों के लेखक का / सचमुच यह एक हो पंक्ति अपने रचयिता के व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिये पर्याप्त है, इससे आत्मविश्वास, अप्रभावित प्रज्ञाशालीनता आदि कितने ही सद्गुणों का बोध होता है। अतः अकलंकदेव का सिद्धान्तमूलक मतभेद केवल जन्मागत नहीं था किन्तु उसमें उनका परीक्षाप्रधानत्व भी कारण था। वे नौद्ध सिद्धान्तों को न्यायसम्मत न होने के साथ ही साथ जनता के लिये कल्याणकारी भी नहीं समझते थे और इसी से उनका प्रसार देखकर दुःखी होते थे। तभी तो न्यायविनिश्चय का प्रारम्भ करते हुए उनका कारुण्यभाव जागृत हो उठता है और वे मलिनीकृत न्याय का शोधन करने के लिये उद्यत होते हैं। परीक्षाप्रधान होते हुए भी अकलङ्कदेव में श्रद्धा का अभाव न था, किन्तु इतना अवश्य है कि उनकी श्रद्धा परीक्षामूलक थी। अनेकान्ती होने के कारण वे न केवल हेतुवाद के ही अनुयायी थे और न केवल आज्ञावाद के ही, प्रत्युत दोनों का समन्वय ही उनके जीवन का मंत्र था / इसी से वे दोनों को प्रमाण मानते हुए लिखते हैं-"सिद्धे पुनराप्तवचने यथा हेतुवादस्तथा आज्ञावादोऽपि प्रमाणम्"। अर्थात् आज्ञा के सम्बन्ध में यह प्रमाणित हो जाना आवश्यक है कि वह आज्ञा किसी आप्तपुरुष के द्वारा दी गई है। यह प्रमाणित हो जाने पर जैसे हेतुवाद प्रमाण है वैसे ही आज्ञावाद भी प्रमाण है। इस प्रकार अकलङ्क के साहित्य के आधार पर उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की झलक का थोड़ा सा आभास मिलता है और उससे हम उनके जीवन की रूपरेखा का अनुमान करने में समर्थ होते है। जैनन्याय के प्रस्थापक अकलङ्क अकलङ्क जैनन्याय के प्रस्थापक थे। उनके पश्चात्वर्ती ग्रन्थकारों ने उनके न्याय का 'आकलकन्याय' शब्द से उल्लेख किया है और उनके द्वारा निर्धारित की गई रूपरेखा को दिगम्बर और श्वेताम्बर, दोनों सम्प्रदायों के आचार्यों ने समान रूप से अपनाया है। अकलङ्क के द्वारा स्थापित की गई रूपरेखा कितनी सुव्यवस्थित और प्रामाणिक थी ? इस बात का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि उनके उत्तरवर्ती किसी भी ग्रन्थकार ने उसमें परिवर्तन या संवर्द्धन