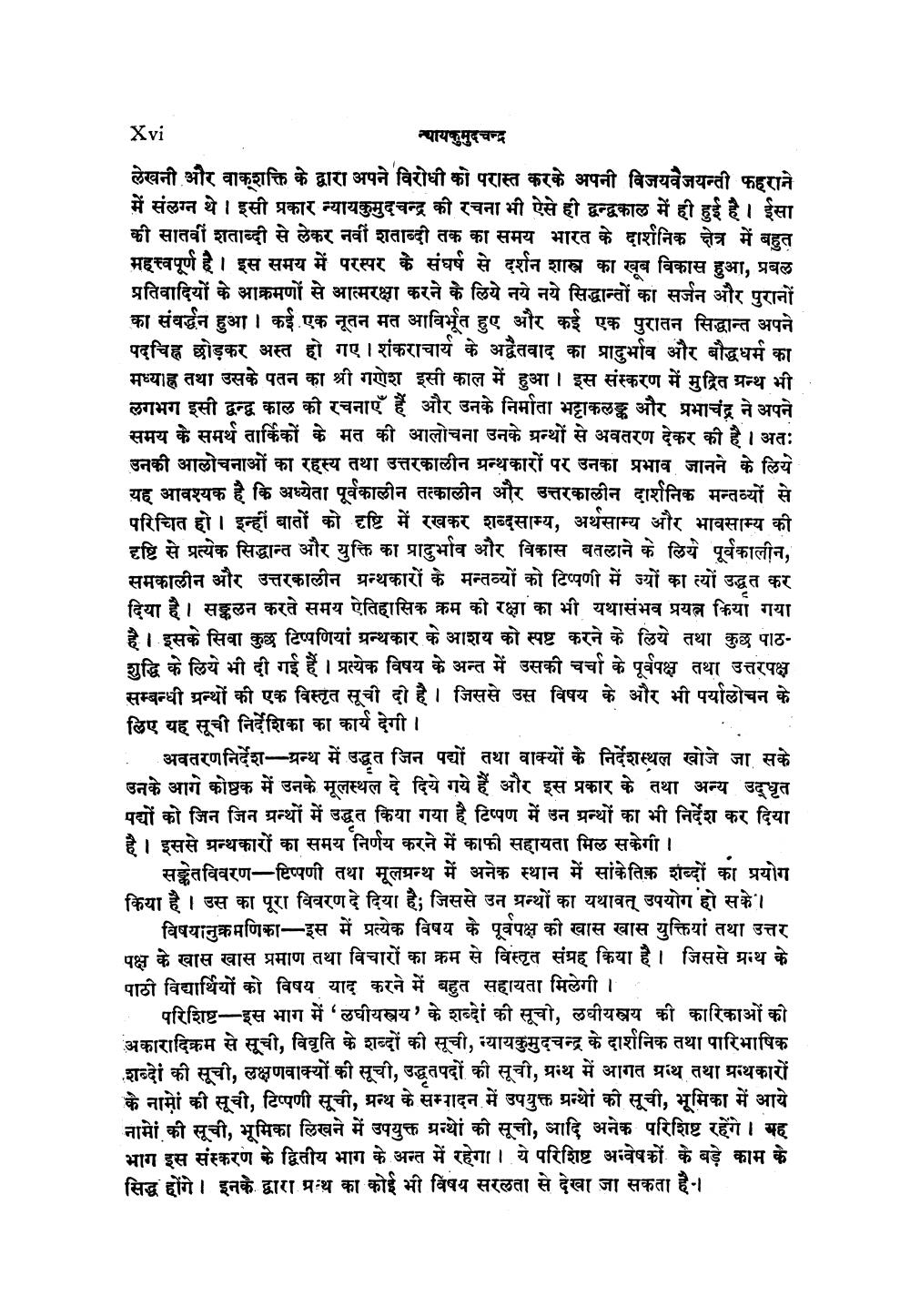________________ Xvi न्यायकुमुदचन्द्र लेखनी और वाकशक्ति के द्वारा अपने विरोधी को परास्त करके अपनी विजयवैजयन्ती फहराने में संलग्न थे / इसी प्रकार न्यायकुमुदचन्द्र की रचना भी ऐसे ही द्वन्द्वकाल में ही हुई है। ईसा की सातवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक का समय भारत के दार्शनिक क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस समय में परस्पर के संघर्ष से दर्शन शास्त्र का खूब विकास हुआ, प्रबल प्रतिवादियों के आक्रमणों से आत्मरक्षा करने के लिये नये नये सिद्धान्तों का सर्जन और पुरानों का संवर्द्धन हुआ। कई एक नूतन मत आविर्भूत हुए और कई एक पुरातन सिद्धान्त अपने पदचिह्न छोड़कर अस्त हो गए / शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रादुर्भाव और बौद्धधर्म का मध्याह्न तथा उसके पतन का श्री गणेश इसी काल में हुआ। इस संस्करण में मुद्रित ग्रन्थ भी लगभग इसी द्वन्द्व काल की रचनाएँ हैं और उनके निर्माता भट्टाकलङ्क और प्रभाचंद्र ने अपने समय के समर्थ तार्किकों के मत की आलोचना उनके ग्रन्थों से अवतरण देकर की है। अतः उनकी आलोचनाओं का रहस्य तथा उत्तरकालीन ग्रन्थकारों पर उनका प्रभाव जानने के लिये यह आवश्यक है कि अध्येता पूर्वकालीन तत्कालीन और उत्तरकालीन दार्शनिक मन्तव्यों से परिचित हो। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर शब्दसाम्य, अर्थसाम्य और भावसाम्य की दृष्टि से प्रत्येक सिद्धान्त और युक्ति का प्रादुर्भाव और विकास बतलाने के लिये पूर्वकालीन, समकालीन और उत्तरकालीन ग्रन्थकारों के मन्तव्यों को टिप्पणी में ज्यों का त्यों उद्धत कर दिया है। सङ्कलन करते समय ऐतिहासिक क्रम को रक्षा का भी यथासंभव प्रयत्न किया गया है। इसके सिवा कुछ टिप्पणियां ग्रन्थकार के आशय को स्पष्ट करने के लिये तथा कुछ पाठशुद्धि के लिये भी दी गई हैं / प्रत्येक विषय के अन्त में उसकी चर्चा के पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष सम्बन्धी ग्रन्थों की एक विस्तृत सूची दी है। जिससे उस विषय के और भी पर्यालोचन के लिए यह सूची निर्देशिका का कार्य देगी। . अवतरणनिर्देश-ग्रन्थ में उद्धृत जिन पद्यों तथा वाक्यों के निर्देशस्थल खोजे जा सके उनके आगे कोष्ठक में उनके मूलस्थल दे दिये गये हैं और इस प्रकार के तथा अन्य उद्धृत पद्यों को जिन जिन ग्रन्थों में उद्धत किया गया है टिप्पण में उन ग्रन्थों का भी निर्देश कर दिया है। इससे ग्रन्थकारों का समय निर्णय करने में काफी सहायता मिल सकेगी। सङ्केतविवरण-टिप्पणी तथा मूलग्रन्थ में अनेक स्थान में सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है / उस का पूरा विवरण दे दिया है। जिससे उन ग्रन्थों का यथावत् उपयोग हो सके। विषयानुक्रमणिका-इस में प्रत्येक विषय के पूर्वपक्ष की खास खास युक्तियां तथा उत्तर पक्ष के खास खास प्रमाण तथा विचारों का क्रम से विस्तृत संग्रह किया है। जिससे ग्रन्थ के पाठी विद्यार्थियों को विषय याद करने में बहुत सहायता मिलेगी। परिशिष्ट-इस भाग में 'लघीयस्त्रय' के शब्दों की सूची, लघीयत्रय की कारिकाओं को अकारादिक्रम से सूची, विवृति के शब्दों की सूची, न्यायकुमुदचन्द्र के दार्शनिक तथा पारिभाषिक शब्दों की सूची, लक्षणवाक्यों की सूची, उद्धृतपदों की सूची, ग्रन्थ में आगत ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारों के नामों की सूची, टिप्पणी सूची, ग्रन्थ के सम्पादन में उपयुक्त ग्रन्थों की सूची, भूमिका में आये नामों की सूची, भूमिका लिखने में उपयुक्त ग्रन्थों की सूची, आदि अनेक परिशिष्ट रहेंगे। यह भाग इस संस्करण के द्वितीय भाग के अन्त में रहेगा। ये परिशिष्ट अन्वेषकों के बड़े काम के सिद्ध होंगे। इनके द्वारा प्रस्थ का कोई भी विषय सरलता से देखा जा सकता है।