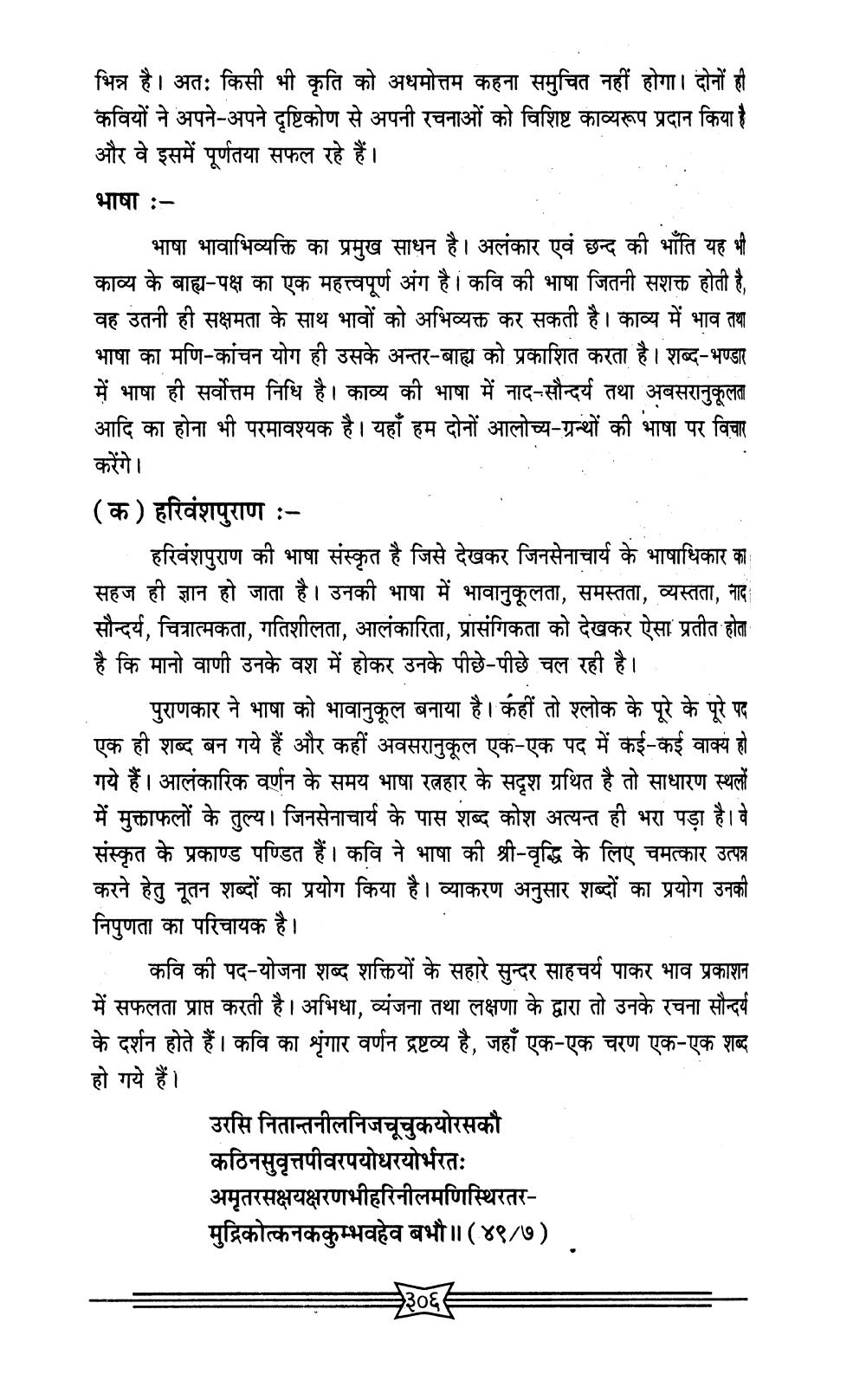________________ भिन्न है। अतः किसी भी कृति को अधमोत्तम कहना समुचित नहीं होगा। दोनों ही कवियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से अपनी रचनाओं को विशिष्ट काव्यरूप प्रदान किया है और वे इसमें पूर्णतया सफल रहे हैं। भाषा : भाषा भावाभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। अलंकार एवं छन्द की भाँति यह भी काव्य के बाह्य-पक्ष का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। कवि की भाषा जितनी सशक्त होती है, वह उतनी ही सक्षमता के साथ भावों को अभिव्यक्त कर सकती है। काव्य में भाव तथा भाषा का मणि-कांचन योग ही उसके अन्तर-बाह्य को प्रकाशित करता है। शब्द-भण्डार में भाषा ही सर्वोत्तम निधि है। काव्य की भाषा में नाद-सौन्दर्य तथा अबसरानुकूलता आदि का होना भी परमावश्यक है। यहाँ हम दोनों आलोच्य-ग्रन्थों की भाषा पर विचार करेंगे। (क) हरिवंशपुराण :____ हरिवंशपुराण की भाषा संस्कृत है जिसे देखकर जिनसेनाचार्य के भाषाधिकार का सहज ही ज्ञान हो जाता है। उनकी भाषा में भावानुकूलता, समस्तता, व्यस्तता, नाद सौन्दर्य, चित्रात्मकता, गतिशीलता, आलंकारिता, प्रासंगिकता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वाणी उनके वश में होकर उनके पीछे-पीछे चल रही है। पुराणकार ने भाषा को भावानुकूल बनाया है। कहीं तो श्लोक के पूरे के पूरे पद एक ही शब्द बन गये हैं और कहीं अवसरानुकूल एक-एक पद में कई-कई वाक्य हो गये हैं। आलंकारिक वर्णन के समय भाषा रत्नहार के सदृश ग्रथित है तो साधारण स्थलों में मुक्ताफलों के तुल्य। जिनसेनाचार्य के पास शब्द कोश अत्यन्त ही भरा पड़ा है। वे संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित हैं। कवि ने भाषा की श्री-वृद्धि के लिए चमत्कार उत्पन्न करने हेतु नूतन शब्दों का प्रयोग किया है। व्याकरण अनुसार शब्दों का प्रयोग उनकी निपुणता का परिचायक है। कवि की पद-योजना शब्द शक्तियों के सहारे सुन्दर साहचर्य पाकर भाव प्रकाशन में सफलता प्राप्त करती है। अभिधा, व्यंजना तथा लक्षणा के द्वारा तो उनके रचना सौन्दर्य के दर्शन होते हैं। कवि का श्रृंगार वर्णन द्रष्टव्य है, जहाँ एक-एक चरण एक-एक शब्द हो गये हैं। उरसि नितान्तनीलनिजचूचुकयोरसको कठिनसुवृत्तपीवरपयोधरयोर्भरतः अमृतरसक्षयक्षरणभीहरिनीलमणिस्थिरतरमुद्रिकोत्कनककुम्भवहेव बभौ॥(४९/७) ..