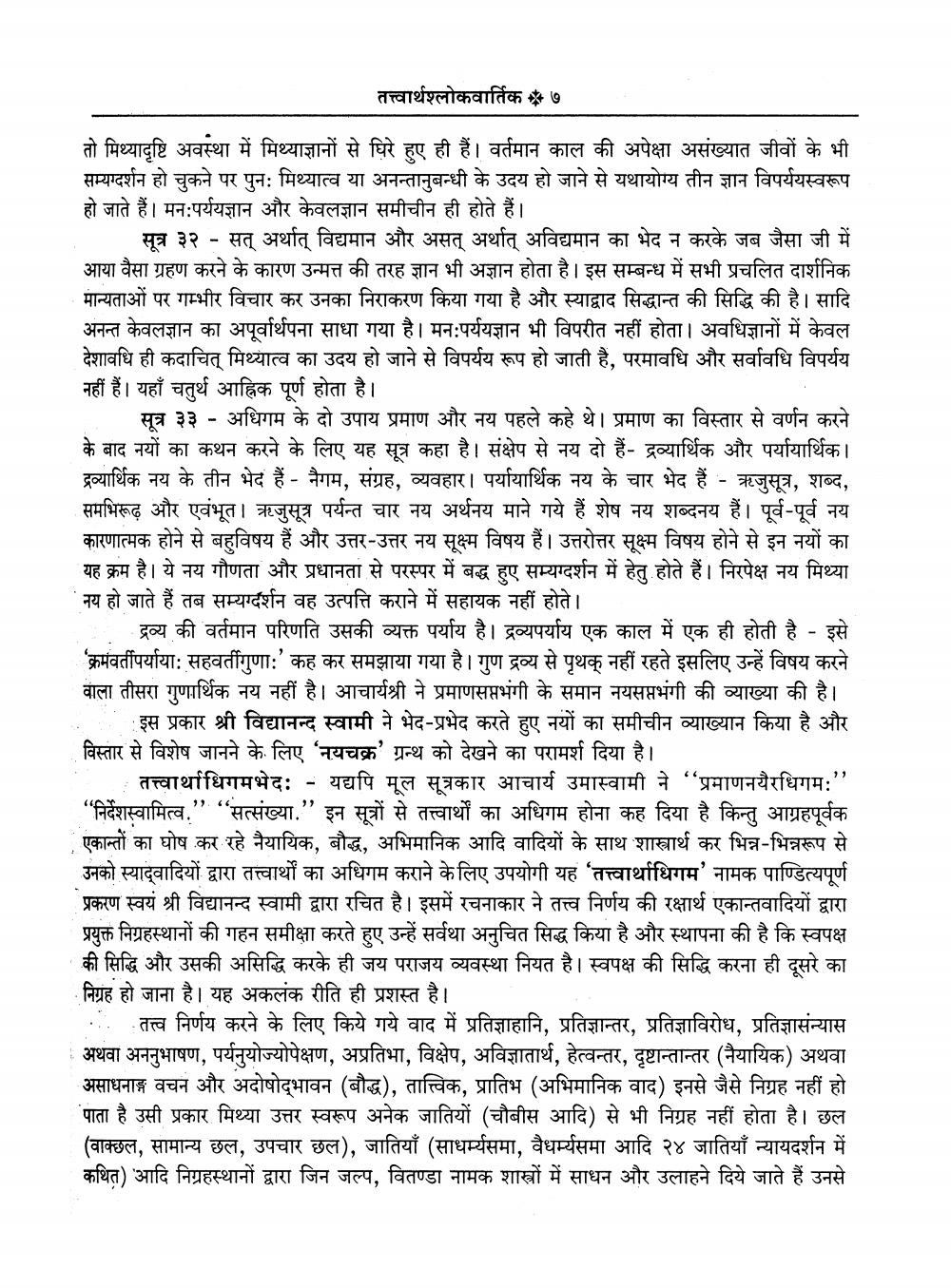________________ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक*७ तो मिथ्यादृष्टि अवस्था में मिथ्याज्ञानों से घिरे हुए ही हैं। वर्तमान काल की अपेक्षा असंख्यात जीवों के भी सम्यग्दर्शन हो चुकने पर पुनः मिथ्यात्व या अनन्तानुबन्धी के उदय हो जाने से यथायोग्य तीन ज्ञान विपर्ययस्वरूप हो जाते हैं। मन:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान समीचीन ही होते हैं। सूत्र 32 - सत् अर्थात् विद्यमान और असत् अर्थात् अविद्यमान का भेद न करके जब जैसा जी में आया वैसा ग्रहण करने के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान होता है। इस सम्बन्ध में सभी प्रचलित दार्शनिक मान्यताओं पर गम्भीर विचार कर उनका निराकरण किया गया है और स्याद्वाद सिद्धान्त की सिद्धि की है। सादि अनन्त केवलज्ञान का अपूर्वार्थपना साधा गया है। मन:पर्ययज्ञान भी विपरीत नहीं होता। अवधिज्ञानों में केवल देशावधि ही कदाचित् मिथ्यात्व का उदय हो जाने से विपर्यय रूप हो जाती हैं, परमावधि और सर्वावधि विपर्यय नहीं हैं। यहाँ चतुर्थ आह्निक पूर्ण होता है। सूत्र 33 - अधिगम के दो उपाय प्रमाण और नय पहले कहे थे। प्रमाण का विस्तार से वर्णन करने के बाद नयों का कथन करने के लिए यह सूत्र कहा है। संक्षेप से नय दो हैं- द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक / व्यार्थिक नय के तीन भेद हैं - नैगम, संग्रह, व्यवहार। पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं - ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत। ऋजुसूत्र पर्यन्त चार नय अर्थनय माने गये हैं शेष नय शब्दनय हैं। पूर्व-पूर्व नय कारणात्मक होने से बहुविषय हैं और उत्तर-उत्तर नय सूक्ष्म विषय हैं। उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय होने से इन नयों का यह क्रम है। प्रय गौणता और प्रधानता से परस्पर में बद्ध हुए सम्यग्दर्शन में हेतु होते हैं। निरपेक्ष नय मिथ्या नय हो जाते हैं तब सम्यग्दर्शन वह उत्पत्ति कराने में सहायक नहीं होते। द्रव्य की वर्तमान परिणति उसकी व्यक्त पर्याय है। द्रव्यपर्याय एक काल में एक ही होती है - इसे 'क्रमवर्तीपर्यायाः सहवर्तीगुणाः' कह कर समझाया गया है। गुण द्रव्य से पृथक् नहीं रहते इसलिए उन्हें विषय करने वाला तीसरा गुणार्थिक नय नहीं है। आचार्यश्री ने प्रमाणसप्तभंगी के समान नयसप्तभंगी की व्याख्या की है। इस प्रकार श्री विद्यानन्द स्वामी ने भेद-प्रभेद करते हए नयों का समीचीन व्याख्यान किया है और विस्तार से विशेष जानने के लिए 'नयचक्र' ग्रन्थ को देखने का परामर्श दिया है। तत्त्वार्थाधिगमभेदः - यद्यपि मूल सूत्रकार आचार्य उमास्वामी ने “प्रमाणनयैरधिगमः' “निर्देशस्वामित्व." “सत्संख्या." इन सूत्रों से तत्त्वार्थों का अधिगम होना कह दिया है किन्तु आग्रहपूर्वक एकान्तों का घोष कर रहे नैयायिक, बौद्ध, अभिमानिक आदि वादियों के साथ शास्त्रार्थ कर भिन्न-भिन्नरूप से उनको स्याद्वादियों द्वारा तत्त्वार्थों का अधिगम कराने के लिए उपयोगी यह 'तत्त्वार्थाधिगम' नामक पाण्डित्यपूर्ण प्रकरण स्वयं श्री विद्यानन्द स्वामी द्वारा रचित है। इसमें रचनाकार ने तत्त्व निर्णय की रक्षार्थ एकान्तवादियों द्वारा प्रयुक्त निग्रहस्थानों की गहन समीक्षा करते हुए उन्हें सर्वथा अनुचित सिद्ध किया है और स्थापना की है कि स्वपक्ष की सिद्धि और उसकी असिद्धि करके ही जय पराजय व्यवस्था नियत है। स्वपक्ष की सिद्धि करना ही दूसरे का निग्रह हो जाना है। यह अकलंक रीति ही प्रशस्त है। ... तत्त्व निर्णय करने के लिए किये गये वाद में प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञासंन्यास अथवा अननुभाषण, पर्यनुयोज्योपेक्षण, अप्रतिभा, विक्षेप, अविज्ञातार्थ, हेत्वन्तर, दृष्टान्तान्तर (नैयायिक) अथवा असाधनाङ्ग वचन और अदोषोद्भावन (बौद्ध), तात्त्विक, प्रातिभ (अभिमानिक वाद) इनसे जैसे निग्रह नहीं हो पाता है उसी प्रकार मिथ्या उत्तर स्वरूप अनेक जातियों (चौबीस आदि) से भी निग्रह नहीं होता है। छल (वाक्छल, सामान्य छल, उपचार छल), जातियाँ (साधर्म्यसमा, वैधर्म्यसमा आदि 24 जातियाँ न्यायदर्शन में कथित) आदि निग्रहस्थानों द्वारा जिन जल्प, वितण्डा नामक शास्त्रों में साधन और उलाहने दिये जाते हैं उनसे