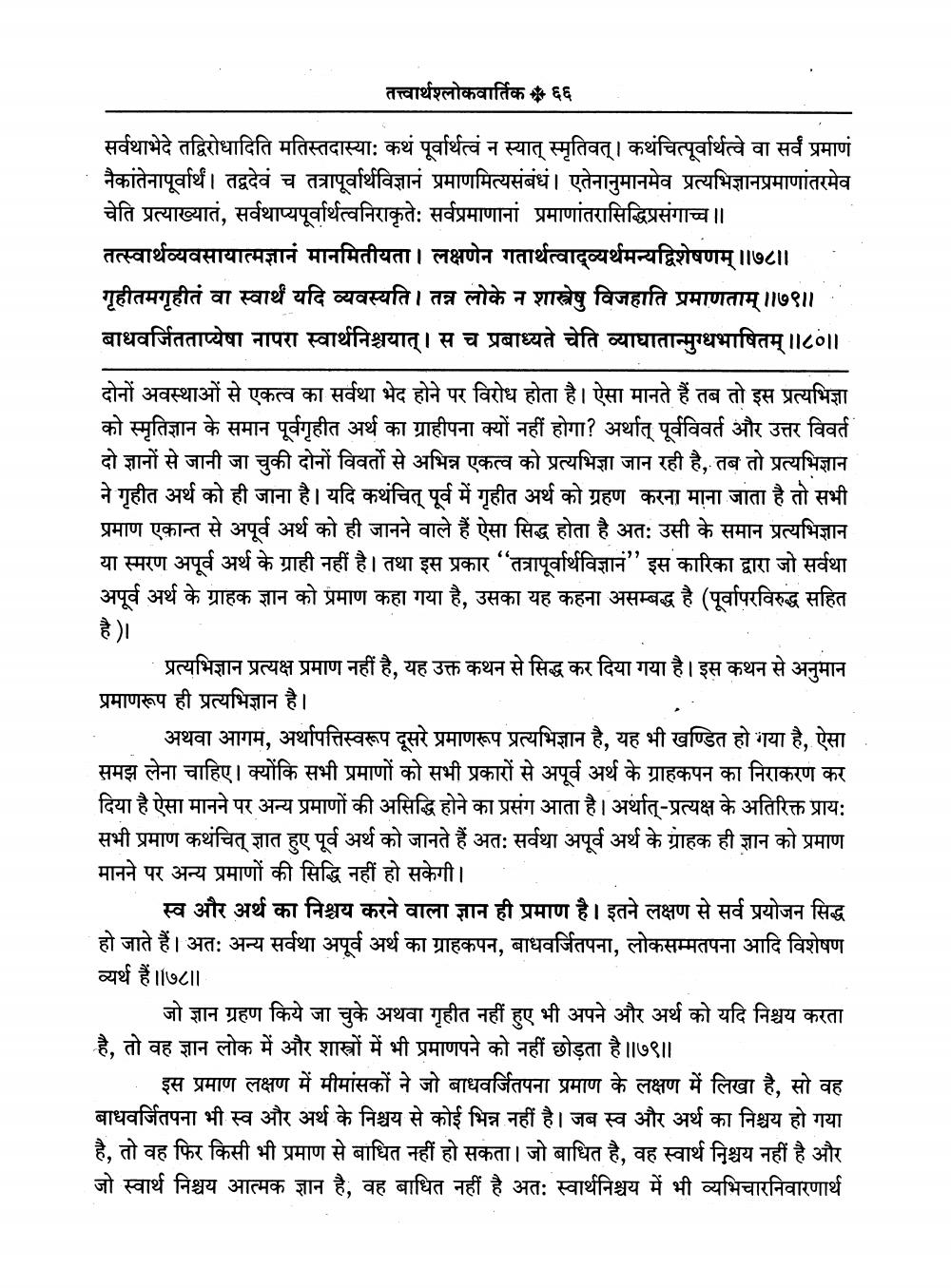________________ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक 66 सर्वथाभेदे तद्विरोधादिति मतिस्तदास्याः कथं पूर्वार्थत्वं न स्यात् स्मृतिवत्। कथंचित्पूर्वार्थत्वे वा सर्वं प्रमाणं नैकांतेनापूर्वार्थं / तद्वदेवं च तत्रापूर्वार्थविज्ञानं प्रमाणमित्यसंबंध। एतेनानुमानमेव प्रत्यभिज्ञानप्रमाणांतरमेव चेति प्रत्याख्यातं, सर्वथाप्यपूर्वार्थत्वनिराकृतेः सर्वप्रमाणानां प्रमाणांतरासिद्धिप्रसंगाच्च / तत्स्वार्थव्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता। लक्षणेन गतार्थत्वाद्व्यर्थमन्यद्विशेषणम् // 7 // गृहीतमगृहीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति / तन्न लोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम् // 79 // बाधवर्जितताप्येषा नापरा स्वार्थनिश्चयात्। स च प्रबाध्यते चेति व्याघातान्मुग्धभाषितम् // 8 // दोनों अवस्थाओं से एकत्व का सर्वथा भेद होने पर विरोध होता है। ऐसा मानते हैं तब तो इस प्रत्यभिज्ञा को स्मृतिज्ञान के समान पूर्वगृहीत अर्थ का ग्राहीपना क्यों नहीं होगा? अर्थात् पूर्वविवर्त और उत्तर विवर्त दो ज्ञानों से जानी जा चुकी दोनों विवर्तो से अभिन्न एकत्व को प्रत्यभिज्ञा जान रही है, तब तो प्रत्यभिज्ञान ने गृहीत अर्थ को ही जाना है। यदि कथंचित् पूर्व में गृहीत अर्थ को ग्रहण करना माना जाता है तो सभी प्रमाण एकान्त से अपूर्व अर्थ को ही जानने वाले हैं ऐसा सिद्ध होता है अत: उसी के समान प्रत्यभिज्ञान या स्मरण अपूर्व अर्थ के ग्राही नहीं है। तथा इस प्रकार "तत्रापूर्वार्थविज्ञानं" इस कारिका द्वारा जो सर्वथा अपूर्व अर्थ के ग्राहक ज्ञान को प्रमाण कहा गया है, उसका यह कहना असम्बद्ध है (पूर्वापरविरुद्ध सहित प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, यह उक्त कथन से सिद्ध कर दिया गया है। इस कथन से अनुमान प्रमाणरूप ही प्रत्यभिज्ञान है। अथवा आगम, अर्थापत्तिस्वरूप दूसरे प्रमाणरूप प्रत्यभिज्ञान है, यह भी खण्डित हो गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि सभी प्रमाणों को सभी प्रकारों से अपूर्व अर्थ के ग्राहकपन का निराकरण कर दिया है ऐसा मानने पर अन्य प्रमाणों की असिद्धि होने का प्रसंग आता है। अर्थात्-प्रत्यक्ष के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रमाण कथंचित् ज्ञात हुए पूर्व अर्थ को जानते हैं अतः सर्वथा अपूर्व अर्थ के ग्राहक ही ज्ञान को प्रमाण मानने पर अन्य प्रमाणों की सिद्धि नहीं हो सकेगी। स्व और अर्थ का निश्चय करने वाला ज्ञान ही प्रमाण है। इतने लक्षण से सर्व प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अत: अन्य सर्वथा अपूर्व अर्थ का ग्राहकपन, बाधवर्जितपना, लोकसम्मतपना आदि विशेषण व्यर्थ हैं॥७॥ जो ज्ञान ग्रहण किये जा चुके अथवा गृहीत नहीं हुए भी अपने और अर्थ को यदि निश्चय करता है, तो वह ज्ञान लोक में और शास्त्रों में भी प्रमाणपने को नहीं छोड़ता है॥७९॥ __इस प्रमाण लक्षण में मीमांसकों ने जो बाधवर्जितपना प्रमाण के लक्षण में लिखा है, सो वह बाधवर्जितपना भी स्व और अर्थ के निश्चय से कोई भिन्न नहीं है। जब स्व और अर्थ का निश्चय हो गया है, तो वह फिर किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं हो सकता। जो बाधित है, वह स्वार्थ निश्चय नहीं है और जो स्वार्थ निश्चय आत्मक ज्ञान है, वह बाधित नहीं है अतः स्वार्थनिश्चय में भी व्यभिचारनिवारणार्थ