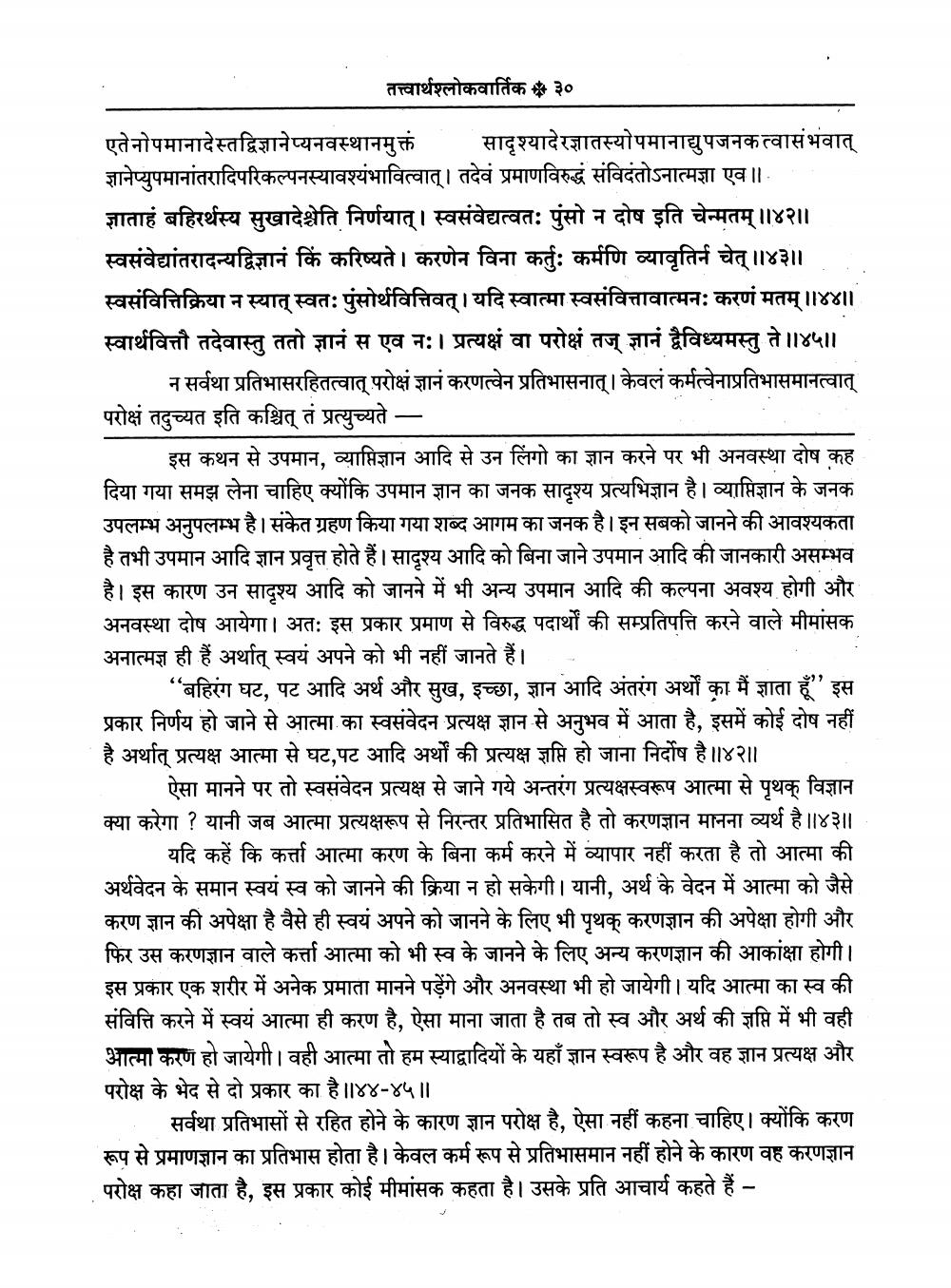________________ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक*३० एतेनोपमानादेस्तद्विज्ञानेप्यनवस्थानमुक्तं सादृश्यादेरज्ञातस्योपमानाद्युपजनक त्वासंभवात् ज्ञानेप्युपमानांतरादिपरिकल्पनस्यावश्यंभावित्वात्। तदेवं प्रमाणविरुद्धं संविदंतोऽनात्मज्ञा एव॥ ज्ञाताहं बहिरर्थस्य सुखादेश्चेति निर्णयात् / स्वसंवेद्यत्वतः पुंसो न दोष इति चेन्मतम् // 42 // स्वसंवेद्यांतरादन्यद्विज्ञानं किं करिष्यते। करणेन विना कर्तुः कर्मणि व्यावृतिर्न चेत् // 43 // स्वसंवित्तिक्रिया न स्यात् स्वतः पुंसोर्थवित्तिवत् / यदि स्वात्मा स्वसंवित्तावात्मनः करणं मतम् // 44 // स्वार्थवित्तौ तदेवास्तु ततो ज्ञानं स एव नः। प्रत्यक्ष वा परोक्षं तज् ज्ञानं द्वैविध्यमस्तु ते॥४५॥ न सर्वथा प्रतिभासरहितत्वात् परोक्षं ज्ञानं करणत्वेन प्रतिभासनात्। केवलं कर्मत्वेनाप्रतिभासमानत्वात् परोक्षं तदुच्यत इति कश्चित् तं प्रत्युच्यते - ___इस कथन से उपमान, व्याप्तिज्ञान आदि से उन लिंगो का ज्ञान करने पर भी अनवस्था दोष कह दिया गया समझ लेना चाहिए क्योंकि उपमान ज्ञान का जनक सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। व्याप्तिज्ञान के जनक उपलम्भ अनुपलम्भ है। संकेत ग्रहण किया गया शब्द आगम का जनक है। इन सबको जानने की आवश्यकता है तभी उपमान आदि ज्ञान प्रवृत्त होते हैं। सादृश्य आदि को बिना जाने उपमान आदि की जानकारी असम्भव है। इस कारण उन सादृश्य आदि को जानने में भी अन्य उपमान आदि की कल्पना अवश्य होगी और अनवस्था दोष आयेगा। अत: इस प्रकार प्रमाण से विरुद्ध पदार्थों की सम्प्रतिपत्ति करने वाले मीमांसक अनात्मज्ञ ही हैं अर्थात् स्वयं अपने को भी नहीं जानते हैं। “बहिरंग घट, पट आदि अर्थ और सुख, इच्छा, ज्ञान आदि अंतरंग अर्थों का मैं ज्ञाता हूँ" इस प्रकार निर्णय हो जाने से आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से अनुभव में आता है, इसमें कोई दोष नहीं है अर्थात् प्रत्यक्ष आत्मा से घट,पट आदि अर्थों की प्रत्यक्ष ज्ञप्ति हो जाना निर्दोष है॥४२॥ ऐसा मानने पर तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जाने गये अन्तरंग प्रत्यक्षस्वरूप आत्मा से पृथक् विज्ञान क्या करेगा ? यानी जब आत्मा प्रत्यक्षरूप से निरन्तर प्रतिभासित है तो करणज्ञान मानना व्यर्थ है॥४३॥ यदि कहें कि कर्ता आत्मा करण के बिना कर्म करने में व्यापार नहीं करता है तो आत्मा की अर्थवेदन के समान स्वयं स्व को जानने की क्रिया न हो सकेगी। यानी, अर्थ के वेदन में आत्मा को जैसे करण ज्ञान की अपेक्षा है वैसे ही स्वयं अपने को जानने के लिए भी पृथक् करणज्ञान की अपेक्षा होगी और फिर उस करणज्ञान वाले कर्ता आत्मा को भी स्व के जानने के लिए अन्य करणज्ञान की आकांक्षा होगी। इस प्रकार एक शरीर में अनेक प्रमाता मानने पड़ेंगे और अनवस्था भी हो जायेगी। यदि आत्मा का स्व की संवित्ति करने में स्वयं आत्मा ही करण है, ऐसा माना जाता है तब तो स्व और अर्थ की ज्ञप्ति में भी वही आत्मा करण हो जायेगी। वही आत्मा तो हम स्याद्वादियों के यहाँ ज्ञान स्वरूप है और वह ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है।४४-४५॥ सर्वथा प्रतिभासों से रहित होने के कारण ज्ञान परोक्ष है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि करण रूप से प्रमाणज्ञान का प्रतिभास होता है। केवल कर्म रूप से प्रतिभासमान नहीं होने के कारण वह करणज्ञान परोक्ष कहा जाता है, इस प्रकार कोई मीमांसक कहता है। उसके प्रति आचार्य कहते हैं -