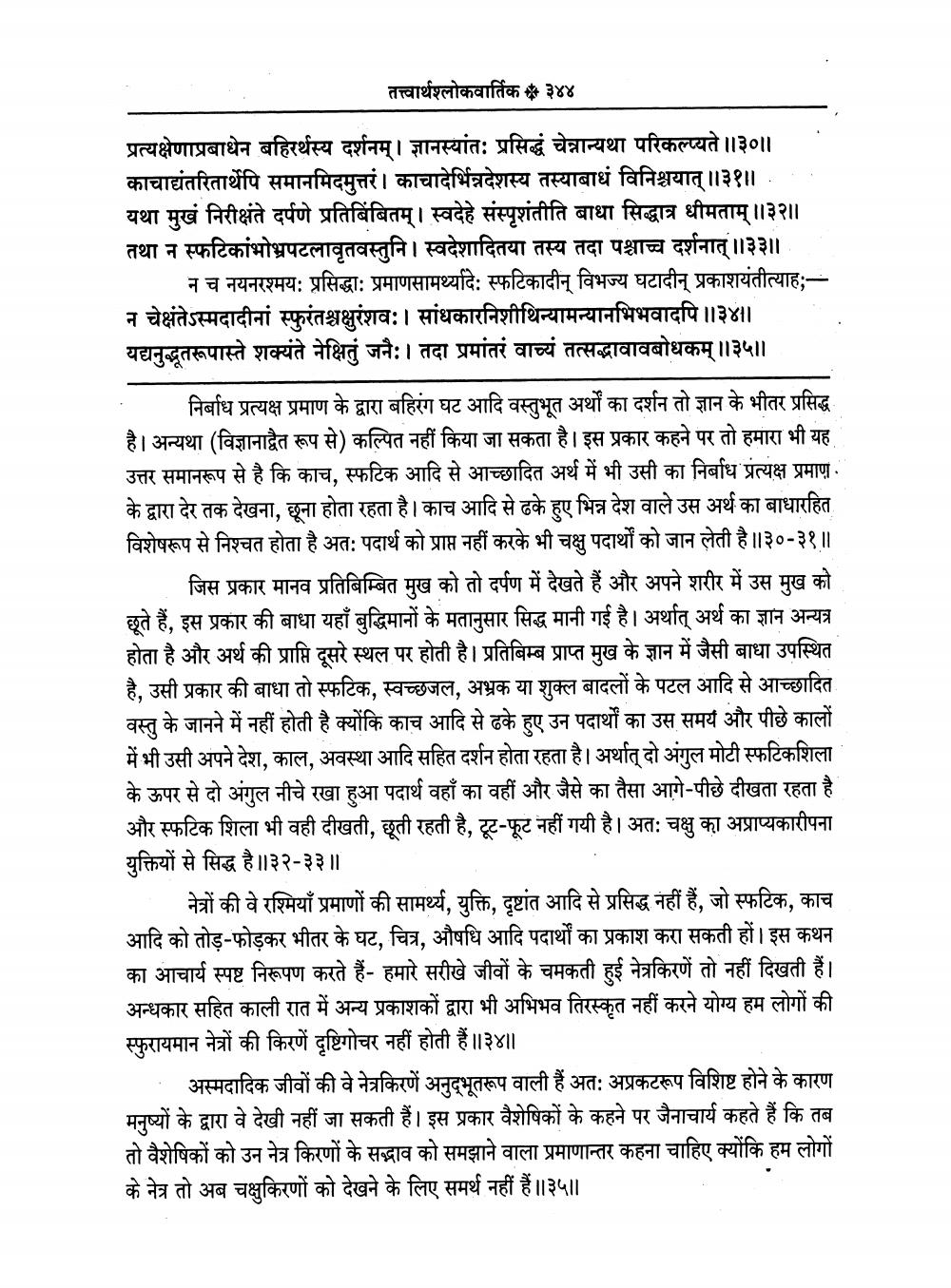________________ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक 344 प्रत्यक्षेणाप्रबाधेन बहिरर्थस्य दर्शनम्। ज्ञानस्यांतः प्रसिद्धं चेन्नान्यथा परिकल्प्यते // 30 // काचाद्यंतरितार्थेपि समानमिदमुत्तरं। काचादेर्भिन्नदेशस्य तस्याबाधं विनिश्चयात् // 31 // . यथा मुखं निरीक्षते दर्पणे प्रतिबिंबितम् / स्वदेहे संस्पृशंतीति बाधा सिद्धात्र धीमताम् // 32 // तथा न स्फटिकांभोभ्रपटलावृतवस्तुनि / स्वदेशादितया तस्य तदा पश्चाच्च दर्शनात् // 33 // न च नयनरश्मयः प्रसिद्धाः प्रमाणसामर्थ्यादेः स्फटिकादीन् विभज्य घटादीन् प्रकाशयंतीत्याह;न चेक्षतेऽस्मदादीनां स्फुरंतश्चक्षुरंशवः। सांधकारनिशीथिन्यामन्यानभिभवादपि // 34 // यद्यनुद्भूतरूपास्ते शक्यंते नेक्षितुं जनैः। तदा प्रमांतरं वाच्यं तत्सद्भावावबोधकम् // 35 // - निर्बाध प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बहिरंग घट आदि वस्तुभूत अर्थों का दर्शन तो ज्ञान के भीतर प्रसिद्ध है। अन्यथा (विज्ञानाद्वैत रूप से) कल्पित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कहने पर तो हमारा भी यह उत्तर समानरूप से है कि काच, स्फटिक आदि से आच्छादित अर्थ में भी उसी का निर्बाध प्रत्यक्ष प्रमाण. के द्वारा देर तक देखना, छूना होता रहता है। काच आदि से ढके हुए भिन्न देश वाले उस अर्थ का बाधारहित विशेषरूप से निश्चत होता है अत: पदार्थ को प्राप्त नहीं करके भी चक्षु पदार्थों को जान लेती है।॥३०-३१॥ जिस प्रकार मानव प्रतिबिम्बित मुख को तो दर्पण में देखते हैं और अपने शरीर में उस मुख को छूते हैं, इस प्रकार की बाधा यहाँ बुद्धिमानों के मतानुसार सिद्ध मानी गई है। अर्थात् अर्थ का ज्ञान अन्यत्र होता है और अर्थ की प्राप्ति दूसरे स्थल पर होती है। प्रतिबिम्ब प्राप्त मुख के ज्ञान में जैसी बाधा उपस्थित है, उसी प्रकार की बाधा तो स्फटिक, स्वच्छजल, अभ्रक या शुक्ल बादलों के पटल आदि से आच्छादित वस्तु के जानने में नहीं होती है क्योंकि काच आदि से ढके हुए उन पदार्थों का उस समय और पीछे कालों में भी उसी अपने देश, काल, अवस्था आदि सहित दर्शन होता रहता है। अर्थात् दो अंगुल मोटी स्फटिकशिला के ऊपर से दो अंगुल नीचे रखा हुआ पदार्थ वहाँ का वहीं और जैसे का तैसा आगे-पीछे दीखता रहता है और स्फटिक शिला भी वही दीखती, छूती रहती है, टूट-फूट नहीं गयी है। अत: चक्षु का अप्राप्यकारीपना युक्तियों से सिद्ध है॥३२-३३॥ नेत्रों की वे रश्मियाँ प्रमाणों की सामर्थ्य, युक्ति, दृष्टांत आदि से प्रसिद्ध नहीं हैं, जो स्फटिक, काच आदि को तोड़-फोड़कर भीतर के घट, चित्र, औषधि आदि पदार्थों का प्रकाश करा सकती हों। इस कथन का आचार्य स्पष्ट निरूपण करते हैं- हमारे सरीखे जीवों के चमकती हुई नेत्रकिरणें तो नहीं दिखती हैं। अन्धकार सहित काली रात में अन्य प्रकाशकों द्वारा भी अभिभव तिरस्कृत नहीं करने योग्य हम लोगों की स्फुरायमान नेत्रों की किरणे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं॥३४॥ - अस्मदादिक जीवों की वे नेत्रकिरणे अनुद्भूतरूप वाली हैं अत: अप्रकटरूप विशिष्ट होने के कारण मनुष्यों के द्वारा वे देखी नहीं जा सकती हैं। इस प्रकार वैशेषिकों के कहने पर जैनाचार्य कहते हैं कि तब तो वैशेषिकों को उन नेत्र किरणों के सद्भाव को समझाने वाला प्रमाणान्तर कहना चाहिए क्योंकि हम लोगों के नेत्र तो अब चक्षुकिरणों को देखने के लिए समर्थ नहीं हैं // 35 //