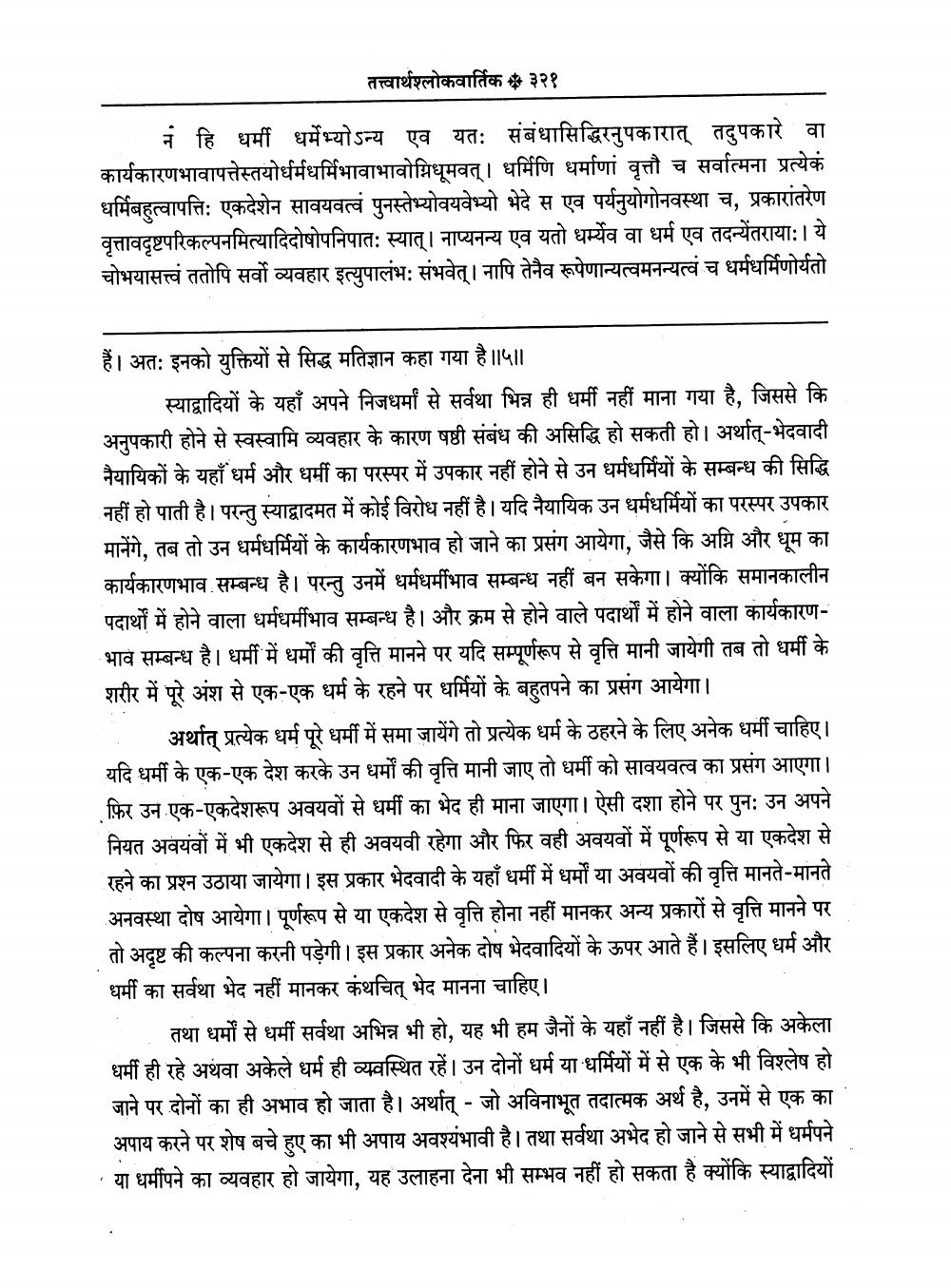________________ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक * 321 नं हि धर्मी धर्मेभ्योऽन्य एव यतः संबंधासिद्धिरनुपकारात् तदुपकारे वा कार्यकारणभावापत्तेस्तयोर्धर्मधर्मिभावाभावोग्निधूमवत् / धर्मिणि धर्माणां वृत्तौ च सर्वात्मना प्रत्येक धर्मिबहुत्वापत्तिः एकदेशेन सावयवत्वं पुनस्तेभ्योवयवेभ्यो भेदे स एव पर्यनुयोगोनवस्था च, प्रकारांतरेण वृत्तावदृष्टपरिकल्पनमित्यादिदोषोपनिपातः स्यात्। नाप्यनन्य एव यतो धर्येव वा धर्म एव तदन्येतरायाः। ये चोभयासत्त्वं ततोपि सर्वो व्यवहार इत्युपालंभः संभवेत्। नापि तेनैव रूपेणान्यत्वमनन्यत्वं च धर्मधर्मिणोर्यतो हैं। अत: इनको युक्तियों से सिद्ध मतिज्ञान कहा गया है॥५॥ स्याद्वादियों के यहाँ अपने निजधर्मां से सर्वथा भिन्न ही धर्मी नहीं माना गया है, जिससे कि अनुपकारी होने से स्वस्वामि व्यवहार के कारण षष्ठी संबंध की असिद्धि हो सकती हो। अर्थात्-भेदवादी नैयायिकों के यहाँ धर्म और धर्मी का परस्पर में उपकार नहीं होने से उन धर्मधर्मियों के सम्बन्ध की सिद्धि नहीं हो पाती है। परन्तु स्याद्वादमत में कोई विरोध नहीं है। यदि नैयायिक उन धर्मधर्मियों का परस्पर उपकार मानेंगे, तब तो उन धर्मधर्मियों के कार्यकारणभाव हो जाने का प्रसंग आयेगा, जैसे कि अग्नि और धूम का कार्यकारणभाव सम्बन्ध है। परन्तु उनमें धर्मधर्मीभाव सम्बन्ध नहीं बन सकेगा। क्योंकि समानकालीन पदार्थों में होने वाला धर्मधर्मीभाव सम्बन्ध है। और क्रम से होने वाले पदार्थों में होने वाला कार्यकारणभाव सम्बन्ध है। धर्मी में धर्मों की वृत्ति मानने पर यदि सम्पूर्णरूप से वृत्ति मानी जायेगी तब तो धर्मी के शरीर में पूरे अंश से एक-एक धर्म के रहने पर धर्मियों के बहुतपने का प्रसंग आयेगा। . अर्थात् प्रत्येक धर्म पूरे धर्मी में समा जायेंगे तो प्रत्येक धर्म के ठहरने के लिए अनेक धर्मी चाहिए। यदि धर्मी के एक-एक देश करके उन धर्मों की वृत्ति मानी जाए तो धर्मी को सावयवत्व का प्रसंग आएगा। फिर उन एक-एकदेशरूप अवयवों से धर्मी का भेद ही माना जाएगा। ऐसी दशा होने पर पुन: उन अपने नियत अवयंवों में भी एकदेश से ही अवयवी रहेगा और फिर वही अवयवों में पूर्णरूप से या एकदेश से रहने का प्रश्न उठाया जायेगा। इस प्रकार भेदवादी के यहाँ धर्मी में धर्मों या अवयवों की वृत्ति मानते-मानते अनवस्था दोष आयेगा। पूर्णरूप से या एकदेश से वृत्ति होना नहीं मानकर अन्य प्रकारों से वृत्ति मानने पर तो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रकार अनेक दोष भेदवादियों के ऊपर आते हैं। इसलिए धर्म और धर्मी का सर्वथा भेद नहीं मानकर कंथचित् भेद मानना चाहिए। तथा धर्मों से धर्मी सर्वथा अभिन्न भी हो, यह भी हम जैनों के यहाँ नहीं है। जिससे कि अकेला धर्मी ही रहे अथवा अकेले धर्म ही व्यवस्थित रहें। उन दोनों धर्म या धर्मियों में से एक के भी विश्लेष हो जाने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है। अर्थात् - जो अविनाभूत तदात्मक अर्थ है, उनमें से एक का अपाय करने पर शेष बचे हुए का भी अपाय अवश्यंभावी है। तथा सर्वथा अभेद हो जाने से सभी में धर्मपने ' या धर्मीपने का व्यवहार हो जायेगा, यह उलाहना देना भी सम्भव नहीं हो सकता है क्योंकि स्याद्वादियों