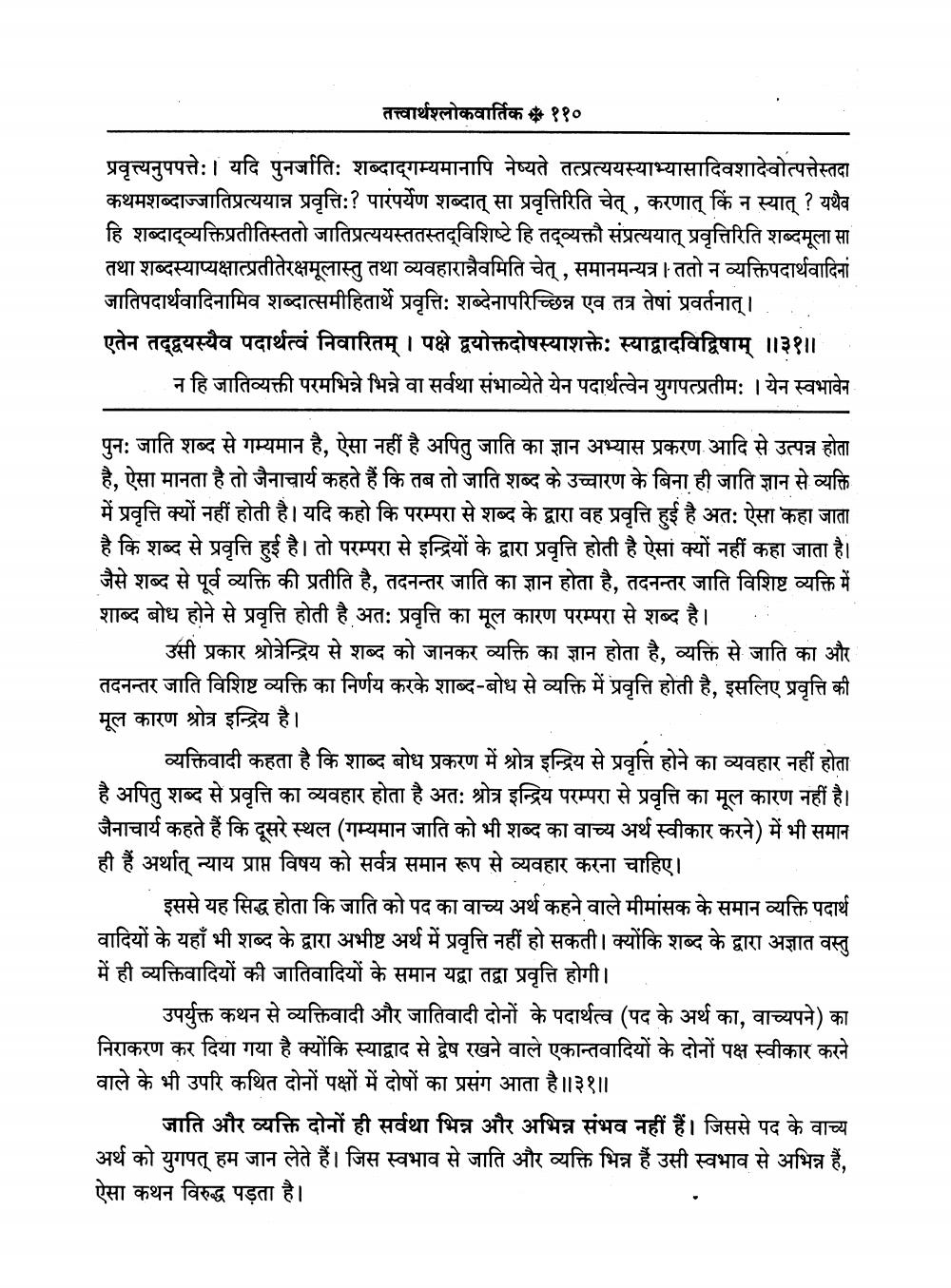________________ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक * 110 प्रवृत्त्यनुपपत्तेः। यदि पुनर्जाति: शब्दाद्गम्यमानापि नेष्यते तत्प्रत्ययस्याभ्यासादिवशादेवोत्पत्तेस्तदा कथमशब्दाज्जातिप्रत्ययान्न प्रवृत्तिः? पारंपर्येण शब्दात् सा प्रवृत्तिरिति चेत् , करणात् किं न स्यात् ? यथैव हि शब्दाद्व्यक्तिप्रतीतिस्ततो जातिप्रत्ययस्ततस्तविशिष्टे हि तद्व्यक्तौ संप्रत्ययात् प्रवृत्तिरिति शब्दमूला सा तथा शब्दस्याप्यक्षात्प्रतीतेरक्षमूलास्तु तथा व्यवहारान्नैवमिति चेत् , समानमन्यत्र / ततो न व्यक्तिपदार्थवादिनां जातिपदार्थवादिनामिव शब्दात्समीहितार्थे प्रवृत्तिः शब्देनापरिच्छिन्न एव तत्र तेषां प्रवर्तनात् / एतेन तवयस्यैव पदार्थत्वं निवारितम् / पक्षे द्वयोक्तदोषस्याशक्तेः स्याद्वादविद्विषाम् // 31 // न हि जातिव्यक्ती परमभिन्ने भिन्ने वा सर्वथा संभाव्येते येन पदार्थत्वेन युगपत्प्रतीमः / येन स्वभावेन पुनः जाति शब्द से गम्यमान है, ऐसा नहीं है अपितु जाति का ज्ञान अभ्यास प्रकरण आदि से उत्पन्न होता है, ऐसा मानता है तो जैनाचार्य कहते हैं कि तब तो जाति शब्द के उच्चारण के बिना ही जाति ज्ञान से व्यक्ति में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है। यदि कहो कि परम्परा से शब्द के द्वारा वह प्रवृत्ति हुई है अत: ऐसा कहा जाता है कि शब्द से प्रवृत्ति हुई है। तो परम्परा से इन्द्रियों के द्वारा प्रवृत्ति होती है ऐसा क्यों नहीं कहा जाता है। जैसे शब्द से पूर्व व्यक्ति की प्रतीति है, तदनन्तर जाति का ज्ञान होता है, तदनन्तर जाति विशिष्ट व्यक्ति में शाब्द बोध होने से प्रवृत्ति होती है अतः प्रवृत्ति का मूल कारण परम्परा से शब्द है। उसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द को जानकर व्यक्ति का ज्ञान होता है, व्यक्ति से जाति का और तदनन्तर जाति विशिष्ट व्यक्ति का निर्णय करके शाब्द-बोध से व्यक्ति में प्रवृत्ति होती है, इसलिए प्रवृत्ति की मूल कारण श्रोत्र इन्द्रिय है। व्यक्तिवादी कहता है कि शाब्द बोध प्रकरण में श्रोत्र इन्द्रिय से प्रवृत्ति होने का व्यवहार नहीं होता है अपितु शब्द से प्रवृत्ति का व्यवहार होता है अतः श्रोत्र इन्द्रिय परम्परा से प्रवृत्ति का मूल कारण नहीं है। जैनाचार्य कहते हैं कि दूसरे स्थल (गम्यमान जाति को भी शब्द का वाच्य अर्थ स्वीकार करने) में भी समान ही हैं अर्थात् न्याय प्राप्त विषय को सर्वत्र समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता कि जाति को पद का वाच्य अर्थ कहने वाले मीमांसक के समान व्यक्ति पदार्थ वादियों के यहाँ भी शब्द के द्वारा अभीष्ट अर्थ में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि शब्द के द्वारा अज्ञात वस्तु में ही व्यक्तिवादियों की जातिवादियों के समान यद्वा तद्वा प्रवृत्ति होगी। उपर्युक्त कथन से व्यक्तिवादी और जातिवादी दोनों के पदार्थत्व (पद के अर्थ का, वाच्यपने) का निराकरण कर दिया गया है क्योंकि स्याद्वाद से द्वेष रखने वाले एकान्तवादियों के दोनों पक्ष स्वीकार करने वाले के भी उपरि कथित दोनों पक्षों में दोषों का प्रसंग आता है॥३१॥ जाति और व्यक्ति दोनों ही सर्वथा भिन्न और अभिन्न संभव नहीं हैं। जिससे पद के वाच्य अर्थ को युगपत् हम जान लेते हैं। जिस स्वभाव से जाति और व्यक्ति भिन्न हैं उसी स्वभाव से अभिन्न हैं, ऐसा कथन विरुद्ध पड़ता है।