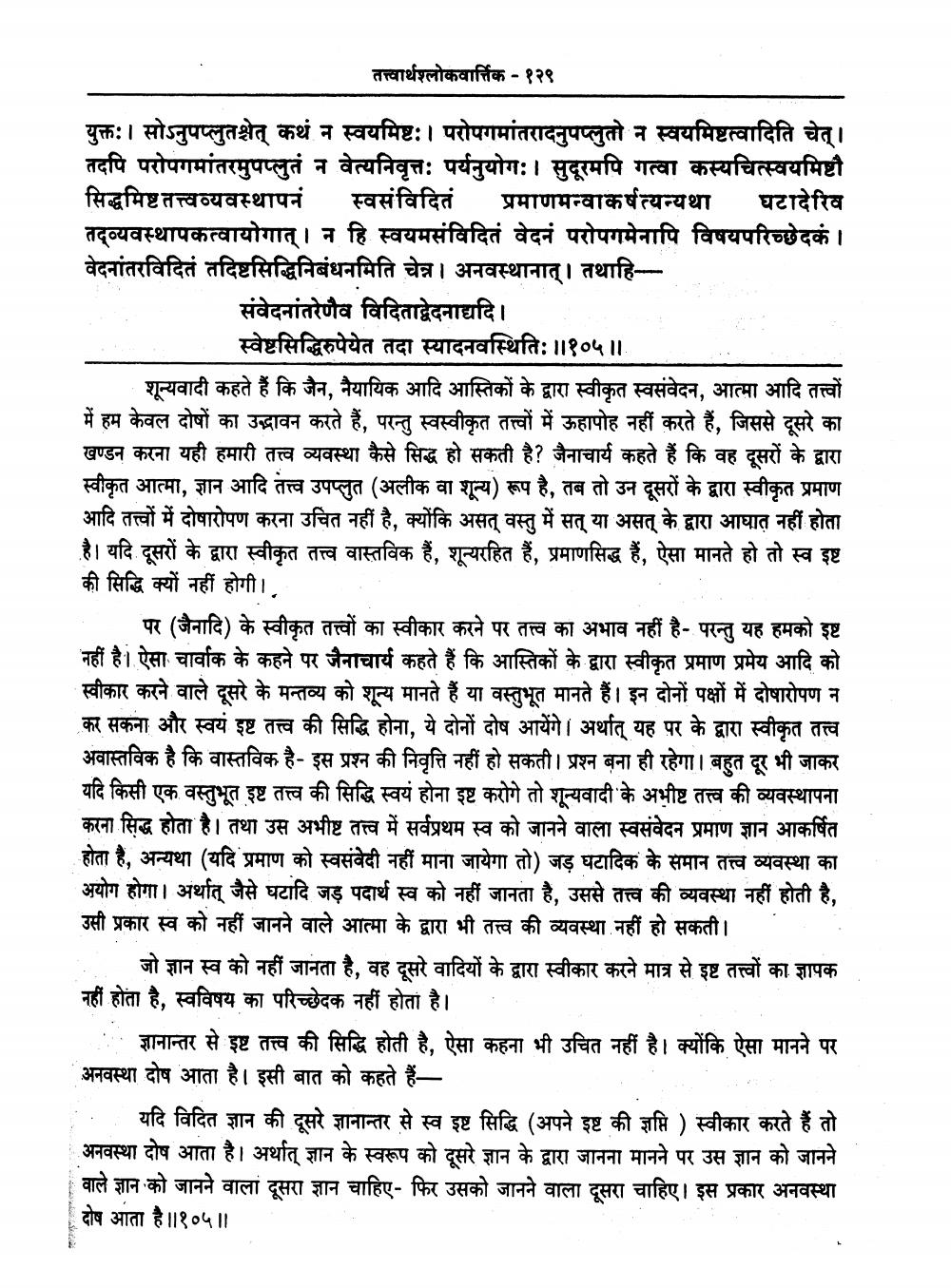________________ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक-१२९ युक्तः। सोऽनुपप्लुतशेत् कथं न स्वयमिष्टः / परोपगमांतरादनुपप्लुतो न स्वयमिष्टत्वादिति चेत् / तदपि परोपगमांतरमुपप्लुतं न वेत्यनिवृत्तः पर्यनुयोगः। सुदूरमपि गत्वा कस्यचित्स्वयमिष्टौ सिद्धमिष्ट तत्त्वव्यवस्थापनं स्वसंविदितं प्रमाणमन्वाकर्षत्यन्यथा घटादेरिव तद्व्यवस्थापकत्वायोगात् / न हि स्वयमसंविदितं वेदनं परोपगमेनापि विषयपरिच्छेदकं / वेदनांतरविदितं तदिष्टसिद्धिनिबंधनमिति चेन्न। अनवस्थानात् / तथाहि संवेदनांतरेणैव विदिताद्वेदनाद्यदि। स्वेष्टसिद्धिरुपेयेत तदा स्यादनवस्थितिः // 105 // ___ शून्यवादी कहते हैं कि जैन, नैयायिक आदि आस्तिकों के द्वारा स्वीकृत स्वसंवेदन, आत्मा आदि तत्त्वों में हम केवल दोषों का उद्भावन करते हैं, परन्तु स्वस्वीकृत तत्त्वों में ऊहापोह नहीं करते हैं, जिससे दूसरे का खण्डन करना यही हमारी तत्त्व व्यवस्था कैसे सिद्ध हो सकती है? जैनाचार्य कहते हैं कि वह दूसरों के द्वारा स्वीकृत आत्मा, ज्ञान आदि तत्त्व उपप्लुत (अलीक वा शून्य) रूप है, तब तो उन दूसरों के द्वारा स्वीकृत प्रमाण आदि तत्त्वों में दोषारोपण करना उचित नहीं है, क्योंकि असत् वस्तु में सत् या असत् के द्वारा आघात नहीं होता है। यदि दूसरों के द्वारा स्वीकृत तत्त्व वास्तविक हैं, शून्यरहित हैं, प्रमाणसिद्ध हैं, ऐसा मानते हो तो स्व इष्ट की सिद्धि क्यों नहीं होगी। पर (जैनादि) के स्वीकृत तत्त्वों का स्वीकार करने पर तत्त्व का अभाव नहीं है- परन्तु यह हमको इष्ट नहीं है। ऐसा चार्वाक के कहने पर जैनाचार्य कहते हैं कि आस्तिकों के द्वारा स्वीकृत प्रमाण प्रमेय आदि को स्वीकार करने वाले दूसरे के मन्तव्य को शून्य मानते हैं या वस्तुभूत मानते हैं। इन दोनों पक्षों में दोषारोपण न कर सकना और स्वयं इष्ट तत्त्व की सिद्धि होना, ये दोनों दोष आयेंगे। अर्थात् यह पर के द्वारा स्वीकृत तत्त्व अवास्तविक है कि वास्तविक है- इस प्रश्न की निवृत्ति नहीं हो सकती। प्रश्न बना ही रहेगा। बहुत दूर भी जाकर यदि किसी एक वस्तुभूत इष्ट तत्त्व की सिद्धि स्वयं होना इष्ट करोगे तो शून्यवादी के अभीष्ट तत्त्व की व्यवस्थापना करना सिद्ध होता है। तथा उस अभीष्ट तत्त्व में सर्वप्रथम स्व को जानने वाला स्वसंवेदन प्रमाण ज्ञान आकर्षित होता है, अन्यथा (यदि प्रमाण को स्वसंवेदी नहीं माना जायेगा तो) जड़ घटादिक के समान तत्त्व व्यवस्था का अयोग होगा। अर्थात् जैसे घटादि जड़ पदार्थ स्व को नहीं जानता है, उससे तत्त्व की व्यवस्था नहीं होती है, उसी प्रकार स्व को नहीं जानने वाले आत्मा के द्वारा भी तत्त्व की व्यवस्था नहीं हो सकती। ___ जो ज्ञान स्व को नहीं जानता है, वह दूसरे वादियों के द्वारा स्वीकार करने मात्र से इष्ट तत्त्वों का ज्ञापक नहीं होता है, स्वविषय का परिच्छेदक नहीं होता है। ज्ञानान्तर से इष्ट तत्त्व की सिद्धि होती है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था दोष आता है। इसी बात को कहते हैं यदि विदित ज्ञान की दूसरे ज्ञानान्तर से स्व इष्ट सिद्धि (अपने इष्ट की ज्ञप्ति ) स्वीकार करते हैं तो अनवस्था दोष आता है। अर्थात् ज्ञान के स्वरूप को दूसरे ज्ञान के द्वारा जानना मानने पर उस ज्ञान को जानने वाले ज्ञान को जानने वाला दूसरा ज्ञान चाहिए- फिर उसको जानने वाला दूसरा चाहिए। इस प्रकार अनवस्था दोष आता है॥१०५॥