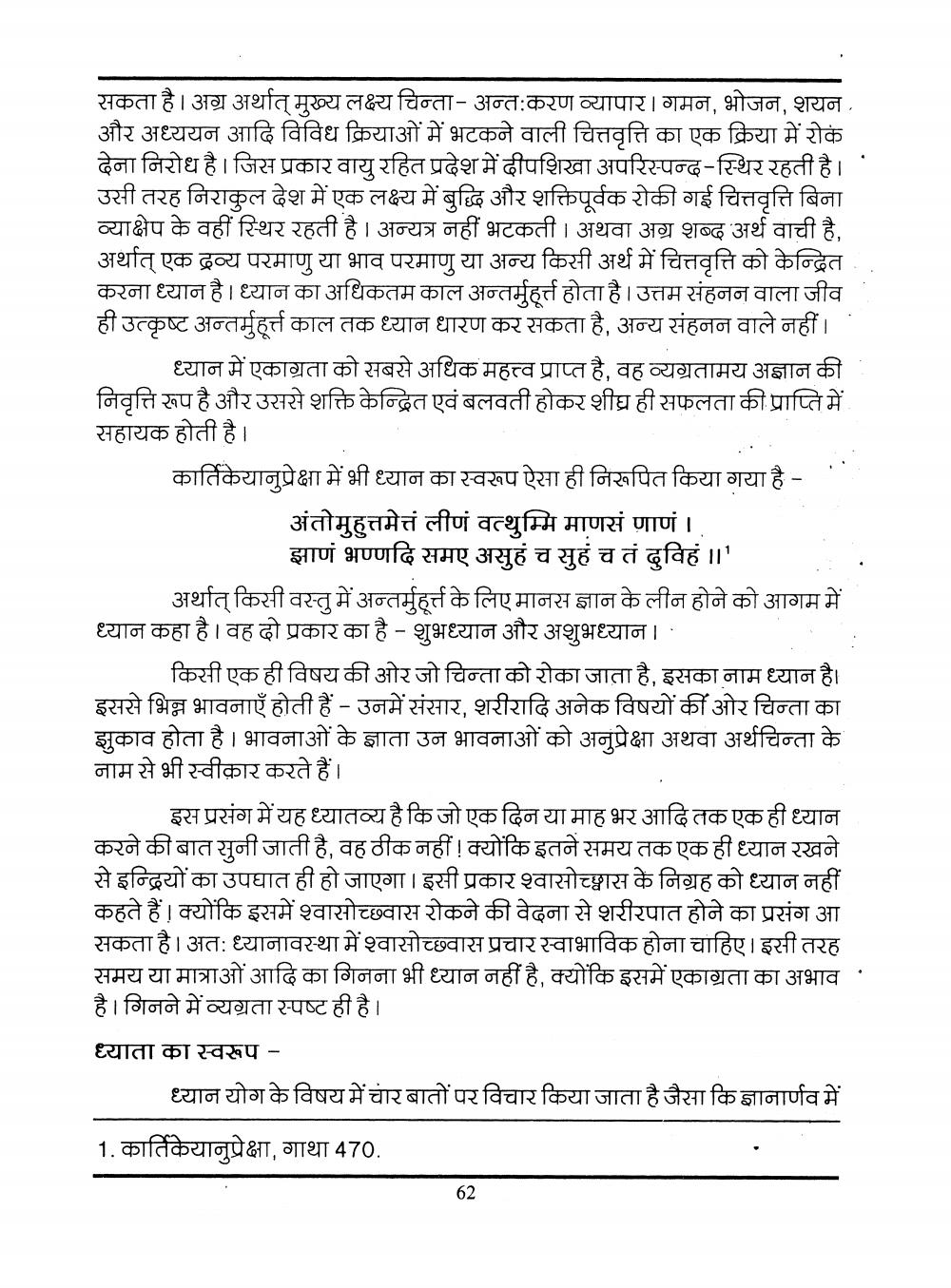________________ सकता है। अग्र अर्थात् मुख्य लक्ष्य चिन्ता- अन्त:करण व्यापार / गमन, भोजन, शयन . और अध्ययन आदि विविध क्रियाओं में भटकने वाली चित्तवृत्ति का एक क्रिया में रोकं देना निरोध है। जिस प्रकार वायु रहित प्रदेश में दीपशिखा अपरिस्पन्द-स्थिर रहती है। . उसी तरह निराकुल देश में एक लक्ष्य में बुद्धि और शक्तिपूर्वक रोकी गई चित्तवृत्ति बिना व्याक्षेप के वहीं स्थिर रहती है। अन्यत्र नहीं भटकती। अथवा अग्र शब्द अर्थ वाची है, अर्थात् एक द्रव्य परमाणु या भाव परमाणु या अन्य किसी अर्थ में चित्तवृत्ति को केन्द्रित करना ध्यान है। ध्यान का अधिकतम काल अन्तर्मुहूर्त होता है। उत्तम संहनन वाला जीव ही उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल तक ध्यान धारण कर सकता है, अन्य संहनन वाले नहीं। ध्यान में एकाग्रता को सबसे अधिक महत्त्व प्राप्त है, वह व्यग्रतामय अज्ञान की निवृत्ति रूप है और उससे शक्ति केन्द्रित एवं बलवती होकर शीघ्र ही सफलता की प्राप्ति में सहायक होती है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में भी ध्यान का स्वरूप ऐसा ही निरूपित किया गया है - अंतोमुहुत्तमेत्तं लीणं वत्थुम्मि माणसं णाणं / झाणं भण्णदि समए असुहं च सुहं च तं दुविहं / / अर्थात् किसी वस्तु में अन्तर्मुहूर्त के लिए मानस ज्ञान के लीन होने को आगम में ध्यान कहा है। वह दो प्रकार का है - शुभध्यान और अशुभध्यान। किसी एक ही विषय की ओर जो चिन्ता को रोका जाता है, इसका नाम ध्यान है। इससे भिन्न भावनाएँ होती हैं - उनमें संसार, शरीरादि अनेक विषयों की ओर चिन्ता का झुकाव होता है। भावनाओं के ज्ञाता उन भावनाओं को अनुप्रेक्षा अथवा अर्थचिन्ता के नाम से भी स्वीकार करते हैं। इस प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि जो एक दिन या माह भर आदि तक एक ही ध्यान करने की बात सुनी जाती है, वह ठीक नहीं! क्योंकि इतने समय तक एक ही ध्यान रखने से इन्द्रियों का उपघात ही हो जाएगा। इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास के निग्रह को ध्यान नहीं कहते हैं। क्योंकि इसमें श्वासोच्छवास रोकने की वेदना से शरीरपात होने का प्रसंग आ सकता है। अत: ध्यानावस्था में श्वासोच्छ्वास प्रचार स्वाभाविक होना चाहिए। इसी तरह समय या मात्राओं आदि का गिनना भी ध्यान नहीं है, क्योंकि इसमें एकाग्रता का अभाव / है। गिनने में व्यग्रता स्पष्ट ही है। ध्याता का स्वरूप - ध्यान योग के विषय में चार बातों पर विचार किया जाता है जैसा कि ज्ञानार्णव में 1. कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गाथा 470.