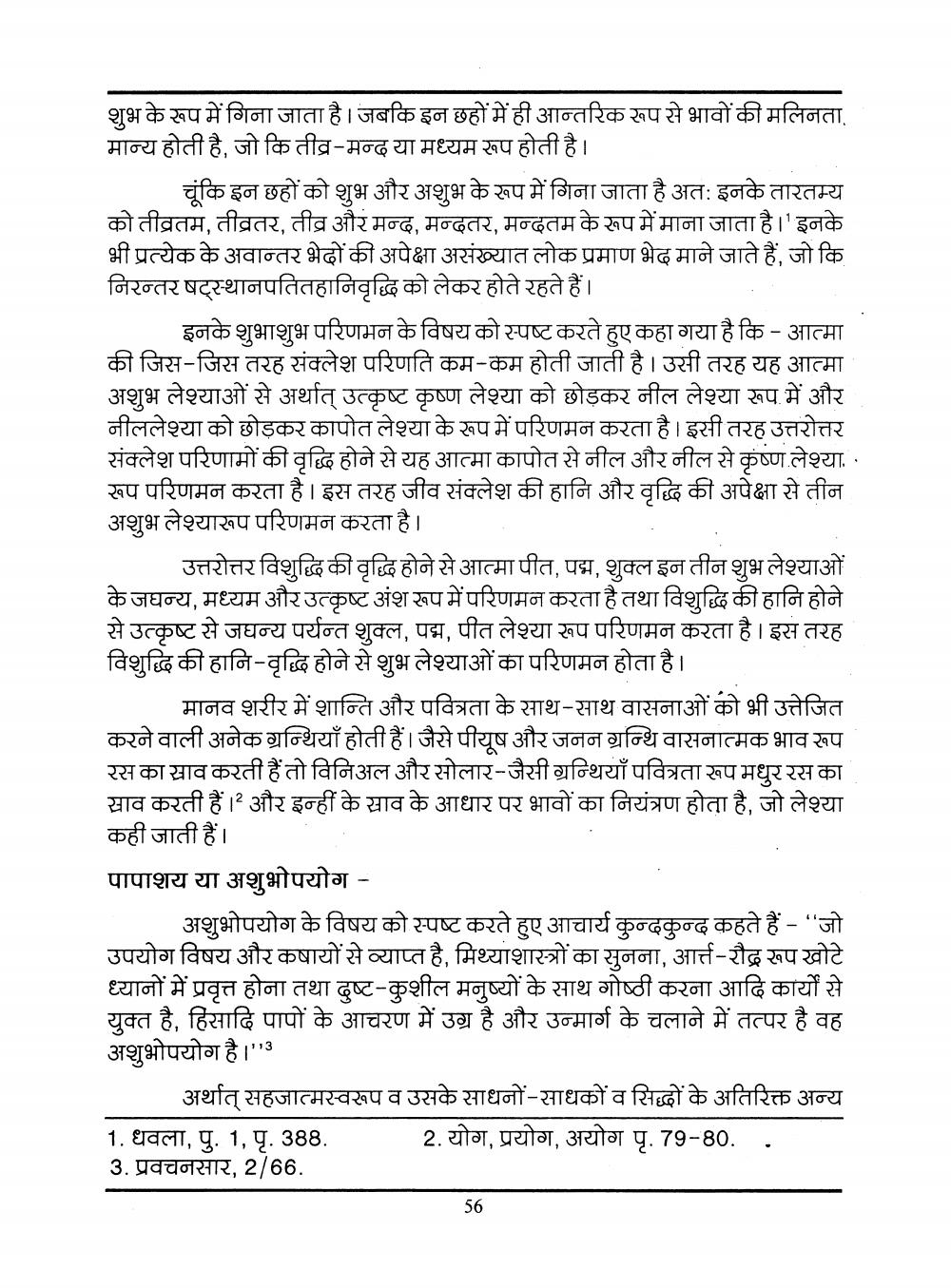________________ शुभ के रूप में गिना जाता है। जबकि इन छहों में ही आन्तरिक रूप से भावों की मलिनता. मान्य होती है, जो कि तीव्र-मन्द या मध्यम रूप होती है। चूंकि इन छहों को शुभ और अशुभ के रूप में गिना जाता है अत: इनके तारतम्य को तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र और मन्द, मन्दतर, मन्दतम के रूप में माना जाता है। इनके भी प्रत्येक के अवान्तर भेदों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद माने जाते हैं, जो कि निरन्तर षट्स्थानपतितहानिवृद्धि को लेकर होते रहते हैं। इनके शुभाशुभ परिणभन के विषय को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि - आत्मा की जिस-जिस तरह संक्लेश परिणति कम-कम होती जाती है। उसी तरह यह आत्मा अशुभ लेश्याओं से अर्थात् उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या को छोड़कर नील लेश्या रूप में और नीललेश्या को छोड़कर कापोत लेश्या के रूप में परिणमन करता है। इसी तरह उत्तरोत्तर संक्लेश परिणामों की वृद्धि होने से यह आत्मा कापोत से नील और नील से कृष्ण लेश्या. . रूप परिणमन करता है। इस तरह जीव संक्लेश की हानि और वृद्धि की अपेक्षा से तीन अशुभ लेश्यारूप परिणमन करता है। उत्तरोत्तर विशुद्धि की वृद्धि होने से आत्मा पीत, पद्म, शुक्ल इन तीन शुभ लेश्याओं के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंश रूप में परिणमन करता है तथा विशुद्धि की हानि होने से उत्कृष्ट से जघन्य पर्यन्त शुक्ल, पद्म, पीत लेश्या रूप परिणमन करता है। इस तरह विशुद्धि की हानि-वृद्धि होने से शुभ लेश्याओं का परिणमन होता है। ____ मानव शरीर में शान्ति और पवित्रता के साथ-साथ वासनाओं को भी उत्तेजित करने वाली अनेक ग्रन्थियाँ होती हैं। जैसे पीयूष और जनन ग्रन्थि वासनात्मक भाव रूप रस का स्राव करती हैं तो विनिअल और सोलार-जैसी ग्रन्थियाँ पवित्रता रूप मधुर रस का स्राव करती हैं। और इन्हीं के स्राव के आधार पर भावों का नियंत्रण होता है, जो लेश्या कही जाती हैं। पापाशय या अशुभोपयोग - अशुभोपयोग के विषय को स्पष्ट करते हुए आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं - "जो उपयोग विषय और कषायों से व्याप्त है, मिथ्याशास्त्रों का सुनना, आर्त-रौद्र रूप खोटे ध्यानों में प्रवृत्त होना तथा दुष्ट-कुशील मनुष्यों के साथ गोष्ठी करना आदि कार्यों से युक्त है, हिंसादि पापों के आचरण में उग्र है और उन्मार्ग के चलाने में तत्पर है वह अशुभोपयोग है।'' अर्थात् सहजात्मस्वरूप व उसके साधनों-साधकों व सिद्धों के अतिरिक्त अन्य 1. धवला, पु. 1, पृ. 388. 2. योग, प्रयोग, अयोग पृ. 79-80. . 3. प्रवचनसार, 2/66. 56