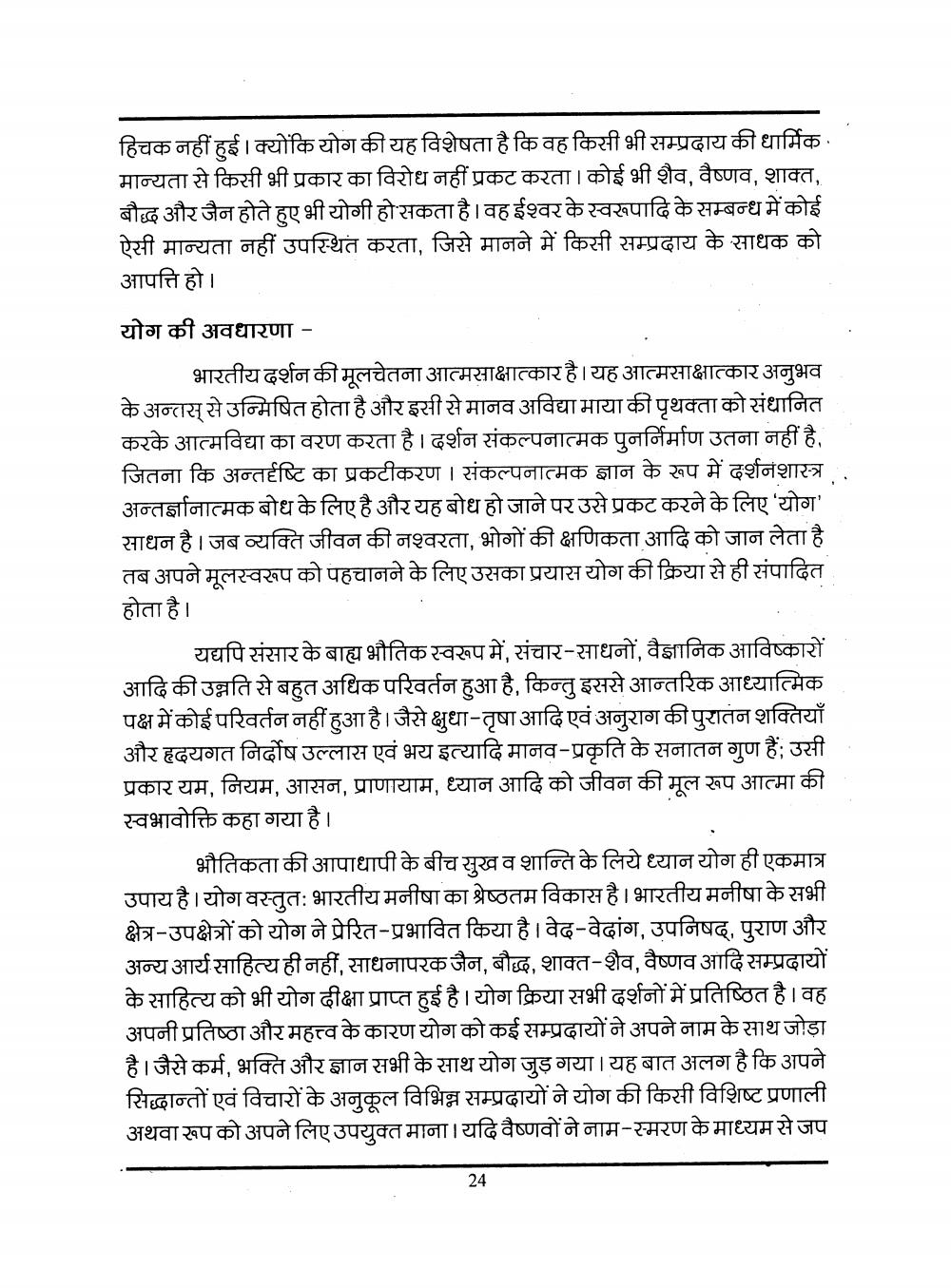________________ हिचक नहीं हुई। क्योंकि योग की यह विशेषता है कि वह किसी भी सम्प्रदाय की धार्मिक मान्यता से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं प्रकट करता। कोई भी शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध और जैन होते हुए भी योगी हो सकता है। वह ईश्वर के स्वरूपादि के सम्बन्ध में कोई ऐसी मान्यता नहीं उपस्थित करता, जिसे मानने में किसी सम्प्रदाय के साधक को आपत्ति हो। योग की अवधारणा - भारतीय दर्शन की मूलचेतना आत्मसाक्षात्कार है। यह आत्मसाक्षात्कार अनुभव के अन्तस् से उन्मिषित होता है और इसी से मानव अविद्या माया की पृथक्ता को संधानित करके आत्मविद्या का वरण करता है। दर्शन संकल्पनात्मक पुनर्निर्माण उतना नहीं है, जितना कि अन्तर्दृष्टि का प्रकटीकरण / संकल्पनात्मक ज्ञान के रूप में दर्शनशास्त्र . अन्तर्ज्ञानात्मक बोध के लिए है और यह बोध हो जाने पर उसे प्रकट करने के लिए 'योग' साधन है। जब व्यक्ति जीवन की नश्वरता, भोगों की क्षणिकता आदि को जान लेता है तब अपने मूलस्वरूप को पहचानने के लिए उसका प्रयास योग की क्रिया से ही संपादित होता है। यद्यपि संसार के बाह्य भौतिक स्वरूप में, संचार-साधनों, वैज्ञानिक आविष्कारों आदि की उन्नति से बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, किन्तु इससे आन्तरिक आध्यात्मिक पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे क्षुधा-तृषा आदि एवं अनुराग की पुरातन शक्तियाँ और हृदयगत निर्दोष उल्लास एवं भय इत्यादि मानव-प्रकृति के सनातन गुण हैं; उसी प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि को जीवन की मूल रूप आत्मा की स्वभावोक्ति कहा गया है। भौतिकता की आपाधापी के बीच सुख व शान्ति के लिये ध्यान योग ही एकमात्र उपाय है। योग वस्तुत: भारतीय मनीषा का श्रेष्ठतम विकास है। भारतीय मनीषा के सभी क्षेत्र-उपक्षेत्रों को योग ने प्रेरित-प्रभावित किया है। वेद-वेदांग, उपनिषद, पुराण और अन्य आर्य साहित्य ही नहीं, साधनापरक जैन, बौद्ध, शाक्त-शैव, वैष्णव आदि सम्प्रदायों के साहित्य को भी योग दीक्षा प्राप्त हुई है। योग क्रिया सभी दर्शनों में प्रतिष्ठित है। वह अपनी प्रतिष्ठा और महत्त्व के कारण योग को कई सम्प्रदायों ने अपने नाम के साथ जोड़ा है। जैसे कर्म, भक्ति और ज्ञान सभी के साथ योग जुड़ गया। यह बात अलग है कि अपने सिद्धान्तों एवं विचारों के अनुकूल विभिन्न सम्प्रदायों ने योग की किसी विशिष्ट प्रणाली अथवा रूप को अपने लिए उपयुक्त माना। यदि वैष्णवों ने नाम-स्मरण के माध्यम से जप 24