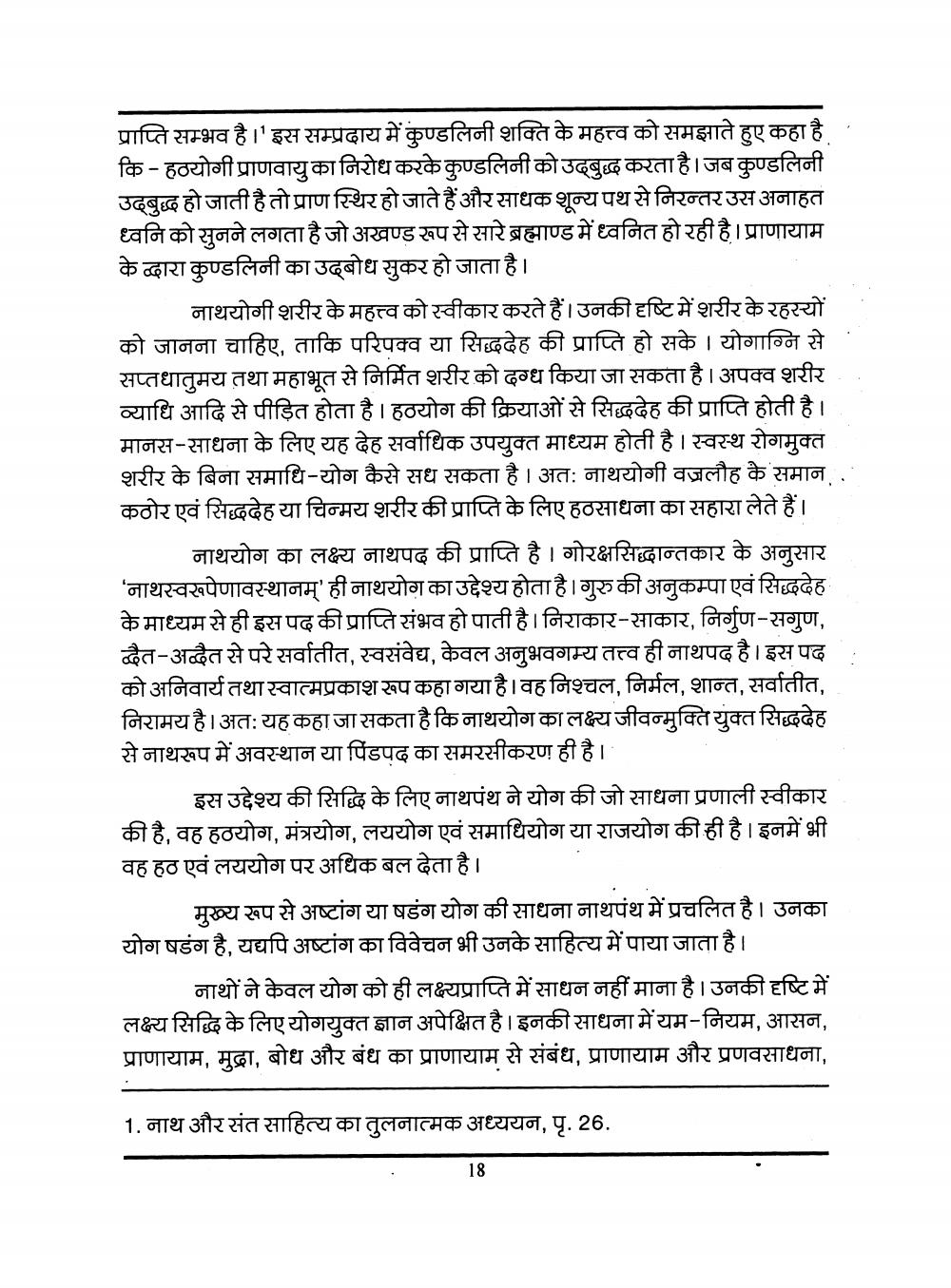________________ प्राप्ति सम्भव है।' इस सम्प्रदाय में कुण्डलिनी शक्ति के महत्त्व को समझाते हुए कहा है. कि - हठयोगी प्राणवायुका निरोध करके कुण्डलिनी को उबुद्ध करता है। जब कुण्डलिनी उदबुद्ध हो जाती है तो प्राण स्थिर हो जाते हैं और साधक शून्य पथ से निरन्तर उस अनाहत ध्वनि को सुनने लगता है जो अखण्ड रूप से सारे ब्रह्माण्ड में ध्वनित हो रही है। प्राणायाम के द्वारा कुण्डलिनी का उदबोध सुकर हो जाता है। ___नाथयोगी शरीर के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में शरीर के रहस्यों को जानना चाहिए, ताकि परिपक्व या सिद्धदेह की प्राप्ति हो सके / योगाग्नि से सप्तधातुमय तथा महाभूत से निर्मित शरीर को दग्ध किया जा सकता है। अपक्व शरीर व्याधि आदि से पीड़ित होता है। हठयोग की क्रियाओं से सिद्धदेह की प्राप्ति होती है। मानस-साधना के लिए यह देह सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम होती है / स्वस्थ रोगमुक्त शरीर के बिना समाधि-योग कैसे सध सकता है। अत: नाथयोगी वज्रलौह के समान . कठोर एवं सिद्धदेह या चिन्मय शरीर की प्राप्ति के लिए हठसाधना का सहारा लेते हैं। नाथयोग का लक्ष्य नाथपद की प्राप्ति है / गोरक्षसिद्धान्तकार के अनुसार 'नाथस्वरूपेणावस्थानम्' ही नाथयोग का उद्देश्य होता है। गुरु की अनुकम्पा एवं सिद्धदेह के माध्यम से ही इस पद की प्राप्ति संभव हो पाती है। निराकार-साकार, निर्गुण-सगुण, दैत-अद्वैत से परे सर्वातीत, स्वसंवेद्य, केवल अनुभवगम्य तत्त्व ही नाथपद है। इस पद को अनिवार्य तथा स्वात्मप्रकाशरूप कहा गया है। वह निश्चल, निर्मल, शान्त,सर्वातीत, निरामय है। अत: यह कहा जा सकता है कि नाथयोग का लक्ष्य जीवन्मुक्तियुक्त सिद्धदेह से नाथरूप में अवस्थान या पिंडपढ का समरसीकरण ही है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नाथपंथ ने योग की जो साधना प्रणाली स्वीकार की है, वह हठयोग, मंत्रयोग, लययोग एवं समाधियोग या राजयोग की ही है। इनमें भी वह हठ एवं लययोग पर अधिक बल देता है। मुख्य रूप से अष्टांग या षडंग योग की साधना नाथपंथ में प्रचलित है। उनका योग षडंग है, यद्यपि अष्टांग का विवेचन भी उनके साहित्य में पाया जाता है। नाथों ने केवल योग को ही लक्ष्यप्राप्ति में साधन नहीं माना है। उनकी दृष्टि में लक्ष्य सिद्धि के लिए योगयुक्त ज्ञान अपेक्षित है। इनकी साधना में यम-नियम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बोध और बंध का प्राणायाम से संबंध, प्राणायाम और प्रणवसाधना, 1. नाथ और संत साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, पृ. 26.