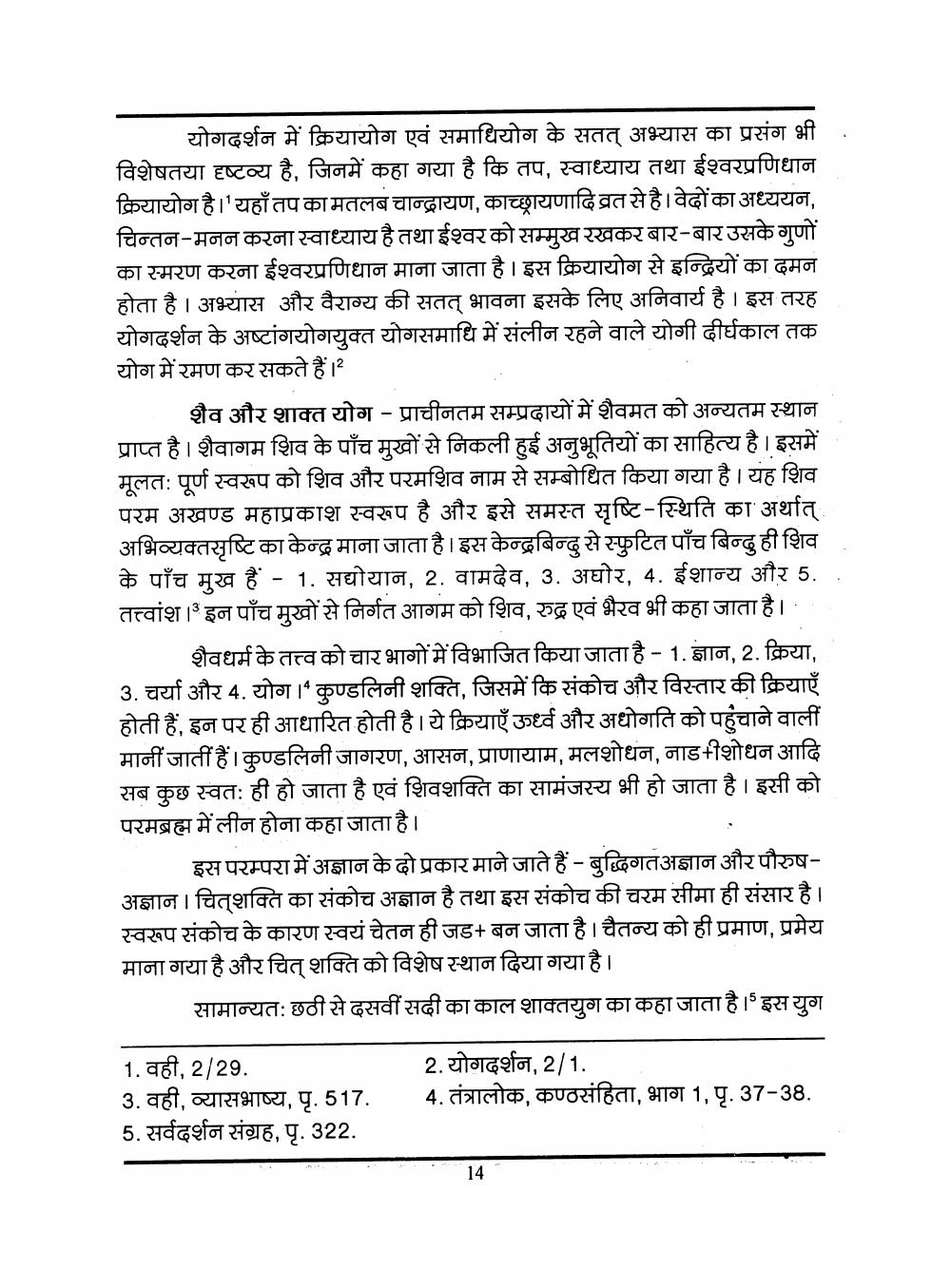________________ योगदर्शन में क्रियायोग एवं समाधियोग के सतत् अभ्यास का प्रसंग भी विशेषतया दृष्टव्य है, जिनमें कहा गया है कि तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग है। यहाँ तप का मतलब चान्द्रायण, काच्छ्रायणादि व्रत से है। वेदों का अध्ययन, चिन्तन-मनन करना स्वाध्याय है तथा ईश्वर को सम्मुख रखकर बार-बार उसके गुणों का स्मरण करना ईश्वरप्रणिधान माना जाता है। इस क्रियायोग से इन्द्रियों का दमन होता है / अभ्यास और वैराग्य की सतत् भावना इसके लिए अनिवार्य है। इस तरह योगदर्शन के अष्टांगयोगयुक्त योगसमाधि में संलीन रहने वाले योगी दीर्घकाल तक योग में रमण कर सकते हैं। शैव और शाक्त योग - प्राचीनतम सम्प्रदायों में शैवमत को अन्यतम स्थान प्राप्त है। शैवागम शिव के पाँच मुखों से निकली हुई अनुभूतियों का साहित्य है। इसमें मूलत: पूर्ण स्वरूप को शिव और परमशिव नाम से सम्बोधित किया गया है। यह शिव परम अखण्ड महाप्रकाश स्वरूप है और इसे समस्त सृष्टि-स्थिति का अर्थात् अभिव्यक्तसृष्टि का केन्द्र माना जाता है। इस केन्द्रबिन्दु से स्फुटित पाँच बिन्दु ही शिव के पाँच मुख हैं - 1. सद्योयान, 2. वामदेव, 3. अघोर, 4. ईशान्य और 5. तत्त्वांश। इन पाँच मुखों से निर्गत आगम को शिव, रुद्र एवं भैरव भी कहा जाता है। शैवधर्म के तत्त्व को चार भागों में विभाजित किया जाता है - 1. ज्ञान, 2. क्रिया, 3. चर्या और 4. योग / कुण्डलिनी शक्ति, जिसमें कि संकोच और विस्तार की क्रियाएँ होती हैं, इन पर ही आधारित होती है। ये क्रियाएँ ऊर्ध्व और अधोगति को पहुंचाने वाली मानी जाती हैं। कुण्डलिनी जागरण, आसन, प्राणायाम, मलशोधन, नाडीशोधन आदि सब कुछ स्वत: ही हो जाता है एवं शिवशक्ति का सामंजस्य भी हो जाता है। इसी को परमब्रह्म में लीन होना कहा जाता है। इस परम्परा में अज्ञान के दो प्रकार माने जाते हैं - बुद्धिगतअज्ञान और पौरुषअज्ञान / चित्शक्ति का संकोच अज्ञान है तथा इस संकोच की चरम सीमा ही संसार है। स्वरूप संकोच के कारण स्वयं चेतन ही जड+ बन जाता है। चैतन्य को ही प्रमाण, प्रमेय माना गया है और चित् शक्ति को विशेष स्थान दिया गया है। सामान्यत: छठी से दसवीं सदी का काल शाक्तयुग का कहा जाता है। इस युग 1. वही, 2/29. 3. वही, व्यासभाष्य, पृ. 517. 5. सर्वदर्शन संग्रह, पृ. 322. 2. योगदर्शन, 2/1. 4. तंत्रालोक, कण्ठसंहिता, भाग 1, पृ. 37-38. 14