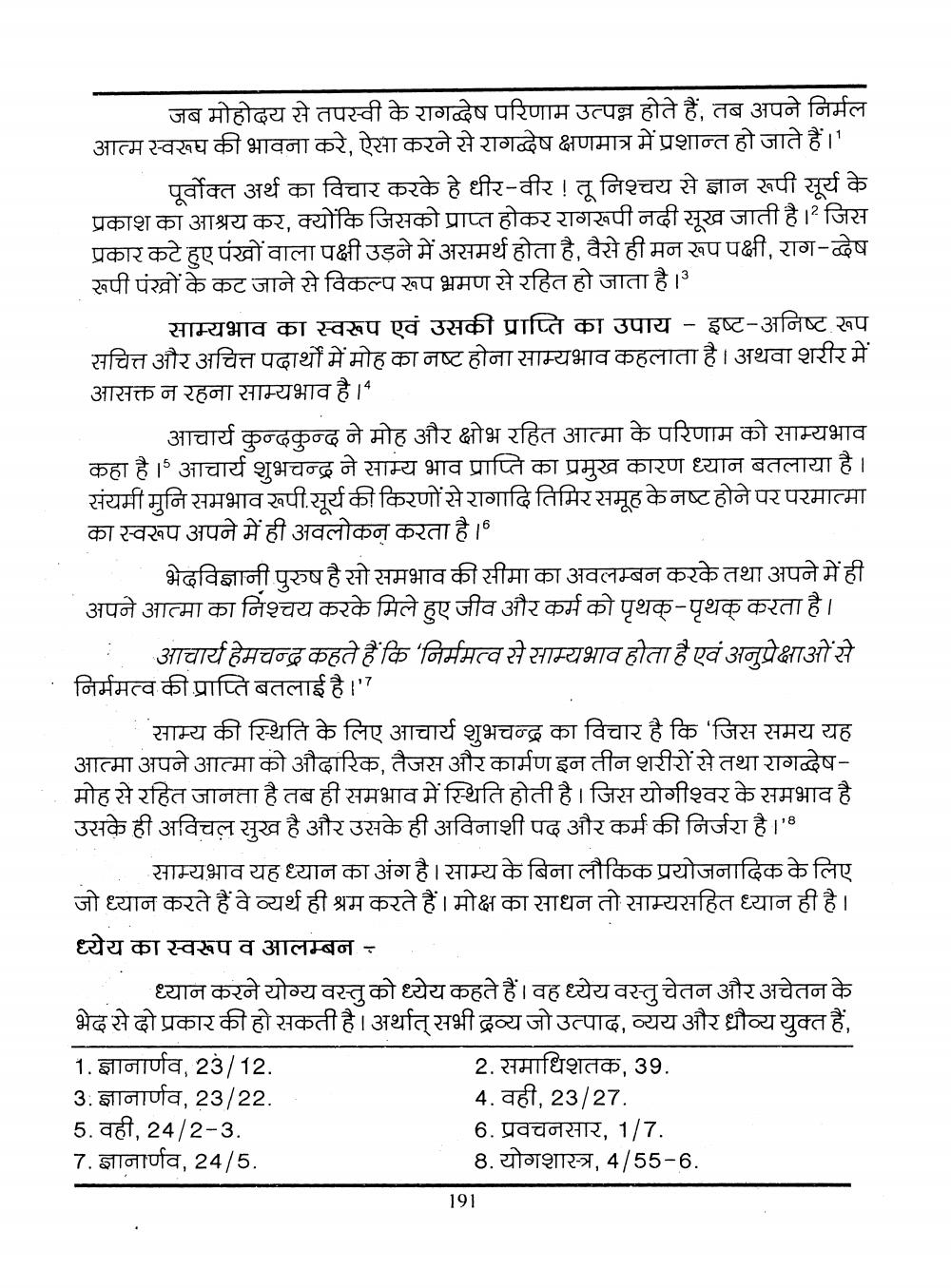________________ जब मोहोदय से तपस्वी के रागद्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं, तब अपने निर्मल आत्म स्वरुप की भावना करे, ऐसा करने से रागद्वेष क्षणमात्र में प्रशान्त हो जाते हैं।' पूर्वोक्त अर्थ का विचार करके हे धीर-वीर ! तू निश्चय से ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश का आश्रय कर, क्योंकि जिसको प्राप्त होकर रागरूपी नदी सूख जाती है। जिस प्रकार कटे हुए पंखों वाला पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है, वैसे ही मन रुप पक्षी, राग-द्वेष रूपी पंखों के कट जाने से विकल्प रूप भ्रमण से रहित हो जाता है। साम्यभाव का स्वरूप एवं उसकी प्राप्ति का उपाय - इष्ट-अनिष्ट रूप सचित्त और अचित्त पदार्थों में मोह का नष्ट होना साम्यभाव कहलाता है। अथवा शरीर में आसक्त न रहना साम्यभाव है। आचार्य कुन्दकुन्द ने मोह और क्षोभ रहित आत्मा के परिणाम को साम्यभाव कहा है। आचार्य शुभचन्द्र ने साम्य भाव प्राप्ति का प्रमुख कारण ध्यान बतलाया है। संयमी मुनि समभाव रूपी.सूर्य की किरणों से रागादि तिमिर समूह के नष्ट होने पर परमात्मा का स्वरूप अपने में ही अवलोकन करता है। भेदविज्ञानी पुरुष है सो समभाव की सीमा का अवलम्बन करके तथा अपने में ही अपने आत्मा का निश्चय करके मिले हुए जीव और कर्म को पृथक्-पृथक् करता है। - आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि 'निर्ममत्व से साम्यभाव होता है एवं अनुप्रेक्षाओं से निर्ममत्व की प्राप्ति बतलाई है। साम्य की स्थिति के लिए आचार्य शुभचन्द्र का विचार है कि जिस समय यह आत्मा अपने आत्मा को औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरों से तथा रागद्वेषमोह से रहित जानता है तब ही समभाव में स्थिति होती है। जिस योगीश्वर के समभाव है उसके ही अविचल सुख है और उसके ही अविनाशी पद और कर्म की निर्जरा है।' साम्यभाव यह ध्यान का अंग है। साम्य के बिना लौकिक प्रयोजनादिक के लिए जो ध्यान करते हैं वे व्यर्थ ही श्रम करते हैं। मोक्ष का साधन तो साम्यसहित ध्यान ही है। ध्येय का स्वरूप व आलम्बन - ध्यान करने योग्य वस्तुको ध्येय कहते हैं। वह ध्येय वस्तुचेतन और अचेतन के भेद से दो प्रकार की हो सकती है। अर्थात् सभी द्रव्य जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त हैं, 1. ज्ञानार्णव, 23/12. 2. समाधिशतक, 39. 3. ज्ञानार्णव, 23/22. 4. वही, 23/27. 5. वही, 24/2-3. 6. प्रवचनसार, 1/7. 7. ज्ञानार्णव, 24/5. 8. योगशास्त्र, 4/55-6. 191