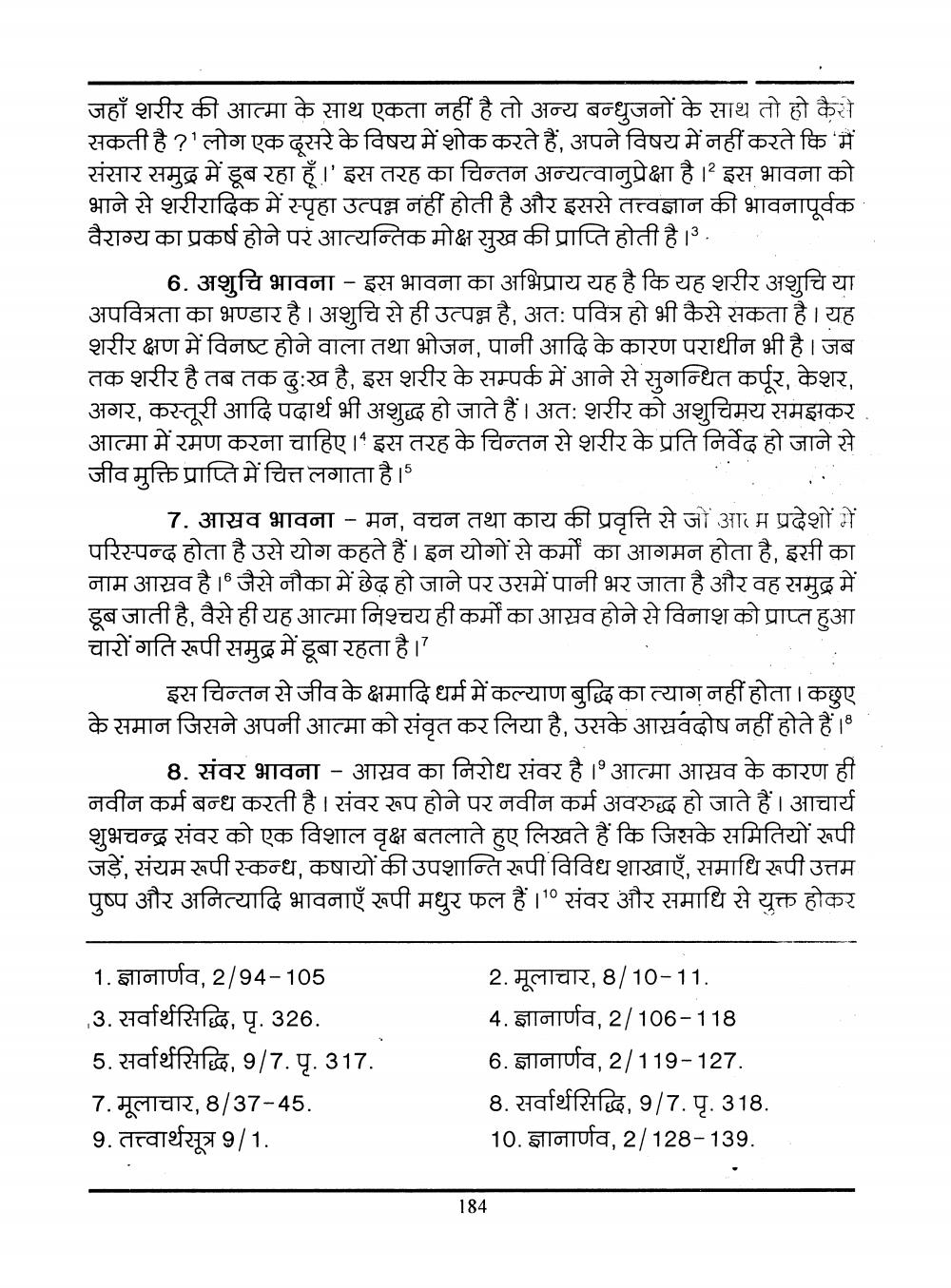________________ जहाँ शरीर की आत्मा के साथ एकता नहीं है तो अन्य बन्धुजनों के साथ तो हो कैसे सकती है ?' लोग एक दूसरे के विषय में शोक करते हैं, अपने विषय में नहीं करते कि मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूँ।' इस तरह का चिन्तन अन्यत्वानुप्रेक्षा है। इस भावना को भाने से शरीराढिक में स्पहा उत्पन्न नहीं होती है और इससे तत्त्वज्ञान की भावनापूर्वक वैराग्य का प्रकर्ष होने परं आत्यन्तिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। 6. अशुचि भावना - इस भावना का अभिप्राय यह है कि यह शरीर अशुचि या अपवित्रता का भण्डार है। अशुचि से ही उत्पन्न है, अत: पवित्र हो भी कैसे सकता है। यह शरीर क्षण में विनष्ट होने वाला तथा भोजन, पानी आदि के कारण पराधीन भी है। जब तक शरीर है तब तक दु:ख है, इस शरीर के सम्पर्क में आने से सुगन्धित कपूर, केशर, अगर, कस्तूरी आदि पदार्थ भी अशुद्ध हो जाते हैं। अत: शरीर को अशुचिमय समझकर आत्मा में रमण करना चाहिए। इस तरह के चिन्तन से शरीर के प्रति निर्वेद हो जाने से जीव मुक्ति प्राप्ति में चित्त लगाता है।' 7. आस्रव भावना - मन, वचन तथा काय की प्रवृत्ति से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पन्द होता है उसे योग कहते हैं। इन योगों से कर्मों का आगमन होता है, इसी का नाम आस्रव है। जैसे नौका में छेद हो जाने पर उसमें पानी भर जाता है और वह समुद्र में डूब जाती है, वैसे ही यह आत्मा निश्चय ही कर्मों का आस्रव होने से विनाश को प्राप्त हुआ चारों गति रूपी समुद्र में डूबा रहता है।' इस चिन्तन से जीव के क्षमादि धर्म में कल्याण बुद्धि का त्याग नहीं होता। कछुए के समान जिसने अपनी आत्मा को संवृत कर लिया है, उसके आस्रवदोष नहीं होते हैं। 8. संवर भावना - आस्रव का निरोध संवर है / आत्मा आस्रव के कारण ही नवीन कर्म बन्ध करती है। संवर रूप होने पर नवीन कर्म अवरुद्ध हो जाते हैं। आचार्य शुभचन्द्र संवर को एक विशाल वृक्ष बतलाते हुए लिखते हैं कि जिसके समितियों रूपी जड़ें, संयम रूपी स्कन्ध, कषायों की उपशान्ति रूपी विविध शाखाएँ, समाधि रूपी उत्तम पुष्प और अनित्यादि भावनाएँ रूपी मधुर फल हैं। संवर और समाधि से युक्त होकर 1. ज्ञानार्णव, 2/94-105 3. सर्वार्थसिद्धि, पृ. 326. 5. सर्वार्थसिद्धि, 9/7. पृ. 317. 7. मूलाचार, 8/37-45. 9. तत्त्वार्थसूत्र 9/1. 2. मूलाचार, 8/10-11. 4. ज्ञानार्णव, 2/106-118 6. ज्ञानार्णव, 2/119-127. 8. सर्वार्थसिद्धि, 9/7. पृ. 318. 10. ज्ञानार्णव, 2/128-139. 184