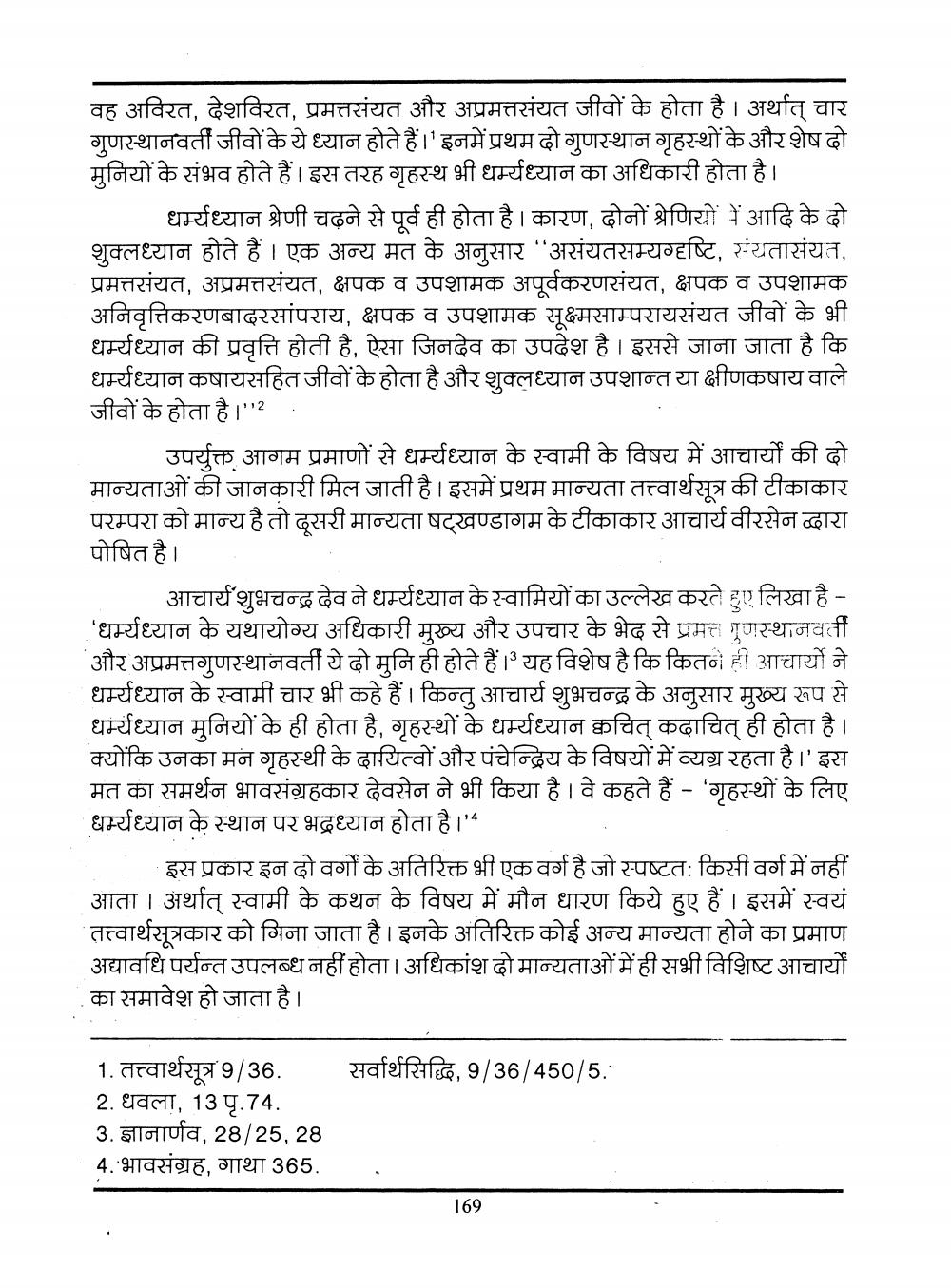________________ वह अविरत, देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवों के होता है। अर्थात् चार गुणस्थानवी जीवों के ये ध्यान होते हैं। इनमें प्रथम दो गुणस्थान गृहस्थों के और शेष दो मुनियों के संभव होते हैं। इस तरह गृहस्थ भी धर्म्यध्यान का अधिकारी होता है। धर्म्यध्यान श्रेणी चढ़ने से पूर्व ही होता है। कारण, दोनों श्रेणियों में आदि के दो शुक्लध्यान होते हैं। एक अन्य मत के अनुसार 'असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, क्षपक व उपशामक अपूर्वकरणसंयत, क्षपक व उपशामक अनिवृत्तिकरणबादरसांपराय, क्षपक व उपशामक सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवों के भी धर्म्यध्यान की प्रवृत्ति होती है, ऐसा जिनदेव का उपदेश है। इससे जाना जाता है कि धर्म्यध्यान कषायसहित जीवों के होता है और शुक्लध्यान उपशान्त या क्षीणकषाय वाले जीवों के होता है।'' उपर्युक्त आगम प्रमाणों से धर्म्यध्यान के स्वामी के विषय में आचार्यों की दो मान्यताओं की जानकारी मिल जाती है। इसमें प्रथम मान्यता तत्त्वार्थसूत्र की टीकाकार परम्परा को मान्य है तो दूसरी मान्यता षट्खण्डागम के टीकाकार आचार्य वीरसेन द्वारा पोषित है। आचार्य शुभचन्द्र देव ने धर्म्यध्यान के स्वामियों का उल्लेख करते हुए लिखा है - 'धर्म्यध्यान के यथायोग्य अधिकारी मुख्य और उपचार के भेद से प्रमत्त गुणस्थाजवर्ती और अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती ये दो मुनि ही होते हैं। यह विशेष है कि कितने ही आचार्यों ने धर्म्यध्यान के स्वामी चार भी कहे हैं। किन्तु आचार्य शुभचन्द्र के अनुसार मुख्य रूप से धर्म्यध्यान मुनियों के ही होता है, गृहस्थों के धर्म्यध्यान क्वचित् कदाचित् ही होता है। क्योंकि उनका मन गृहस्थी के दायित्वों और पंचेन्द्रिय के विषयों में व्यग्र रहता है।' इस मत का समर्थन भावसंग्रहकार देवसेन ने भी किया है। वे कहते हैं - 'गृहस्थों के लिए धर्म्यध्यान के स्थान पर भद्रध्यान होता है।' इस प्रकार इन दो वर्गों के अतिरिक्त भी एक वर्ग है जो स्पष्टत: किसी वर्ग में नहीं आता / अर्थात् स्वामी के कथन के विषय में मौन धारण किये हुए हैं। इसमें स्वयं तत्त्वार्थसूत्रकार को गिना जाता है। इनके अतिरिक्त कोई अन्य मान्यता होने का प्रमाण अद्यावधि पर्यन्त उपलब्ध नहीं होता। अधिकांश दो मान्यताओं में ही सभी विशिष्ट आचार्यों का समावेश हो जाता है। सर्वार्थसिद्धि, 9/36/450/5. 1. तत्त्वार्थसूत्र 9/36. 2. धवला, 13 पृ.74. 3.ज्ञानाणव, 28/25, 28 4. भावसंग्रह, गाथा 365. - 169