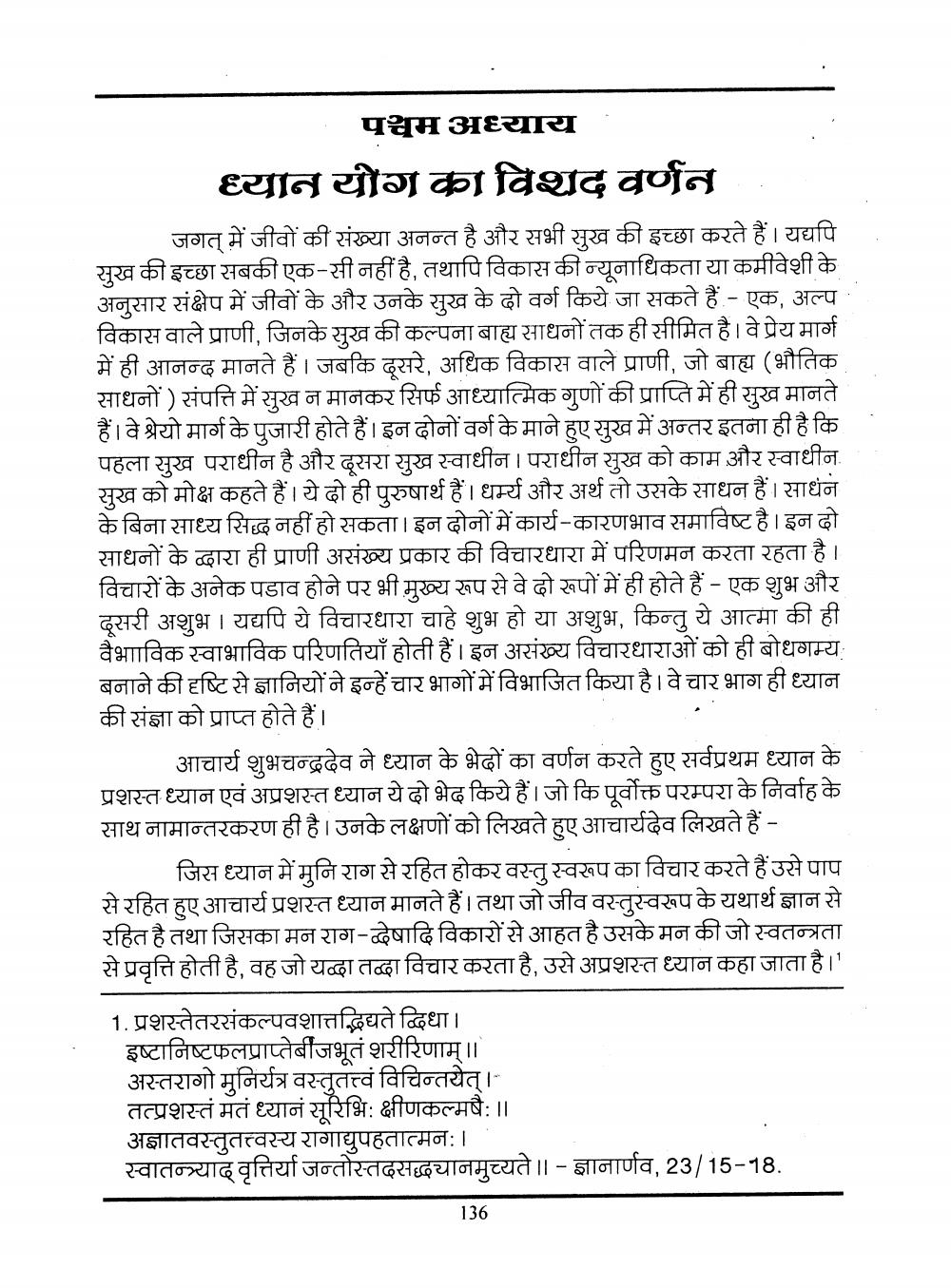________________ पञ्चम अध्याय ध्यान योग का विशद वर्णन जगत् में जीवों की संख्या अनन्त है और सभी सुख की इच्छा करते हैं। यद्यपि सुख की इच्छा सबकी एक-सी नहीं है, तथापि विकास की न्यूनाधिकता या कमीवेशी के अनुसार संक्षेप में जीवों के और उनके सुख के दो वर्ग किये जा सकते हैं - एक, अल्प विकास वाले प्राणी, जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों तक ही सीमित है। वे प्रेय मार्ग में ही आनन्द मानते हैं। जबकि दूसरे, अधिक विकास वाले प्राणी, जो बाह्य (भौतिक साधनों) संपत्ति में सुख न मानकर सिर्फ आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति में ही सुख मानते हैं। वे श्रेयो मार्ग के पुजारी होते हैं। इन दोनों वर्ग के माने हुए सुख में अन्तर इतना ही है कि पहला सुख पराधीन है और दूसरा सुख स्वाधीन / पराधीन सुख को काम और स्वाधीन सुख को मोक्ष कहते हैं। ये दो ही पुरुषार्थ हैं। धर्म्य और अर्थ तो उसके साधन हैं। साधन के बिना साध्य सिद्ध नहीं हो सकता। इन दोनों में कार्य-कारणभाव समाविष्ट है। इन दो साधनों के द्वारा ही प्राणी असंख्य प्रकार की विचारधारा में परिणमन करता रहता है। विचारों के अनेक पडाव होने पर भी मुख्य रूप से वे दो रूपों में ही होते हैं - एक शुभ और दूसरी अशुभ / यद्यपि ये विचारधारा चाहे शुभ हो या अशुभ, किन्तु ये आत्मा की ही वैभाविक स्वाभाविक परिणतियाँ होती हैं। इन असंख्य विचारधाराओं को ही बोधगम्य बनाने की दृष्टि से ज्ञानियों ने इन्हें चार भागों में विभाजित किया है। वे चार भाग ही ध्यान की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। आचार्य शुभचन्द्रदेव ने ध्यान के भेदों का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम ध्यान के प्रशस्त ध्यान एवं अप्रशस्त ध्यान ये दो भेद किये हैं। जो कि पूर्वोक्त परम्परा के निर्वाह के साथ नामान्तरकरण ही है। उनके लक्षणों को लिखते हुए आचार्यदेव लिखते हैं - जिस ध्यान में मुनि राग से रहित होकर वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं उसे पाप से रहित हए आचार्य प्रशस्त ध्यान मानते हैं। तथा जो जीव वस्तुस्वरूपके यथार्थ ज्ञान से रहित है तथा जिसका मन राग-द्वेषादि विकारों से आहत है उसके मन की जो स्वतन्त्रता से प्रवृत्ति होती है, वह जो यदा तदा विचार करता है, उसे अप्रशस्त ध्यान कहा जाता है।' 1. प्रशस्तेतरसंकल्पवशात्तद्भिद्यते विधा। इष्टानिष्टफलप्राप्तेर्बीजभूतं शरीरिणाम् / / अस्तरागो मुनिर्यत्र वस्तुतत्त्वं विचिन्तयेत्। तत्प्रशस्तं मतं ध्यानं सूरिभिः क्षीणकल्मषैः / / अज्ञातवस्तुतत्त्वस्य रागाद्युपहतात्मनः। स्वातन्त्र्याद वृत्तिर्या जन्तोस्तदसढ्यानमुच्यते।। - ज्ञानार्णव, 23/15-18. 136