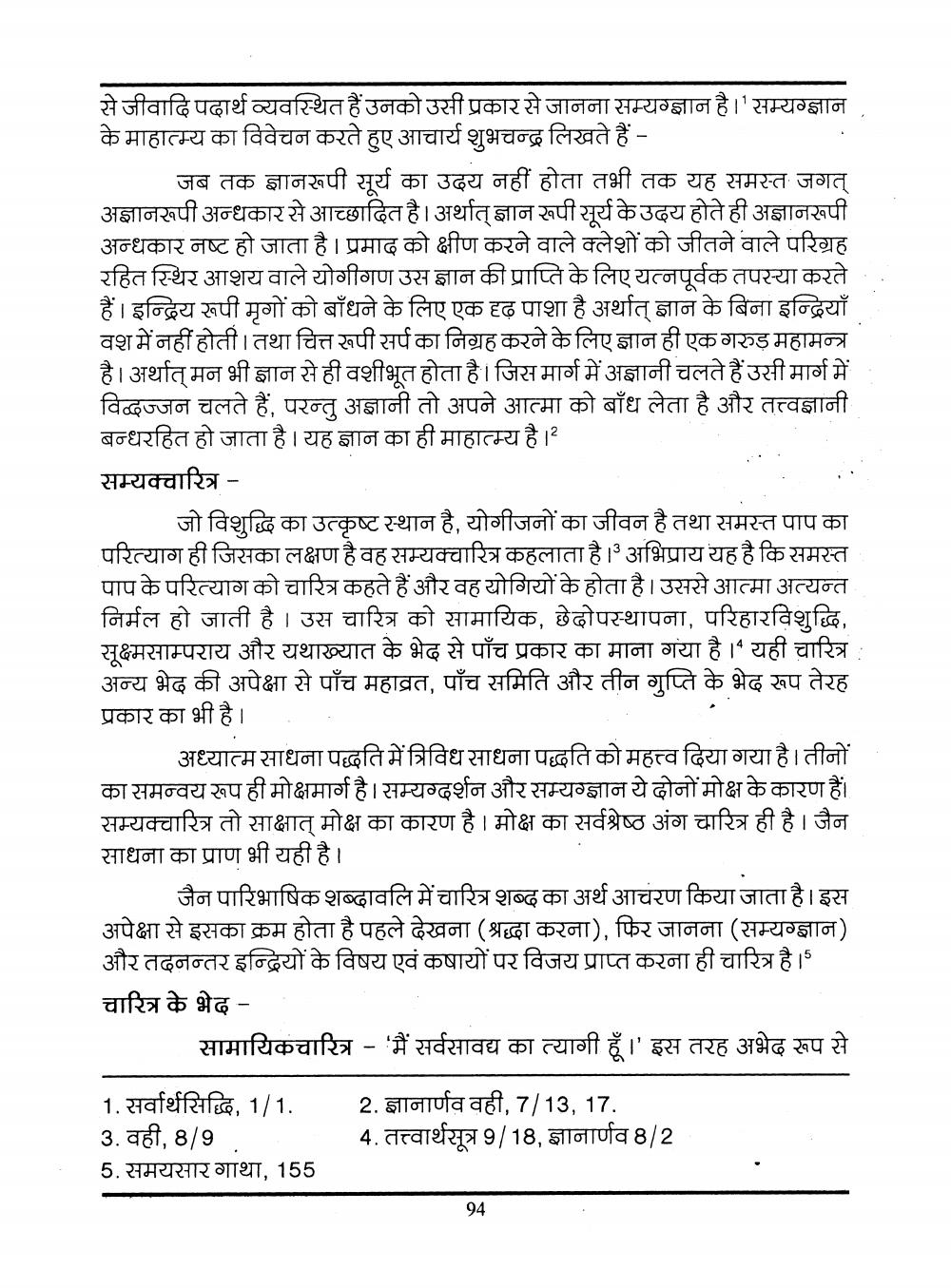________________ से जीवादि पदार्थ व्यवस्थित हैं उनको उसी प्रकार से जानना सम्यग्ज्ञान है।' सम्यग्ज्ञान के माहात्म्य का विवेचन करते हुए आचार्य शुभचन्द्र लिखते हैं - ___ जब तक ज्ञानरूपी सूर्य का उदय नहीं होता तभी तक यह समस्त जगत् अज्ञानरूपी अन्धकार से आच्छादित है। अर्थात् ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है। प्रमाद को क्षीण करने वाले क्लेशों को जीतने वाले परिग्रह रहित स्थिर आशय वाले योगीगण उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्नपूर्वक तपस्या करते हैं। इन्द्रिय रूपी मृगों को बाँधने के लिए एक दृढ़ पाशा है अर्थात् ज्ञान के बिना इन्द्रियाँ वश में नहीं होती। तथा चित्त रूपी सर्प का निग्रह करने के लिए ज्ञान ही एक गरुड़ महामन्त्र है। अर्थात् मन भी ज्ञान से ही वशीभूत होता है। जिस मार्ग में अज्ञानी चलते हैं उसी मार्ग में विदज्जन चलते हैं, परन्तु अज्ञानी तो अपने आत्मा को बाँध लेता है और तत्त्वज्ञानी बन्धरहित हो जाता है। यह ज्ञान का ही माहात्म्य है। सम्यक्चारित्र - जो विशुद्धि का उत्कृष्ट स्थान है,योगीजनों का जीवन है तथा समस्त पाप का परित्याग ही जिसका लक्षण है वह सम्यक्चारित्र कहलाता है। अभिप्राय यह है कि समस्त पाप के परित्याग को चारित्र कहते हैं और वह योगियों के होता है। उससे आत्मा अत्यन्त निर्मल हो जाती है / उस चारित्र को सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात के भेद से पाँच प्रकार का माना गया है। यही चारित्र अन्य भेद की अपेक्षा से पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति के भेद रूप तेरह प्रकार का भी है। अध्यात्म साधना पद्धति में त्रिविध साधना पद्धति को महत्त्व दिया गया है। तीनों का समन्वय रूप ही मोक्षमार्ग है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ये दोनों मोक्ष के कारण हैं। सम्यक्चारित्र तो साक्षात् मोक्ष का कारण है। मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ अंग चारित्र ही है। जैन साधना का प्राण भी यही है। जैन पारिभाषिक शब्दावलि में चारित्र शब्द का अर्थ आचरण किया जाता है। इस अपेक्षा से इसका क्रम होता है पहले देखना (श्रद्धा करना), फिर जानना (सम्यग्ज्ञान) और तदनन्तर इन्द्रियों के विषय एवं कषायों पर विजय प्राप्त करना ही चारित्र है। चारित्र के भेद - सामायिकचारित्र - 'मैं सर्वसावद्य का त्यागी हूँ।' इस तरह अभेद रूप से 1. सर्वार्थसिद्धि, 1/1. 2. ज्ञानार्णव वही, 7/13, 17. 3. वही, 8/9. 4. तत्त्वार्थसूत्र 9/18, ज्ञानार्णव 8/2 5.समयसारगाथा, 155