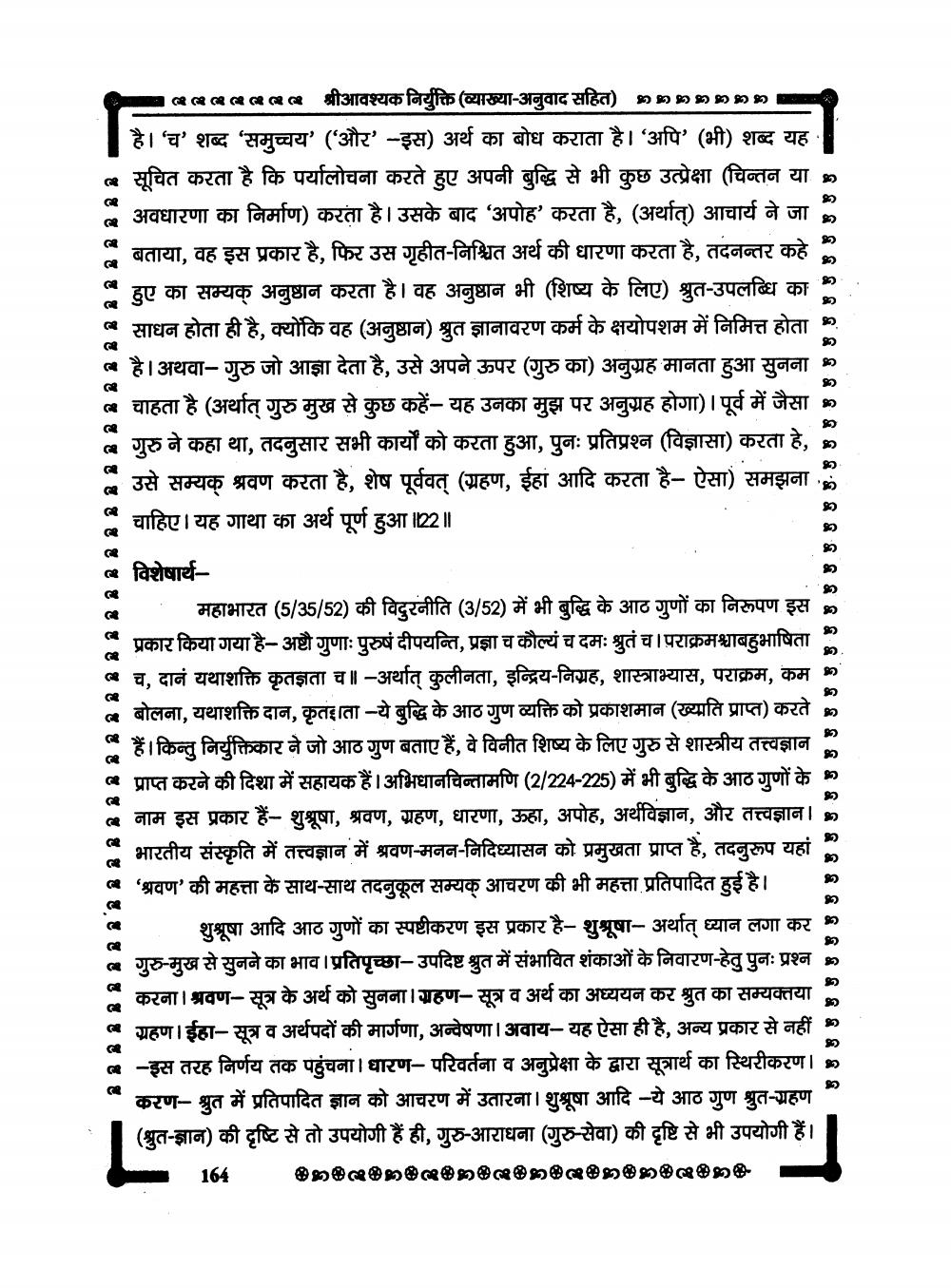________________ 333333232322222222333 888888 -cacacacacace श्रीआवश्यक नियुक्ति (व्याख्या-अनुवाद सहित) 00000000 है। 'च' शब्द 'समुच्चय' ('और' -इस) अर्थ का बोध कराता है। 'अपि' (भी) शब्द यह | सूचित करता है कि पर्यालोचना करते हुए अपनी बुद्धि से भी कुछ उत्प्रेक्षा (चिन्तन या " & अवधारणा का निर्माण) करता है। उसके बाद 'अपोह' करता है, (अर्थात्) आचार्य ने जा, बताया, वह इस प्रकार है, फिर उस गृहीत-निश्चित अर्थ की धारणा करता है, तदनन्तर कहे . हुए का सम्यक् अनुष्ठान करता है। वह अनुष्ठान भी (शिष्य के लिए) श्रुत-उपलब्धि का व साधन होता ही है, क्योंकि वह (अनुष्ठान) श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में निमित्त होता है ca है। अथवा- गुरु जो आज्ञा देता है, उसे अपने ऊपर (गुरु का) अनुग्रह मानता हुआ सुनना , a चाहता है (अर्थात् गुरु मुख से कुछ कहें- यह उनका मुझ पर अनुग्रह होगा)। पूर्व में जैसा " a गुरु ने कहा था, तदनुसार सभी कार्यों को करता हुआ, पुनः प्रतिप्रश्न (विज्ञासा) करता है, . उसे सम्यक् श्रवण करता है, शेष पूर्ववत् (ग्रहण, ईहा आदि करता है- ऐसा) समझना चाहिए। यह गाथा का अर्थ पूर्ण हुआ // 22 // विशेषार्थ - महाभारत (5/35/52) की विदुरनीति (3/52) में भी बुद्धि के आठ गुणों का निरूपण इस : प्रकार किया गया है- अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च / पराक्रमश्चाबहुभाषिता / ca च, दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च॥ -अर्थात् कुलीनता, इन्द्रिय-निग्रह, शास्त्राभ्यास, पराक्रम, कम " बोलना, यथाशक्ति दान, कृतहाता -ये बुद्धि के आठ गुण व्यक्ति को प्रकाशमान (ख्याति प्राप्त) करते , 54 हैं। किन्तु नियुक्तिकार ने जो आठ गुण बताए हैं, वे विनीत शिष्य के लिए गुरु से शास्त्रीय तत्त्वज्ञान / * प्राप्त करने की दिशा में सहायक हैं। अभिधानचिन्तामणि (2/224-225) में भी बुद्धि के आठ गुणों के , नाम इस प्रकार हैं- शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, ऊहा, अपोह, अर्थविज्ञान, और तत्त्वज्ञान। " a भारतीय संस्कृति में तत्त्वज्ञान में श्रवण-मनन-निदिध्यासन को प्रमुखता प्राप्त है, तदनुरुप यहां / ca 'श्रवण' की महत्ता के साथ-साथ तदनुकूल सम्यक् आचरण की भी महत्ता प्रतिपादित हुई है। शुश्रूषा आदि आठ गुणों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है- शुश्रूषा- अर्थात् ध्यान लगा कर , - गुरु-मुख से सुनने का भाव / प्रतिपृच्छा-उपदिष्ट श्रुत में संभावित शंकाओं के निवारण हेतु पुनः प्रश्न - करना। श्रवण-सूत्र के अर्थ को सुनना। ग्रहण-सूत्र व अर्थ का अध्ययन कर श्रुत का सम्यक्तया / ग्रहण। ईहा-सूत्र व अर्थपदों की मार्गणा, अन्वेषणा। अवाय- यह ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं , a -इस तरह निर्णय तक पहुंचना / धारण- परिवर्तना व अनुप्रेक्षा के द्वारा सूत्रार्थ का स्थिरीकरण। " करण-श्रुत में प्रतिपादित ज्ञान को आचरण में उतारना। शुश्रूषा आदि -ये आठ गुण श्रुत-ग्रहण | (श्रुत-ज्ञान) की दृष्टि से तो उपयोगी हैं ही, गुरु-आराधना (गुरु-सेवा) की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। | 09081890c0000000000000000 222222 164