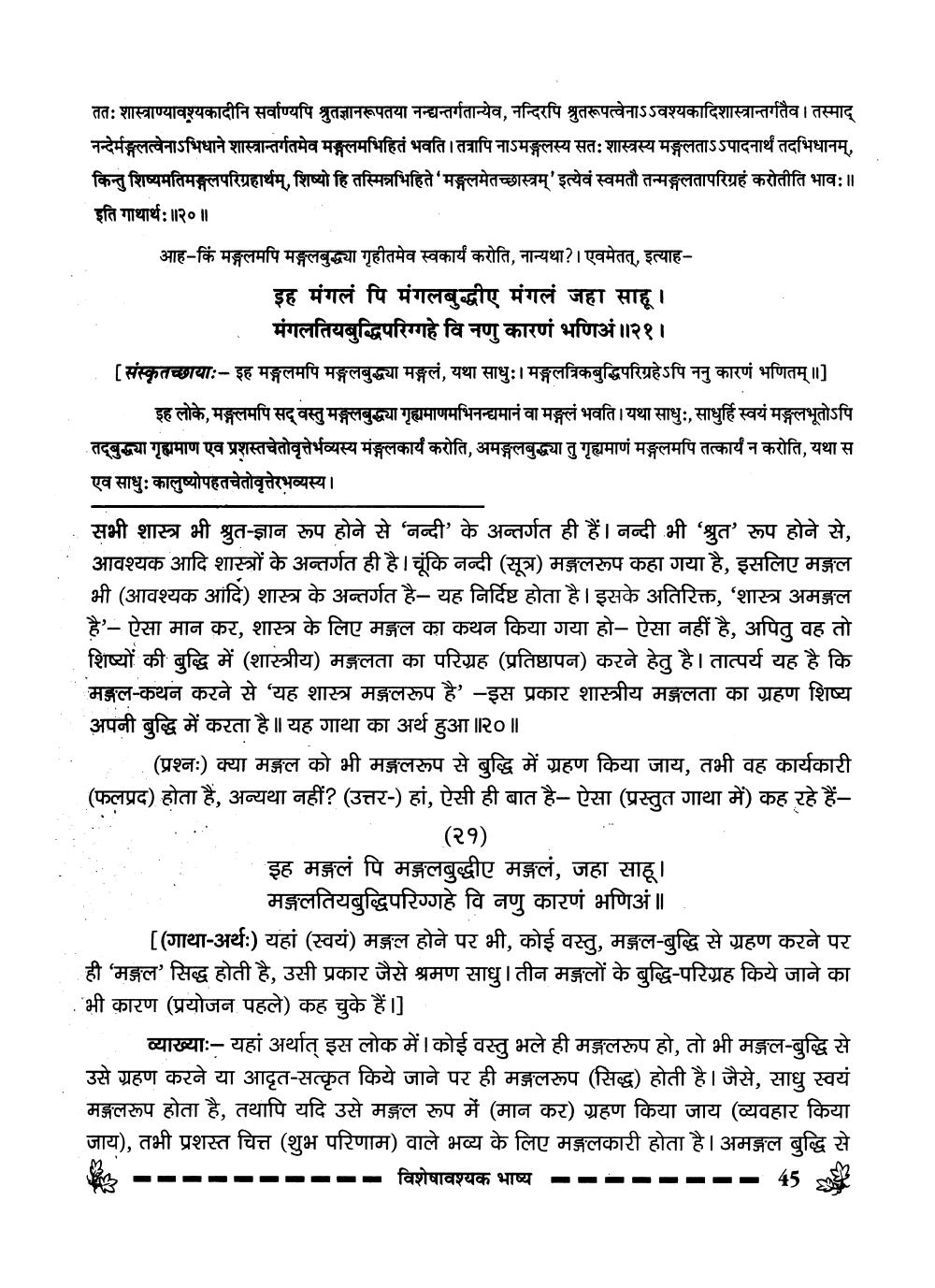________________ ततः शास्त्राण्यावश्यकादीनि सर्वाण्यपि श्रुतज्ञानरूपतया नन्द्यन्तर्गतान्येव, नन्दिरपि श्रुतरूपत्वेनाऽऽवश्यकादिशास्त्रान्तर्गतैव। तस्माद् नन्देर्मङ्गलत्वेनाऽभिधाने शास्त्रान्तर्गतमेव मङ्गलमभिहितं भवति। तत्रापि नाऽमङ्गलस्य सतः शास्त्रस्य मङ्गलताऽऽपादनार्थं तदभिधानम्, किन्तु शिष्यमतिमङ्गलपरिग्रहार्थम्, शिष्यो हि तस्मिन्नभिहिते मङ्गलमेतच्छास्त्रम्' इत्येवं स्वमतौ तन्मङ्गलतापरिग्रहं करोतीति भावः॥ इति गाथार्थः॥२०॥ आह-किं मङ्गलमपि मङ्गलबुद्ध्या गृहीतमेव स्वकार्यं करोति, नान्यथा? / एवमेतत्, इत्याह इह मंगलं पि मंगलबुद्धीए मंगलं जहा साहू। . मंगलतियबुद्धिपरिग्गहे वि नणु कारणं भणिअं॥२१। [संस्कृतच्छाया:- इह मङ्गलमपि मङ्गलबुद्ध्या मङ्गलं, यथा साधुः। मङ्गलत्रिकबुद्धिपरिग्रहेऽपि ननु कारणं भणितम्॥] ___ इह लोके, मङ्गलमपि सद्वस्तु मङ्गलबुद्ध्या गृह्यमाणमभिनन्द्यमानं वा मङ्गलं भवति / यथा साधुः, साधुर्हि स्वयं मङ्गलभूतोऽपि तबुद्ध्या गृह्यमाण एव प्रशस्तचेतोवृत्ते व्यस्य मंगलकार्यं करोति, अमङ्गलबुद्ध्या तु गृह्यमाणं मङ्गलमपि तत्कार्यं न करोति, यथा स एव साधुः कालुष्योपहतचेतोवृत्तेरभव्यस्य। सभी शास्त्र भी श्रुत-ज्ञान रूप होने से 'नन्दी' के अन्तर्गत ही हैं। नन्दी भी 'श्रुत' रूप होने से, आवश्यक आदि शास्त्रों के अन्तर्गत ही है। चूंकि नन्दी (सूत्र) मङ्गलरूप कहा गया है, इसलिए मङ्गल भी (आवश्यक आदि) शास्त्र के अन्तर्गत है- यह निर्दिष्ट होता है। इसके अतिरिक्त, 'शास्त्र अमङ्गल है'- ऐसा मान कर, शास्त्र के लिए मङ्गल का कथन किया गया हो- ऐसा नहीं है, अपितु वह तो शिष्यों की बुद्धि में (शास्त्रीय) मङ्गलता का परिग्रह (प्रतिष्ठापन) करने हेतु है। तात्पर्य यह है कि मङ्गल-कथन करने से 'यह शास्त्र मङ्गलरूप है' -इस प्रकार शास्त्रीय मङ्गलता का ग्रहण शिष्य अपनी बुद्धि में करता है। यह गाथा का अर्थ हुआ // 20 // (प्रश्नः) क्या मङ्गल को भी मङ्गलरूप से बुद्धि में ग्रहण किया जाय, तभी वह कार्यकारी (फलप्रद) होता है, अन्यथा नहीं? (उत्तर-) हां, ऐसी ही बात है- ऐसा (प्रस्तुत गाथा में) कह रहे हैं (21) इह मङ्गलं पि मङ्गलबुद्धीए मङ्गलं, जहा साहू। मङ्गलतियबुद्धिपरिग्गहे वि नणु कारणं भणिअं॥ [(गाथा-अर्थः) यहां (स्वयं) मङ्गल होने पर भी, कोई वस्तु, मङ्गल-बुद्धि से ग्रहण करने पर ही 'मङ्गल' सिद्ध होती है, उसी प्रकार जैसे श्रमण साधु / तीन मङ्गलों के बुद्धि-परिग्रह किये जाने का भी कारण (प्रयोजन पहले) कह चुके हैं।] व्याख्याः- यहां अर्थात् इस लोक में। कोई वस्तु भले ही मङ्गलरूप हो, तो भी मङ्गल-बुद्धि से उसे ग्रहण करने या आदृत-सत्कृत किये जाने पर ही मङ्गलरूप (सिद्ध) होती है। जैसे, साधु स्वयं मङ्गलरूप होता है, तथापि यदि उसे मङ्गल रूप में (मान कर) ग्रहण किया जाय (व्यवहार किया जाय), तभी प्रशस्त चित्त (शुभ परिणाम) वाले भव्य के लिए मङ्गलकारी होता है। अमङ्गल बुद्धि से ----- विशेषावश्यक भाष्य ---- 45