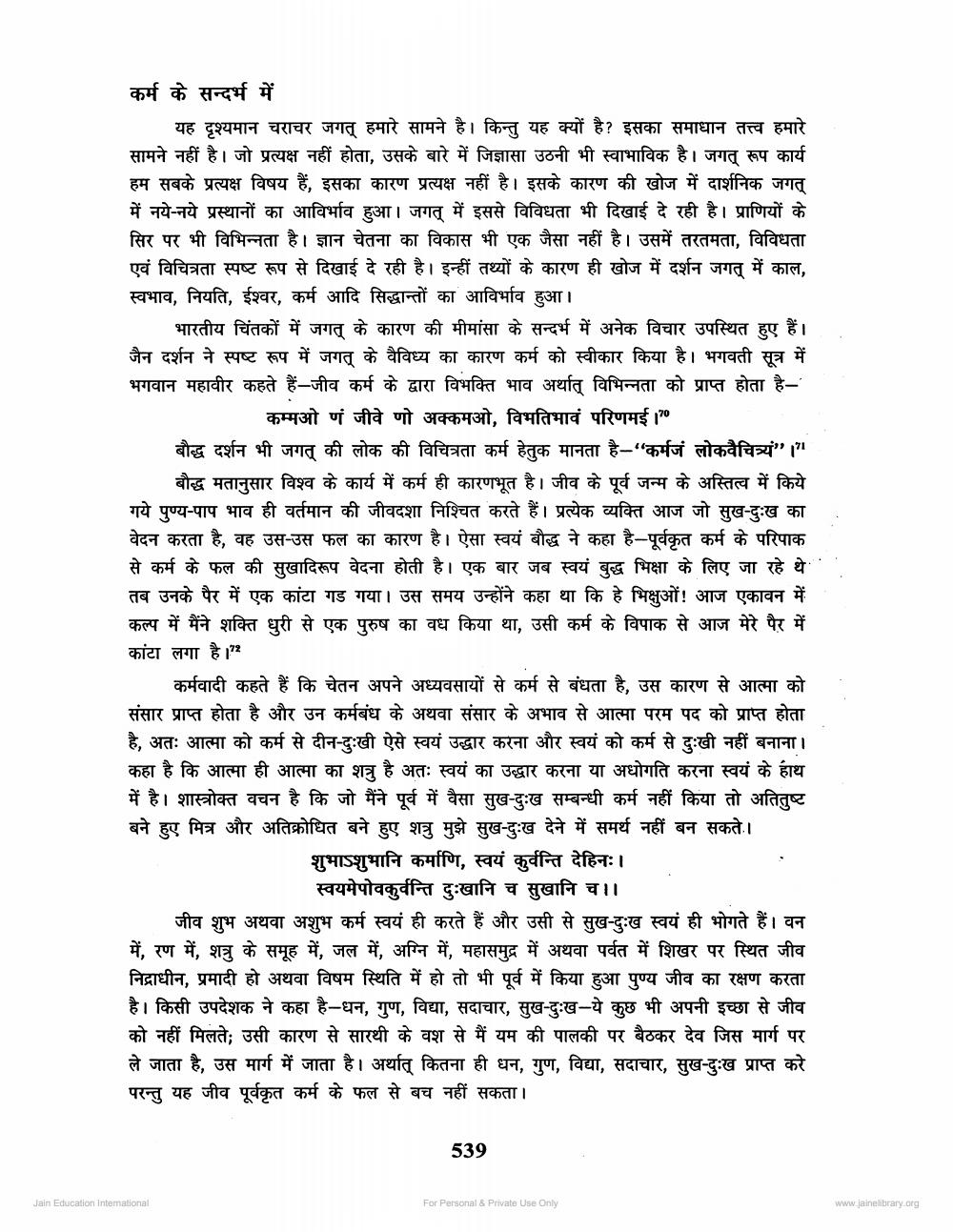________________ कर्म के सन्दर्भ में यह दृश्यमान चराचर जगत् हमारे सामने है। किन्तु यह क्यों है? इसका समाधान तत्त्व हमारे सामने नहीं है। जो प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके बारे में जिज्ञासा उठनी भी स्वाभाविक है। जगत् रूप कार्य हम सबके प्रत्यक्ष विषय हैं, इसका कारण प्रत्यक्ष नहीं है। इसके कारण की खोज में दार्शनिक जगत् में नये-नये प्रस्थानों का आविर्भाव हुआ। जगत् में इससे विविधता भी दिखाई दे रही है। प्राणियों के सिर पर भी विभिन्नता है। ज्ञान चेतना का विकास भी एक जैसा नहीं है। उसमें तरतमता, विविधता एवं विचित्रता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इन्हीं तथ्यों के कारण ही खोज में दर्शन जगत् में काल, स्वभाव, नियति, ईश्वर, कर्म आदि सिद्धान्तों का आविर्भाव हुआ। भारतीय चिंतकों में जगत् के कारण की मीमांसा के सन्दर्भ में अनेक विचार उपस्थित हुए हैं। जैन दर्शन ने स्पष्ट रूप में जगत् के वैविध्य का कारण कर्म को स्वीकार किया है। भगवती सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं-जीव कर्म के द्वारा विभक्ति भाव अर्थात् विभिन्नता को प्राप्त होता है कम्मओ णं जीवे णो अक्कमओ, विभतिभावं परिणमई। बौद्ध दर्शन भी जगत् की लोक की विचित्रता कर्म हेतुक मानता है-“कर्मजं लोकवैचित्र्यं"।" बौद्ध मतानुसार विश्व के कार्य में कर्म ही कारणभूत है। जीव के पूर्व जन्म के अस्तित्व में किये गये पुण्य-पाप भाव ही वर्तमान की जीवदशा निश्चित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आज जो सुख-दुःख का वेदन करता है, वह उस-उस फल का कारण है। ऐसा स्वयं बौद्ध ने कहा है-पूर्वकृत कर्म के परिपाक से कर्म के फल की सुखादिरूप वेदना होती है। एक बार जब स्वयं बुद्ध भिक्षा के लिए जा रहे थे तब उनके पैर में एक कांटा गड गया। उस समय उन्होंने कहा था कि हे भिक्षुओं! आज एकावन में कल्प में मैंने शक्ति धुरी से एक पुरुष का वध किया था, उसी कर्म के विपाक से आज मेरे पैर में कांटा लगा है। कर्मवादी कहते हैं कि चेतन अपने अध्यवसायों से कर्म से बंधता है, उस कारण से आत्मा को संसार प्राप्त होता है और उन कर्मबंध के अथवा संसार के अभाव से आत्मा परम पद को प्राप्त होता है, अतः आत्मा को कर्म से दीन-दुःखी ऐसे स्वयं उद्धार करना और स्वयं को कर्म से दुःखी नहीं बनाना। कहा है कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है अतः स्वयं का उद्धार करना या अधोगति करना स्वयं के हाथ में है। शास्त्रोक्त वचन है कि जो मैंने पूर्व में वैसा सुख-दुःख सम्बन्धी कर्म नहीं किया तो अतितुष्ट बने हुए मित्र और अतिक्रोधित बने हुए शत्रु मुझे सुख-दुःख देने में समर्थ नहीं बन सकते। शुभाशुभानि कर्माणि, स्वयं कुर्वन्ति देहिनः। स्वयमेपोवकुर्वन्ति दुःखानि च सुखानि च।। जीव शुभ अथवा अशुभ कर्म स्वयं ही करते हैं और उसी से सुख-दुःख स्वयं ही भोगते हैं। वन में, रण में, शत्रु के समूह में, जल में, अग्नि में, महासमुद्र में अथवा पर्वत में शिखर पर स्थित जीव निद्राधीन, प्रमादी हो अथवा विषम स्थिति में हो तो भी पूर्व में किया हुआ पुण्य जीव का रक्षण करता है। किसी उपदेशक ने कहा है-धन, गुण, विद्या, सदाचार, सुख-दुःख-ये कुछ भी अपनी इच्छा से जीव को नहीं मिलते; उसी कारण से सारथी के वश से मैं यम की पालकी पर बैठकर देव जिस मार्ग पर ले जाता है, उस मार्ग में जाता है। अर्थात् कितना ही धन, गुण, विद्या, सदाचार, सुख-दुःख प्राप्त करे परन्तु यह जीव पूर्वकृत कर्म के फल से बच नहीं सकता। 539 Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org