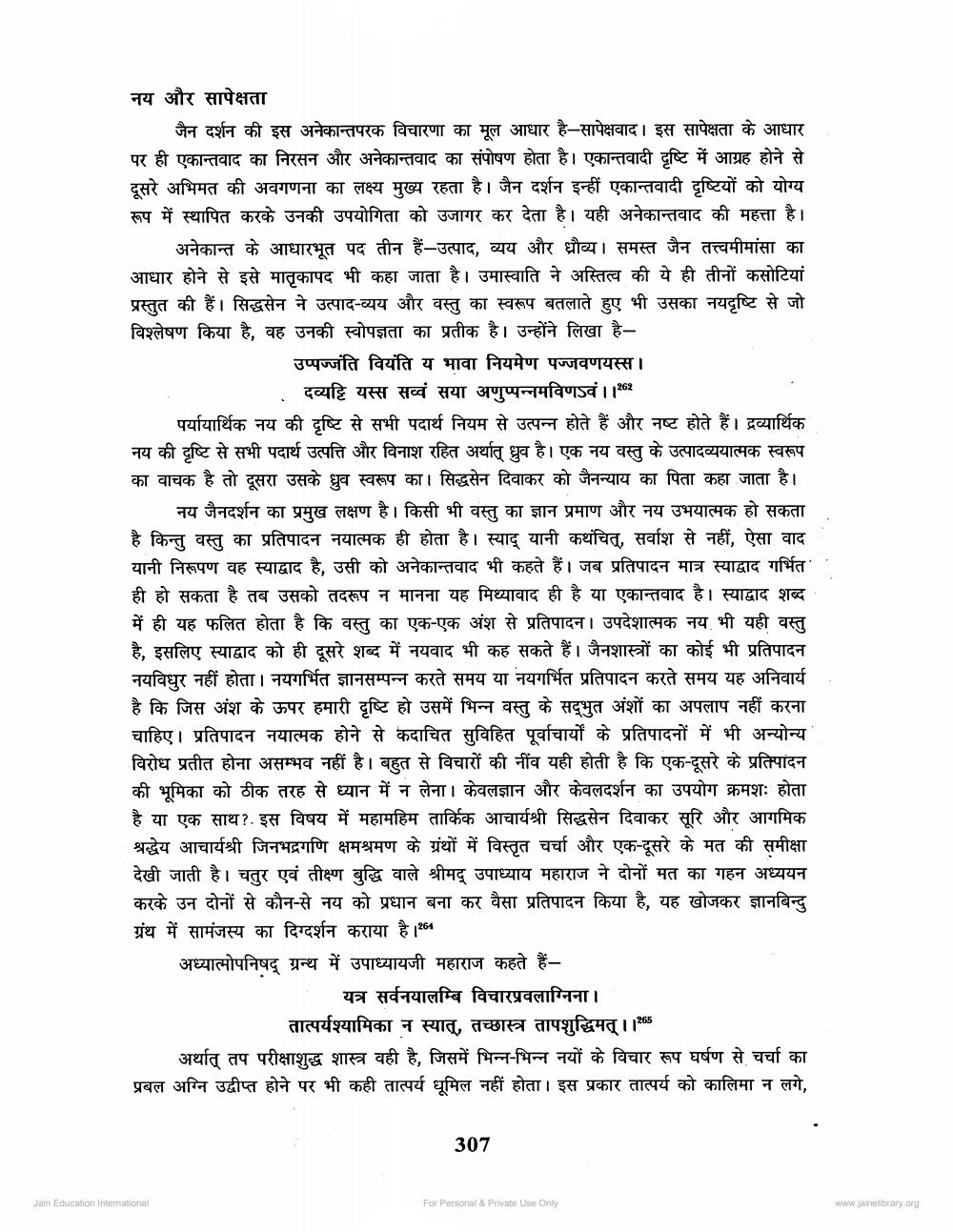________________ नय और सापेक्षता जैन दर्शन की इस अनेकान्तपरक विचारणा का मूल आधार है-सापेक्षवाद। इस सापेक्षता के आधार पर ही एकान्तवाद का निरसन और अनेकान्तवाद का संपोषण होता है। एकान्तवादी दृष्टि में आग्रह होने से दूसरे अभिमत की अवगणना का लक्ष्य मुख्य रहता है। जैन दर्शन इन्हीं एकान्तवादी दृष्टियों को योग्य रूप में स्थापित करके उनकी उपयोगिता को उजागर कर देता है। यही अनेकान्तवाद की महत्ता है। अनेकान्त के आधारभूत पद तीन हैं-उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य। समस्त जैन तत्त्वमीमांसा का आधार होने से इसे मातृकापद भी कहा जाता है। उमास्वाति ने अस्तित्व की ये ही तीनों कसोटियां प्रस्तुत की हैं। सिद्धसेन ने उत्पाद-व्यय और वस्तु का स्वरूप बतलाते हुए भी उसका नयदृष्टि से जो विश्लेषण किया है, वह उनकी स्वोपज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने लिखा है उप्पज्जति वियंति य भावा नियमेण पज्जवणयस्स। . दव्यट्टि यस्स सव्वं सया अणुप्पन्नमविणऽवं / / 11 पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से सभी पदार्थ नियम से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से सभी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश रहित अर्थात् ध्रुव है। एक नय वस्तु के उत्पादव्ययात्मक स्वरूप का वाचक है तो दूसरा उसके ध्रुव स्वरूप का। सिद्धसेन दिवाकर को जैनन्याय का पिता कहा जाता है। नय जैनदर्शन का प्रमुख लक्षण है। किसी भी वस्तु का ज्ञान प्रमाण और नय उभयात्मक हो सकता है किन्तु वस्तु का प्रतिपादन नयात्मक ही होता है। स्याद् यानी कथंचित्, सर्वाश से नहीं, ऐसा वाद यानी निरूपण वह स्याद्वाद है, उसी को अनेकान्तवाद भी कहते हैं। जब प्रतिपादन मात्र स्याद्वाद गर्भित ही हो सकता है तब उसको तदरूप न मानना यह मिथ्यावाद ही है या एकान्तवाद है। स्याद्वाद शब्द में ही यह फलित होता है कि वस्तु का एक-एक अंश से प्रतिपादन। उपदेशात्मक नय भी यही वस्तु है, इसलिए स्याद्वाद को ही दूसरे शब्द में नयवाद भी कह सकते हैं। जैनशास्त्रों का कोई भी प्रतिपादन नयविधुर नहीं होता। नयगर्भित ज्ञानसम्पन्न करते समय या नयगर्भित प्रतिपादन करते समय यह अनिवार्य है कि जिस अंश के ऊपर हमारी दृष्टि हो उसमें भिन्न वस्तु के सद्भुत अंशों का अपलाप नहीं करना चाहिए। प्रतिपादन नयात्मक होने से कदाचित सुविहित पूर्वाचार्यों के प्रतिपादनों में भी अन्योन्य विरोध प्रतीत होना असम्भव नहीं है। बहुत से विचारों की नींव यही होती है कि एक-दूसरे के प्रतिपादन की भूमिका को ठीक तरह से ध्यान में न लेना। केवलज्ञान और केवलदर्शन का उपयोग क्रमशः होता है या एक साथ?. इस विषय में महामहिम तार्किक आचार्यश्री सिद्धसेन दिवाकर सूरि और आगमिक श्रद्धेय आचार्यश्री जिनभद्रगणि क्षमश्रमण के ग्रंथों में विस्तृत चर्चा और एक-दूसरे के मत की समीक्षा देखी जाती है। चतुर एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले श्रीमद् उपाध्याय महाराज ने दोनों मत का गहन अध्ययन करके उन दोनों से कौन-से नय को प्रधान बना कर वैसा प्रतिपादन किया है, यह खोजकर ज्ञानबिन्दु ग्रंथ में सामंजस्य का दिग्दर्शन कराया है। अध्यात्मोपनिषद् ग्रन्थ में उपाध्यायजी महाराज कहते हैं यत्र सर्वनयालम्बि विचारप्रवलाग्निना। तात्पर्यश्यामिका न स्यात्, तच्छास्त्र तापशुद्धिमत् / / 265 अर्थात् तप परीक्षाशुद्ध शास्त्र वही है, जिसमें भिन्न-भिन्न नयों के विचार रूप घर्षण से चर्चा का प्रबल अग्नि उद्वीप्त होने पर भी कही तात्पर्य धूमिल नहीं होता। इस प्रकार तात्पर्य को कालिमा न लगे, 307 Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org