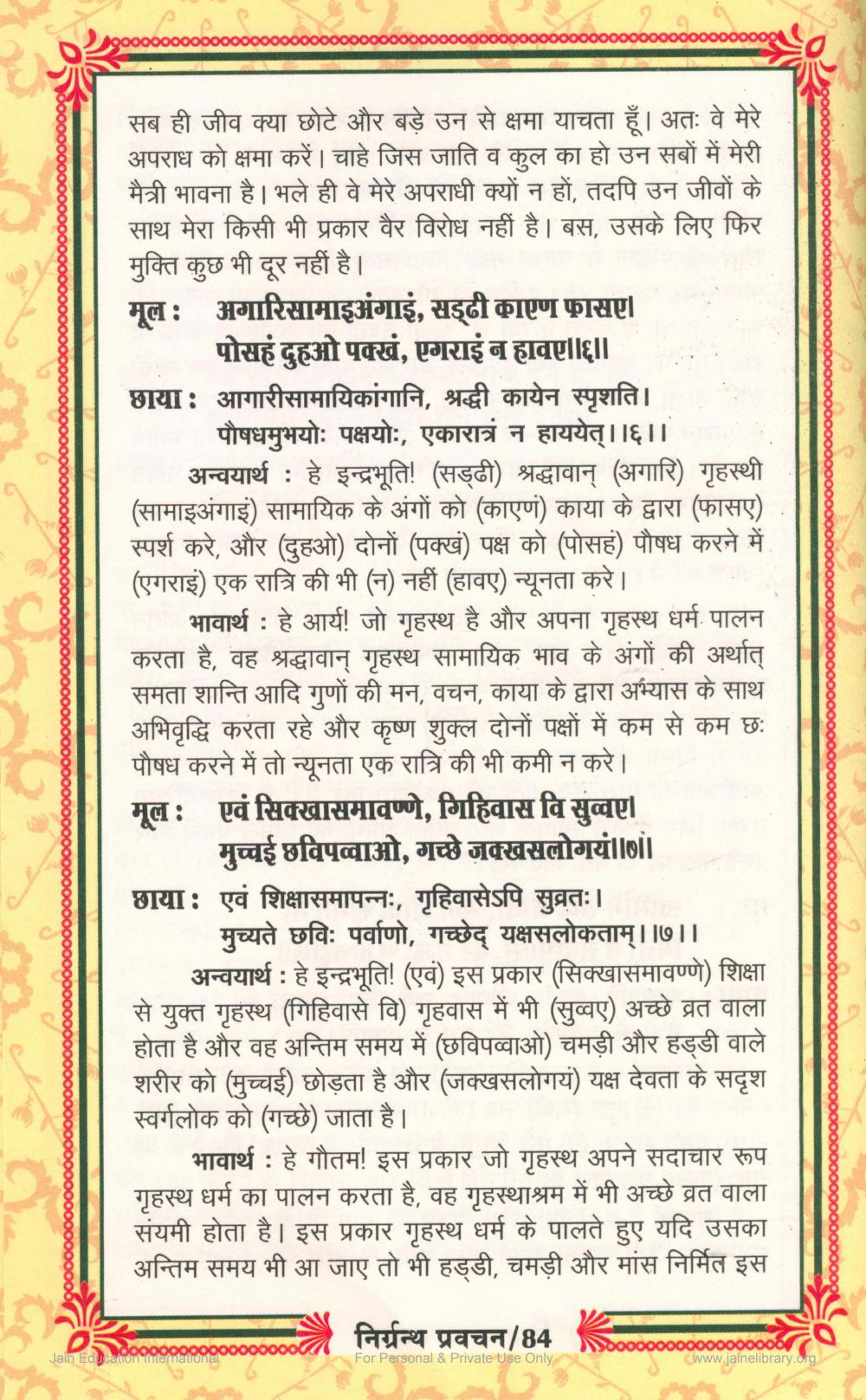________________ 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000og oooooor 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 सब ही जीव क्या छोटे और बड़े उन से क्षमा याचता हूँ। अतः वे मेरे अपराध को क्षमा करें। चाहे जिस जाति व कुल का हो उन सबों में मेरी मैत्री भावना है। भले ही वे मेरे अपराधी क्यों न हों, तदपि उन जीवों के साथ मेरा किसी भी प्रकार वैर विरोध नहीं है। बस, उसके लिए फिर मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है। मूल: अगारिसामाइअंगाई, सड्ढी काएण फासए। पोसहं दुहओ पक्खं, एगराइं न हावए||६|| छाया: आगारीसामायिकांगानि, श्रद्धी कायेन स्पृशति। पौषधमुभयोः पक्षयोः, एकारात्रं न हाययेत्।।६।। अन्वयार्थ : हे इन्द्रभूति! (सड्ढी) श्रद्धावान् (अगारि) गृहस्थी (सामाइअंगाई) सामायिक के अंगों को (काएण) काया के द्वारा (फासए) स्पर्श करे, और (दुहओ) दोनों (पक्खं) पक्ष को (पोसह) पौषध करने में (एगराइं) एक रात्रि की भी (न) नहीं (हावए) न्यूनता करे। भावार्थ : हे आर्य! जो गृहस्थ है और अपना गृहस्थ धर्म पालन करता है, वह श्रद्धावान् गृहस्थ सामायिक भाव के अंगों की अर्थात् समता शान्ति आदि गुणों की मन, वचन, काया के द्वारा अभ्यास के साथ अभिवृद्धि करता रहे और कृष्ण शुक्ल दोनों पक्षों में कम से कम छ: पौषध करने में तो न्यूनता एक रात्रि की भी कमी न करे। मूल : एवं सिक्खासमावण्णे, गिहिवास वि सुब्बए। मुच्चई छविपवाओ, गच्छे जक्खसलोगय||७|| छायाः एवं शिक्षासमापन्नः, गृहिवासेऽपि सुव्रतः। मुच्यते छविः पर्वाणो, गच्छेद् यक्षसलोकताम्।।७।। अन्वयार्थ : हे इन्द्रभूति! (एवं) इस प्रकार (सिक्खासमावण्णे) शिक्षा से युक्त गृहस्थ (गिहिवासे वि) गृहवास में भी (सुव्वए) अच्छे व्रत वाला होता है और वह अन्तिम समय में (छविपव्वाओ) चमड़ी और हड्डी वाले शरीर को (मुच्चई) छोड़ता है और (जक्खसलोगय) यक्ष देवता के सदृश स्वर्गलोक को (गच्छे) जाता है। भावार्थ : हे गौतम! इस प्रकार जो गृहस्थ अपने सदाचार रूप गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वह गृहस्थाश्रम में भी अच्छे व्रत वाला संयमी होता है। इस प्रकार गृहस्थ धर्म के पालते हुए यदि उसका अन्तिम समय भी आ जाए तो भी हड्डी, चमड़ी और मांस निर्मित इस ago00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 4 निर्ग्रन्थ प्रवचन/84 00000000000000000 Jain Edalcon international For Personal & Private Use Only DO0000000000000 Cwww.jainelibrary.org.