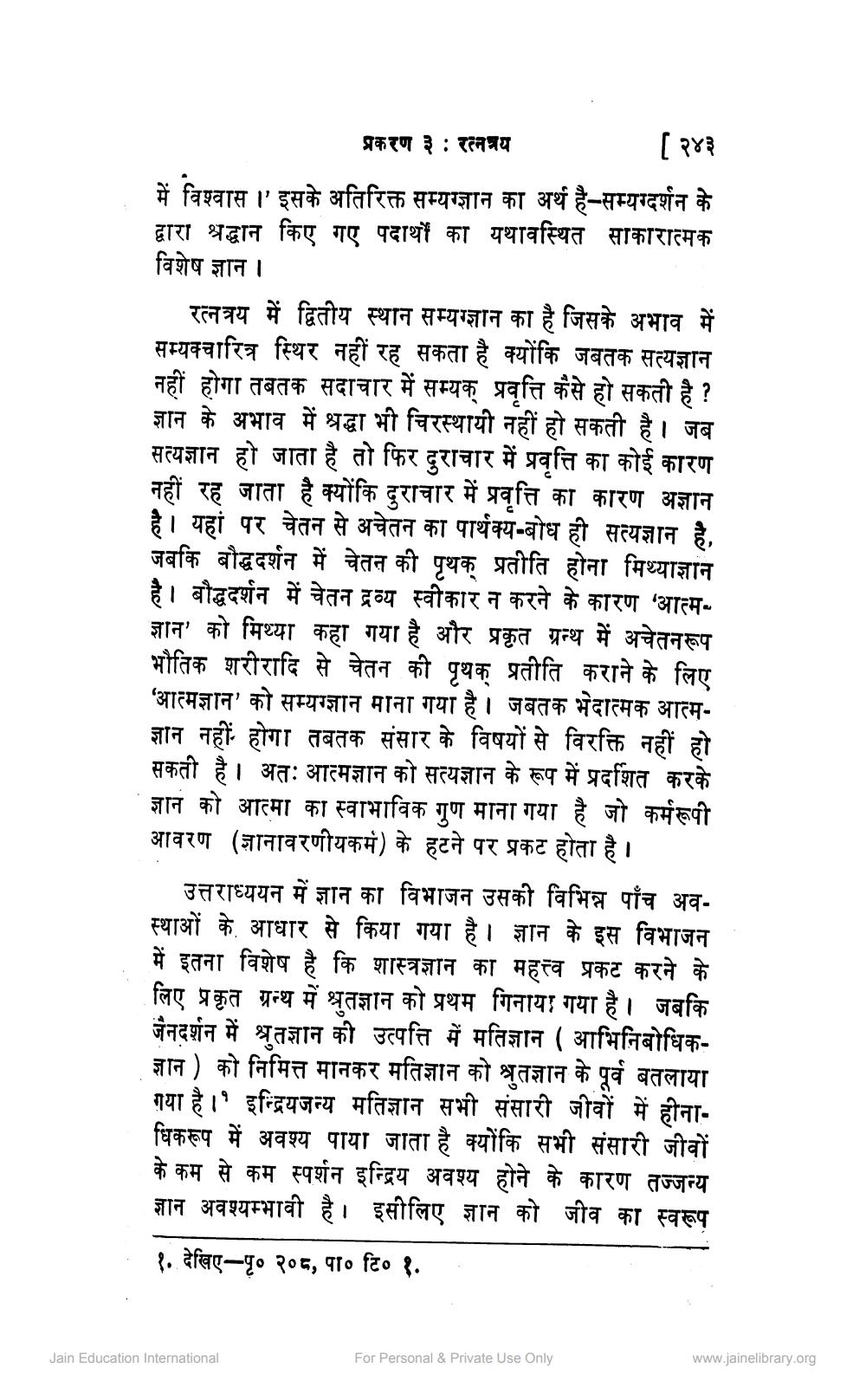________________
प्रकरण ३ : रत्नत्रय
[ २४३
में विश्वास ।' इसके अतिरिक्त सम्यग्ज्ञान का अर्थ है - सम्यग्दर्शन के द्वारा श्रद्धान किए गए पदार्थों का यथावस्थित साकारात्मक विशेष ज्ञान ।
रत्नत्रय में द्वितीय स्थान सम्यग्ज्ञान का है जिसके अभाव में सम्यक्चारित्र स्थिर नहीं रह सकता है क्योंकि जबतक सत्यज्ञान नहीं होगा तबतक सदाचार में सम्यक् प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? ज्ञान के अभाव में श्रद्धा भी चिरस्थायी नहीं हो सकती है । जब सत्यज्ञान हो जाता है तो फिर दुराचार में प्रवृत्ति का कोई कारण नहीं रह जाता है क्योंकि दुराचार में प्रवृत्ति का कारण अज्ञान है । यहां पर चेतन से अचेतन का पार्थक्य - बोध ही सत्यज्ञान है, जबकि बौद्धदर्शन में चेतन की पृथक् प्रतीति होना मिथ्याज्ञान है । बौद्धदर्शन में चेतन द्रव्य स्वीकार न करने के कारण 'आत्मज्ञान' को मिथ्या कहा गया है और प्रकृत ग्रन्थ में अचेतनरूप भौतिक शरीरादि से चेतन की पृथक् प्रतीति कराने के लिए 'आत्मज्ञान' को सम्यग्ज्ञान माना गया है । जबतक भेदात्मक आत्मज्ञान नहीं होगा तबतक संसार के विषयों से विरक्ति नहीं हो सकती है । अतः आत्मज्ञान को सत्यज्ञान के रूप में प्रदर्शित करके ज्ञान को आत्मा का स्वाभाविक गुण माना गया है जो कर्मरूपी आवरण (ज्ञानावरणीयकर्म) के हटने पर प्रकट होता है ।
उत्तराध्ययन में ज्ञान का विभाजन उसकी विभिन्न पाँच अवस्थाओं के आधार से किया गया है। ज्ञान के इस विभाजन में इतना विशेष है कि शास्त्रज्ञान का महत्त्व प्रकट करने के लिए प्रकृत ग्रन्थ में श्रुतज्ञान को प्रथम गिनाया गया है। जबकि जैनदर्शन में श्रुतज्ञान की उत्पत्ति में मतिज्ञान ( आभिनिबोधिकज्ञान ) को निमित्त मानकर मतिज्ञान को श्रुतज्ञान के पूर्व बतलाया गया है ।' इन्द्रियजन्य मतिज्ञान सभी संसारी जीवों में हीनाधिकरूप में अवश्य पाया जाता है क्योंकि सभी संसारी जीवों के कम से कम स्पर्शन इन्द्रिय अवश्य होने के कारण तज्जन्य ज्ञान अवश्यम्भावी है । इसीलिए ज्ञान को जीव का स्वरूप
१. देखिए - पृ० २०८, पा० टि० १.
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org