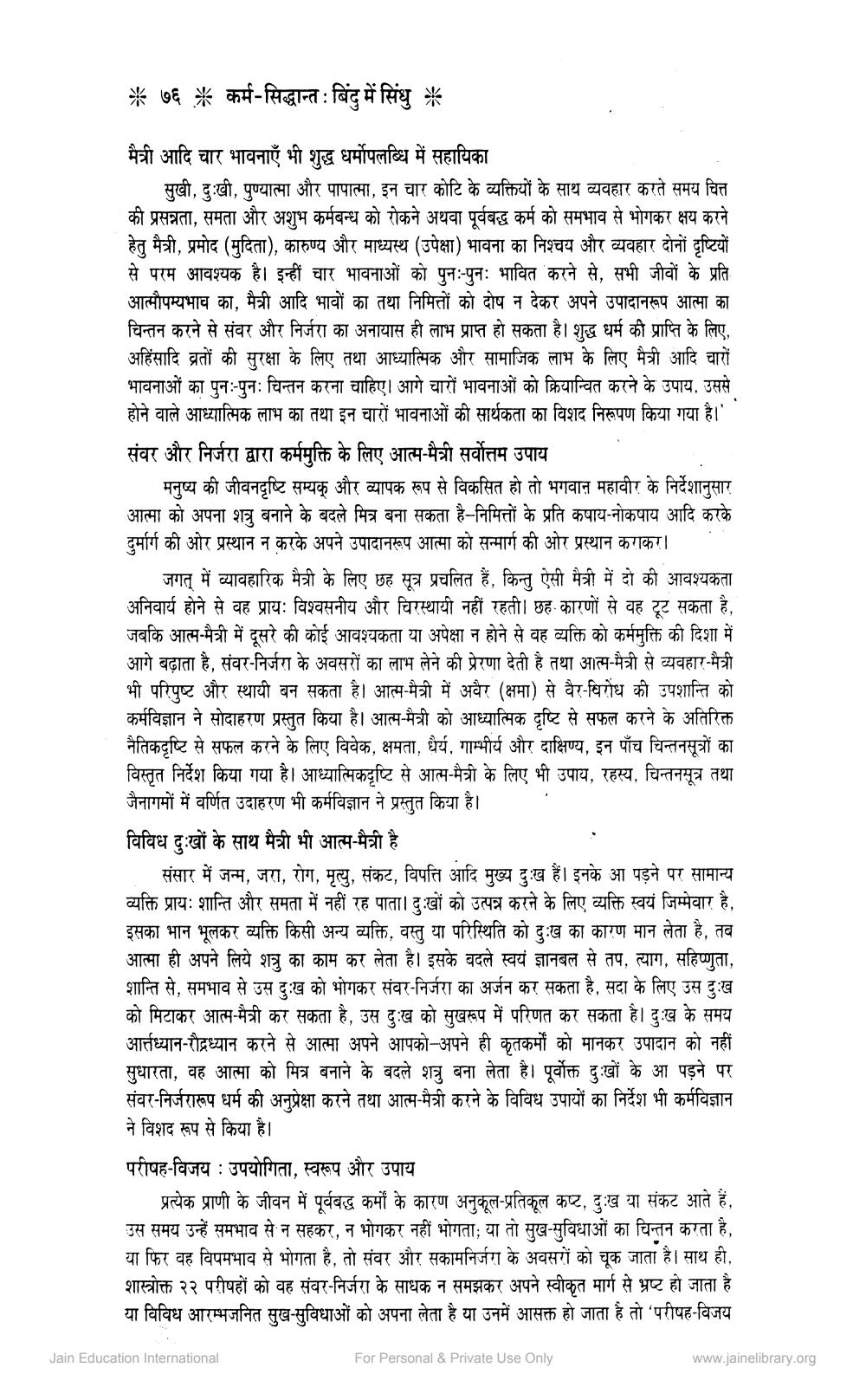________________
* ७६ * कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
मैत्री आदि चार भावनाएँ भी शुद्ध धर्मोपलब्धि में सहायिका
सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, इन चार कोटि के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय चित्त की प्रसन्नता, समता और अशुभ कर्मबन्ध को रोकने अथवा पूर्वबद्ध कर्म को समभाव से भोगकर क्षय करने हेतु मैत्री, प्रमोद (मुदिता), कारुण्य और माध्यस्थ (उपेक्षा) भावना का निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों से परम आवश्यक है। इन्हीं चार भावनाओं को पुनः-पुनः भावित करने से, सभी जीवों के प्रति आत्मौपम्यभाव का, मैत्री आदि भावों का तथा निमित्तों को दोष न देकर अपने उपादानरूप आत्मा का चिन्तन करने से संवर और निर्जरा का अनायास ही लाभ प्राप्त हो सकता है। शुद्ध धर्म की प्राप्ति के लिए, अहिंसादि व्रतों की सुरक्षा के लिए तथा आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ के लिए मैत्री आदि चारों भावनाओं का पुनः पुनः चिन्तन करना चाहिए। आगे चारों भावनाओं को क्रियान्वित करने के उपाय. उससे होने वाले आध्यात्मिक लाभ का तथा इन चारों भावनाओं की सार्थकता का विशद निरूपण किया गया है।' संवर और निर्जरा द्वारा कर्ममुक्ति के लिए आत्म-मैत्री सर्वोत्तम उपाय
मनुष्य की जीवनदृष्टि सम्यक् और व्यापक रूप से विकसित हो तो भगवान महावीर के निर्देशानुसार आत्मा को अपना शत्रु बनाने के बदले मित्र बना सकता है-निमित्तों के प्रति कषाय-नोकषाय आदि करके दुर्मार्ग की ओर प्रस्थान न करके अपने उपादानरूप आत्मा को सन्मार्ग की ओर प्रस्थान कराकर।
जगत् में व्यावहारिक मैत्री के लिए छह सूत्र प्रचलित हैं, किन्तु ऐसी मैत्री में दो की आवश्यकता अनिवार्य होने से वह प्रायः विश्वसनीय और चिरस्थायी नहीं रहती। छह कारणों से वह टूट सकता है, जबकि आत्म-मैत्री में दूसरे की कोई आवश्यकता या अपेक्षा न होने से वह व्यक्ति को कर्ममुक्ति की दिशा में आगे बढ़ाता है, संवर-निर्जरा के अवसरों का लाभ लेने की प्रेरणा देती है तथा आत्म-मैत्री से व्यवहार-मैत्री भी परिपुष्ट और स्थायी बन सकता है। आत्म-मैत्री में अवैर (क्षमा) से वैर-विरोध की उपशान्ति को कर्मविज्ञान ने सोदाहरण प्रस्तुत किया है। आत्म-मैत्री को आध्यात्मिक दृष्टि से सफल करने के अतिरिक्त नैतिकदृष्टि से सफल करने के लिए विवेक, क्षमता, धैर्य, गाम्भीर्य और दाक्षिण्य, इन पाँच चिन्तनसूत्रों का विस्तृत निर्देश किया गया है। आध्यात्मिकदृष्टि से आत्म-मैत्री के लिए भी उपाय, रहस्य, चिन्तनसूत्र तथा
जैनागमों में वर्णित उदाहरण भी कर्मविज्ञान ने प्रस्तुत किया है। विविध दुःखों के साथ मैत्री भी आत्म-मैत्री है
संसार में जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, संकट, विपत्ति आदि मुख्य दुःख हैं। इनके आ पड़ने पर सामान्य व्यक्ति प्रायः शान्ति और समता में नहीं रह पाता। दुःखों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है, इसका भान भूलकर व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को दुःख का कारण मान लेता है, तब आत्मा ही अपने लिये शत्रु का काम कर लेता है। इसके बदले स्वयं ज्ञानबल से तप, त्याग, सहिष्णुता, शान्ति से, समभाव से उस दुःख को भोगकर संवर-निर्जरा का अर्जन कर सकता है, सदा के लिए उस दुःख को मिटाकर आत्म-मैत्री कर सकता है, उस दुःख को सुखरूप में परिणत कर सकता है। दुःख के समय आर्तध्यान-रौद्रध्यान करने से आत्मा अपने आपको अपने ही कृतकर्मों को मानकर उपादान को नहीं सुधारता, वह आत्मा को मित्र बनाने के बदले शत्रु बना लेता है। पूर्वोक्त दुःखों के आ पड़ने पर संवर-निर्जरारूप धर्म की अनुप्रेक्षा करने तथा आत्म-मैत्री करने के विविध उपायों का निर्देश भी कर्मविज्ञान ने विशद रूप से किया है। परीषह-विजय : उपयोगिता, स्वरूप और उपाय
प्रत्येक प्राणी के जीवन में पूर्वबद्ध कर्मों के कारण अनुकूल-प्रतिकूल कष्ट, दुःख या संकट आते हैं, उस समय उन्हें समभाव से न सहकर, न भोगकर नहीं भोगता; या तो सुख-सुविधाओं का चिन्तन करता है, या फिर वह विपमभाव से भोगता है, तो संवर और सकामनिर्जरा के अवसरों को चूक जाता है। साथ ही, शास्त्रोक्त २२ परीषहों को वह संवर-निर्जरा के साधक न समझकर अपने स्वीकृत मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है या विविध आरम्भजनित सुख-सुविधाओं को अपना लेता है या उनमें आसक्त हो जाता है तो ‘परीषह-विजय
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org