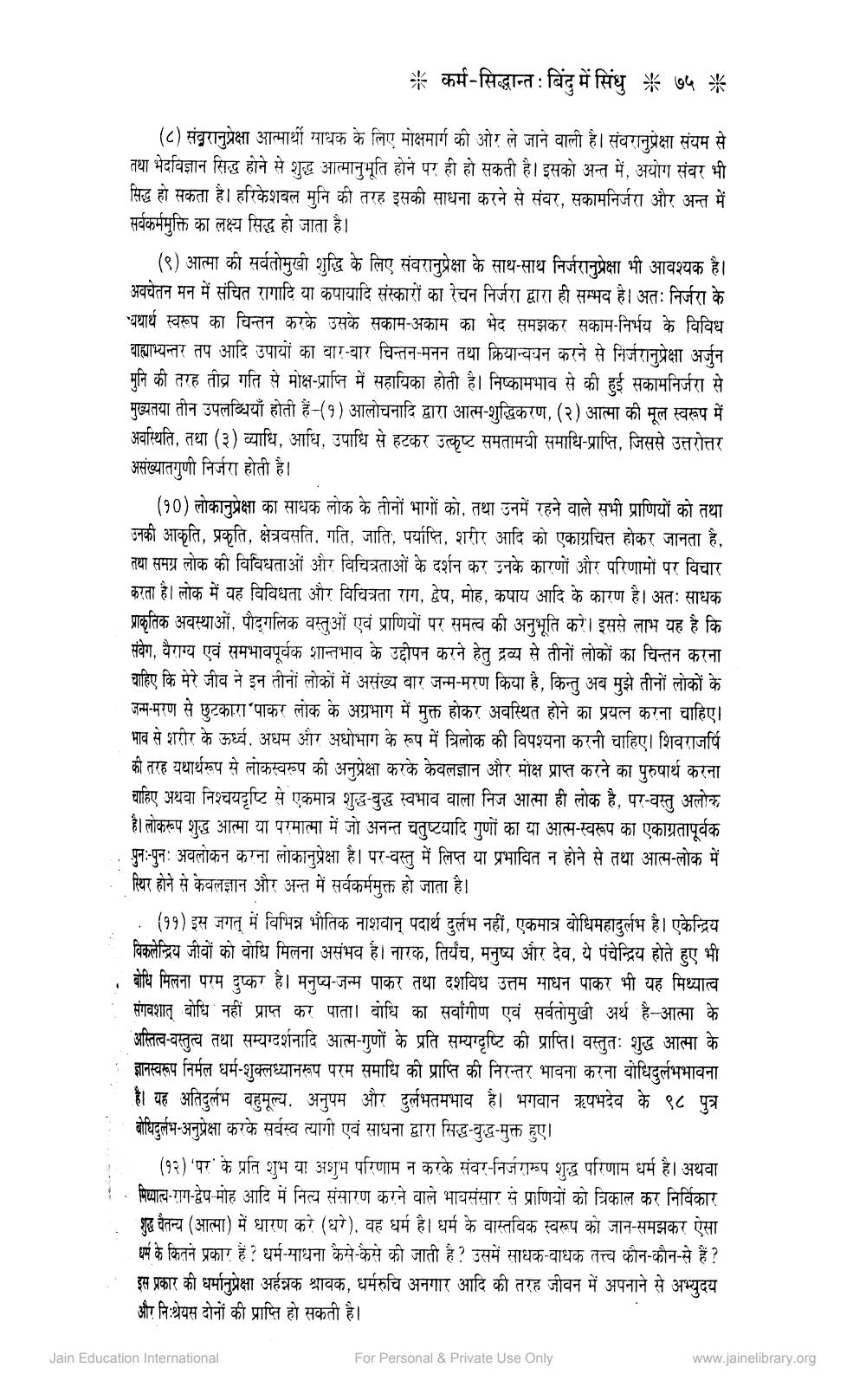________________
* कर्म - सिद्धान्त: बिंदु में सिंधु * ७५ *
(८) संवरानुप्रेक्षा आत्मार्थी साधक के लिए मोक्षमार्ग की ओर ले जाने वाली है। संवरानुप्रेक्षा संयम से तथा भेदविज्ञान सिद्ध होने से शुद्ध आत्मानुभूति होने पर ही हो सकती है। इसको अन्त में, अयोग संवर भी सिद्ध हो सकता है। हरिकेशबल मुनि की तरह इसकी साधना करने से संवर, सकामनिर्जरा और अन्त में सर्वकर्ममुक्ति का लक्ष्य सिद्ध हो जाता है।
(९) आत्मा की सर्वतोमुखी शुद्धि के लिए संवरानुप्रेक्षा के साथ-साथ निर्जरानुप्रेक्षा भी आवश्यक है। अवचेतन मन में संचित रागादि या कपायादि संस्कारों का रेचन निर्जरा द्वारा ही सम्भव है। अतः निर्जरा के यथार्थ स्वरूप का चिन्तन करके उसके सकाम अकाम का भेद समझकर सकाम-निर्भय के विविध बाह्याभ्यन्तर तप आदि उपायों का बार-बार चिन्तन-मनन तथा क्रियान्वयन करने से निर्जरानुप्रेक्षा अर्जुन मुनि की तरह तीव्र गति से मोक्ष प्राप्ति में सहायिका होती है। निष्कामभाव से की हुई सकामनिर्जरा से मुख्यतया तीन उपलब्धियाँ होती हैं - ( १ ) आलोचनादि द्वारा आत्म-शुद्धिकरण, (२) आत्मा की मूल स्वरूप में अवस्थिति, तथा (३) व्याधि, आधि, उपाधि से हटकर उत्कृष्ट समतामयी समाधि- प्राप्ति, जिससे उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है।
(१०) लोकानुप्रेक्षा का साधक लोक के तीनों भागों को, तथा उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को तथा उनकी आकृति, प्रकृति, क्षेत्रवसति, गति, जाति, पर्याप्ति, शरीर आदि को एकाग्रचित्त होकर जानता है, तथा समग्र लोक की विविधताओं और विचित्रताओं के दर्शन कर उनके कारणों और परिणामों पर विचार करता है। लोक में यह विविधता और विचित्रता राग, द्वेष, मोह, कषाय आदि के कारण है। अतः साधक प्राकृतिक अवस्थाओं, पौद्गलिक वस्तुओं एवं प्राणियों पर समत्व की अनुभूति करे। इससे लाभ यह है कि संवेग, वैराग्य एवं समभावपूर्वक शान्तभाव के उद्दीपन करने हेतु द्रव्य से तीनों लोकों का चिन्तन करना चाहिए कि मेरे जीव ने इन तीनों लोकों में असंख्य बार जन्म-मरण किया है, किन्तु अब मुझे तीनों लोकों के जन्म-मरण से छुटकारा पाकर लोक के अग्रभाग में मुक्त होकर अवस्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए। भाव से शरीर के ऊर्ध्व, अधम और अधोभाग के रूप में त्रिलोक की विपश्यना करनी चाहिए। शिवराजर्षि की तरह यथार्थरूप से लोकस्वरूप की अनुप्रेक्षा करके केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए अथवा निश्चयदृष्टि से एकमात्र शुद्ध-बुद्ध स्वभाव वाला निज आत्मा ही लोक है, पर वस्तु अलोक है। लोकरूप शुद्ध आत्मा या परमात्मा में जो अनन्त चतुष्टयादि गुणों का या आत्म-स्वरूप का एकाग्रतापूर्वक पुनः-पुनः अवलोकन करना लोकानुप्रेक्षा है। पर वस्तु में लिप्त या प्रभावित न होने से तथा आत्म-लोक में स्थिर होने से केवलज्ञान और अन्त में सर्वकर्ममुक्त हो जाता है ।
(११) इस जगत् में विभिन्न भौतिक नाशवान् पदार्थ दुर्लभ नहीं, एकमात्र बोधिमहादुर्लभ है। एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय जीवों को वोधि मिलना असंभव है। नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये पंचेन्द्रिय होते हुए भी बोधि मिलना परम दुष्कर है। मनुष्य जन्म पाकर तथा दशविध उत्तम साधन पाकर भी यह मिथ्यात्व संगवशात् बोधि नहीं प्राप्त कर पाता । बोधि का सर्वांगीण एवं सर्वतोमुखी अर्थ है - आत्मा के अस्तित्व-वस्तुत्व तथा सम्यग्दर्शनादि आत्म- गुणों के प्रति सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति । वस्तुतः शुद्ध आत्मा के ज्ञानस्वरूप निर्मल धर्म-शुक्लध्यानरूप परम समाधि की प्राप्ति की निरन्तर भावना करना बोधिदुर्लभभावना
। यह अतिदुर्लभ बहुमूल्य अनुपम और दुर्लभतमभाव है। भगवान ऋषभदेव के ९८ पुत्र बोधिदुर्लभ-अनुप्रेक्षा करके सर्वस्व त्यागी एवं साधना द्वारा सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए।
(१२) 'पर' के प्रति शुभ या अशुभ परिणाम न करके संवर-निर्जरारूप शुद्ध परिणाम धर्म है। अथवा मिथ्यात्व - राग-द्वेष-मोह आदि में नित्य संसारण करने वाले भावसंसार से प्राणियों को त्रिकाल कर निर्विकार शुद्ध चैतन्य (आत्मा) में धारण करे ( धरे). वह धर्म है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को जान-समझकर ऐसा धर्म के कितने प्रकार हैं ? धर्म-साधना कैसे-कैसे की जाती है? उसमें साधक-बाधक तत्त्व कौन-कौन-से हैं ? इस प्रकार की धर्मानुप्रेक्षा अर्हनक श्रावक, धर्मरुचि अनगार आदि की तरह जीवन में अपनाने से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति हो सकती है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org