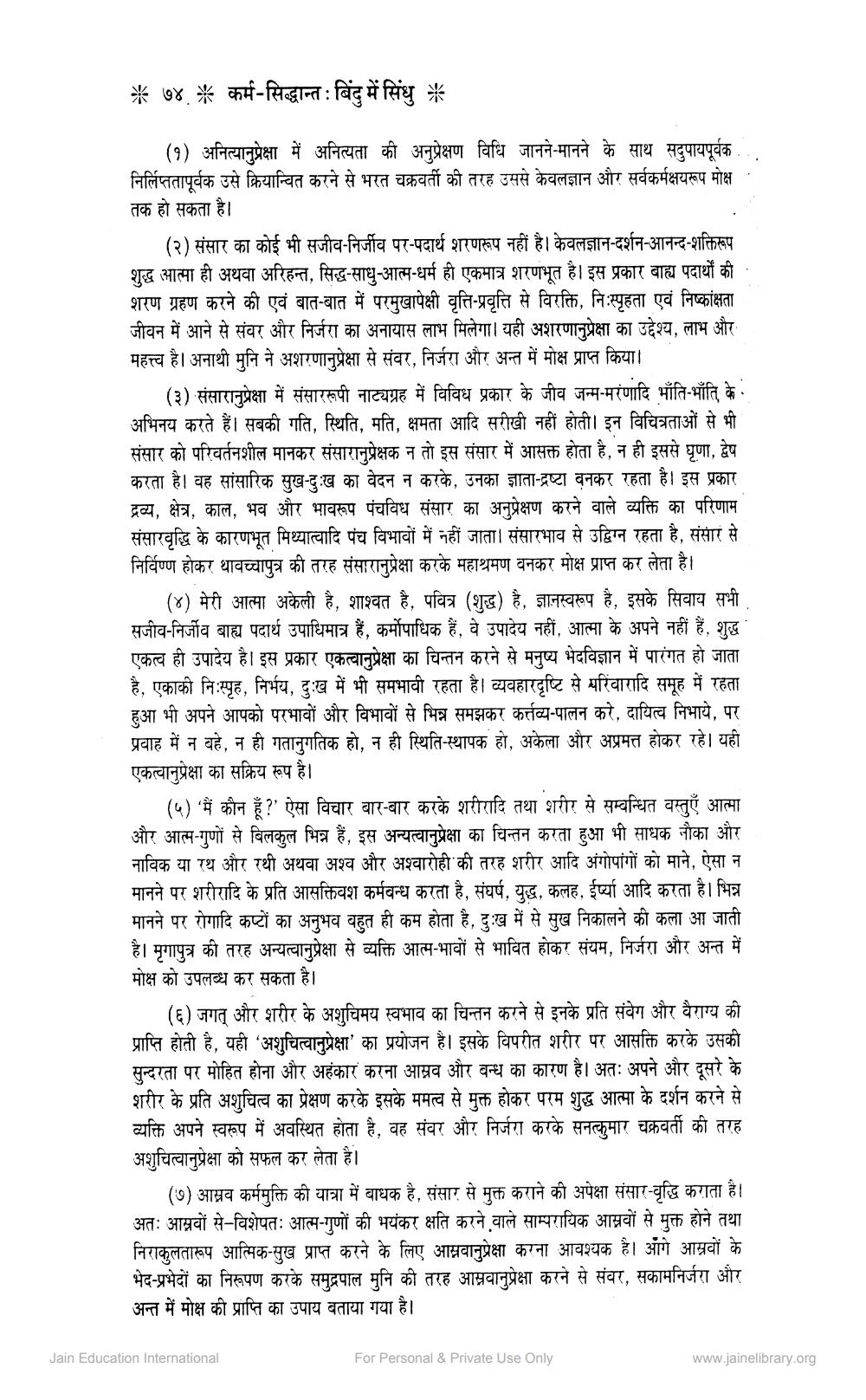________________
* ७४ * कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
(१) अनित्यानुप्रेक्षा में अनित्यता की अनुप्रेक्षण विधि जानने-मानने के साथ सदुपायपूर्वक ... निर्लिप्ततापूर्वक उसे क्रियान्वित करने से भरत चक्रवर्ती की तरह उससे केवलज्ञान और सर्वकर्मक्षयरूप मोक्ष . तक हो सकता है।
(२) संसार का कोई भी सजीव-निर्जीव पर-पदार्थ शरणरूप नहीं है। केवलज्ञान-दर्शन-आनन्द-शक्तिरूप शुद्ध आत्मा ही अथवा अरिहन्त, सिद्ध-साधु-आत्म-धर्म ही एकमात्र शरणभूत है। इस प्रकार बाह्य पदार्थों की शरण ग्रहण करने की एवं बात-बात में परमुखापेक्षी वृत्ति-प्रवृत्ति से विरक्ति, निःस्पृहता एवं निष्कांक्षता जीवन में आने से संवर और निर्जरा का अनायास लाभ मिलेगा। यही अशरणानुप्रेक्षा का उद्देश्य, लाभ और महत्त्व है। अनाथी मुनि ने अशरणानुप्रेक्षा से संवर, निर्जरा और अन्त में मोक्ष प्राप्त किया।
(३) संसारानुप्रेक्षा में संसाररूपी नाट्यग्रह में विविध प्रकार के जीव जन्म-मरणादि भाँति-भाँति के अभिनय करते हैं। सबकी गति, स्थिति, मति, क्षमता आदि सरीखी नहीं होती। इन विचित्रताओं से भी संसार को परिवर्तनशील मानकर संसारानुप्रेक्षक न तो इस संसार में आसक्त होता है, न ही इससे घृणा, द्वेष करता है। वह सांसारिक सुख-दुःख का वेदन न करके, उनका ज्ञाता-द्रष्टा वनकर रहता है। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप पंचविध संसार का अनुप्रेक्षण करने वाले व्यक्ति का परिणाम संसारवृद्धि के कारणभूत मिथ्यात्वादि पंच विभावों में नहीं जाता। संसारभाव से उद्विग्न रहता है, संसार से निर्विण्ण होकर थावच्चापुत्र की तरह संसारानुप्रेक्षा करके महाश्रमण वनकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
(४) मेरी आत्मा अकेली है, शाश्वत है, पवित्र (शुद्ध) है, ज्ञानस्वरूप है, इसके सिवाय सभी सजीव-निर्जीव बाह्य पदार्थ उपाधिमात्र हैं, कर्मोपाधिक हैं, वे उपादेय नहीं, आत्मा के अपने नहीं हैं, शुद्ध एकत्व ही उपादेय है। इस प्रकार एकत्वानुप्रेक्षा का चिन्तन करने से मनुष्य भेदविज्ञान में पारंगत हो जाता है, एकाकी निःस्पृह, निर्भय, दुःख में भी समभावी रहता है। व्यवहारदृष्टि से परिवारादि समूह में रहता हआ भी अपने आपको परभावों और विभावों से भिन्न समझकर कर्तव्य-पालन करे. दायित्व निभाये. पर प्रवाह में न बहे. न ही गतानगतिक हो. न ही स्थिति-स्थापक हो. अकेला और अप्रमत्त होकर रहे। यही एकत्वानुप्रेक्षा का सक्रिय रूप है।
(५) 'मैं कौन हूँ ?' ऐसा विचार बार-बार करके शरीरादि तथा शरीर से सम्बन्धित वस्तुएँ आत्मा और आत्म-गुणों से बिलकुल भिन्न हैं, इस अन्यत्वानुप्रेक्षा का चिन्तन करता हुआ भी साधक नौका और नाविक या रथ और रथी अथवा अश्व और अश्वारोही की तरह शरीर आदि अंगोपांगों को माने, ऐसा न मानने पर शरीरादि के प्रति आसक्तिवश कर्मबन्ध करता है, संघर्ष, युद्ध, कलह, ईर्ष्या आदि करता है। भिन्न मानने पर रोगादि कष्टों का अनुभव बहुत ही कम होता है, दुःख में से सुख निकालने की कला आ जाती है। मृगापुत्र की तरह अन्यत्वानुप्रेक्षा से व्यक्ति आत्म-भावों से भावित होकर संयम, निर्जरा और अन्त में मोक्ष को उपलब्ध कर सकता है।
(६) जगत् और शरीर के अशुचिमय स्वभाव का चिन्तन करने से इनके प्रति संवेग और वैराग्य की प्राप्ति होती है, यही 'अशुचित्वानुप्रेक्षा' का प्रयोजन है। इसके विपरीत शरीर पर आसक्ति करके उसकी सुन्दरता पर मोहित होना और अहंकार करना आस्रव और बन्ध का कारण है। अतः अपने और दूसरे के शरीर के प्रति अशुचित्व का प्रेक्षण करके इसके ममत्व से मुक्त होकर परम शुद्ध आत्मा के दर्शन करने से व्यक्ति अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, वह संवर और निर्जरा करके सनत्कुमार चक्रवर्ती की तरह अशुचित्वानुप्रेक्षा को सफल कर लेता है।
(७) आम्रव कर्ममुक्ति की यात्रा में बाधक है, संसार से मुक्त कराने की अपेक्षा संसार-वृद्धि कराता है। अतः आनवों से-विशेषतः आत्म-गुणों की भयंकर क्षति करने वाले साम्परायिक आम्रवों से मुक्त होने तथा निराकुलतारूप आत्मिक-सुख प्राप्त करने के लिए आनवानुप्रेक्षा करना आवश्यक है। आंगे आम्रवों के भेद-प्रभेदों का निरूपण करके समुद्रपाल मुनि की तरह आसवानुप्रेक्षा करने से संवर, सकामनिर्जरा और अन्त में मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया गया है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org