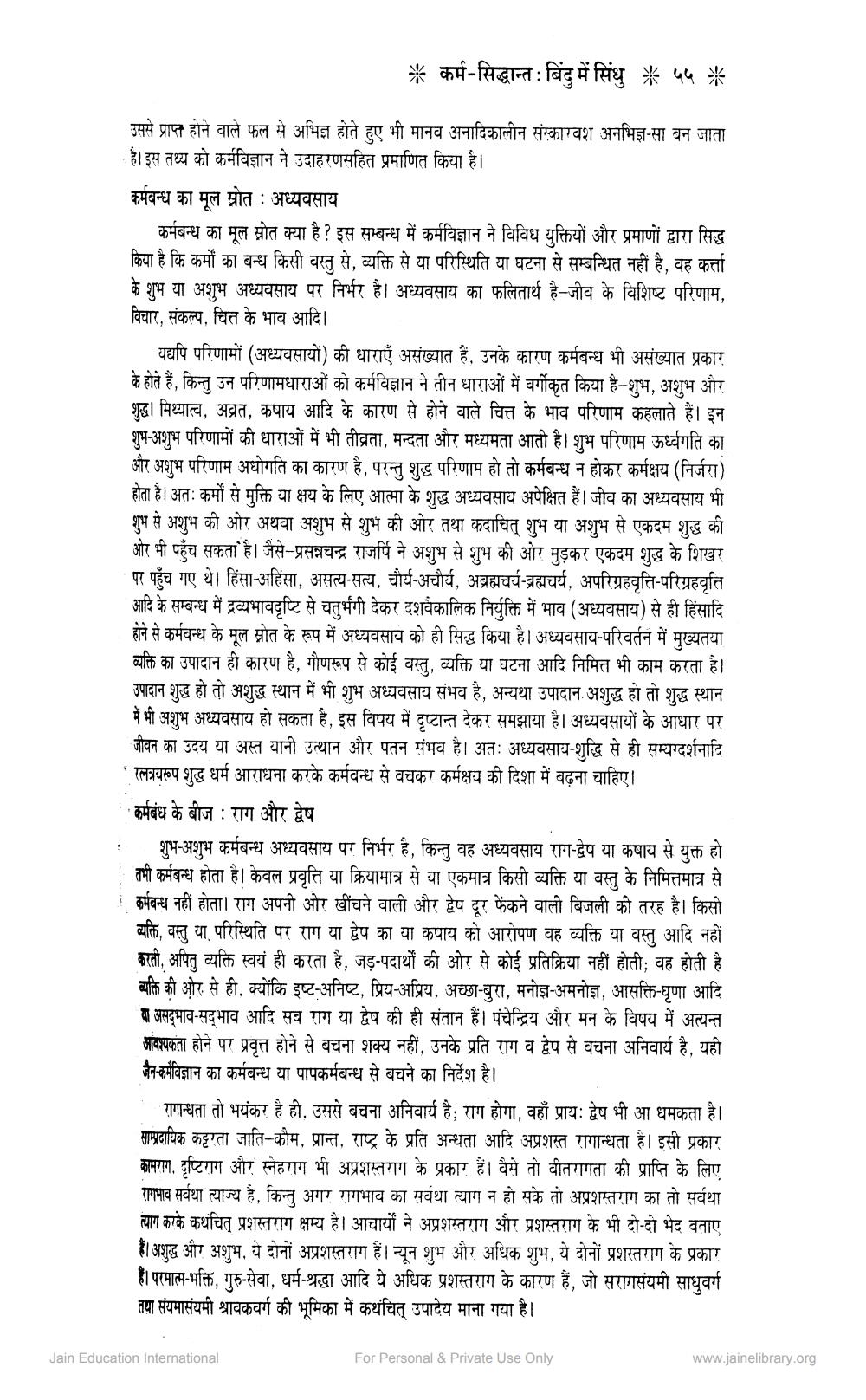________________
* कर्म - सिद्धान्त: बिंदु में सिंधु * ५५ *
उससे प्राप्त होने वाले फल से अभिज्ञ होते हुए भी मानव अनादिकालीन संस्कारवश अनभिज्ञ-सा बन जाता है । इस तथ्य को कर्मविज्ञान ने उदाहरणसहित प्रमाणित किया है।
कर्मबन्ध का मूल स्रोत : अध्यवसाय
कर्मबन्ध का मूल स्रोत क्या है ? इस सम्बन्ध में कर्मविज्ञान ने विविध युक्तियों और प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया है कि कर्मों का बन्ध किसी वस्तु से, व्यक्ति से या परिस्थिति या घटना से सम्बन्धित नहीं है, वह कर्ता के शुभ या अशुभ अध्यवसाय पर निर्भर है। अध्यवसाय का फलितार्थ है - जीव के विशिष्ट परिणाम, विचार, संकल्प, चित्त के भाव आदि ।
यद्यपि परिणामों (अध्यवसायों) की धाराएँ असंख्यात हैं, उनके कारण कर्मबन्ध भी असंख्यात प्रकार के होते हैं, किन्तु उन परिणामधाराओं को कर्मविज्ञान ने तीन धाराओं में वर्गीकृत किया है - शुभ, अशुभ और शुद्ध । मिथ्यात्व अव्रत, कषाय आदि के कारण से होने वाले चित्त के भाव परिणाम कहलाते हैं। इन शुभ-अशुभ परिणामों की धाराओं में भी तीव्रता, मन्दता और मध्यमता आती है। शुभ परिणाम ऊर्ध्वगति का और • अशुभ परिणाम अधोगति का कारण है, परन्तु शुद्ध परिणाम हो तो कर्मबन्ध न होकर कर्मक्षय (निर्जरा) होता है। अतः कर्मों से मुक्ति या क्षय के लिए आत्मा के शुद्ध अध्यवसाय अपेक्षित हैं। जीव का अध्यवसाय भी शुभ से अशुभ की ओर अथवा अशुभ से शुभ की ओर तथा कदाचित् शुभ या अशुभ से एकदम शुद्ध की ओर भी पहुँच सकता है। जैसे-प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ने अशुभ से शुभ की ओर मुड़कर एकदम शुद्ध के शिखर पर पहुँच गए थे। हिंसा-अहिंसा, असत्य- सत्य, चौर्य-अचौर्य, अब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवृत्ति-परिग्रहवृत्ति आदि के सम्बन्ध में द्रव्यभावदृष्टि से चतुर्भगी देकर दशवैकालिक नियुक्ति में भाव (अध्यवसाय ) से ही हिंसादि होने से कर्मबन्ध के मूल स्रोत के रूप में अध्यवसाय को ही सिद्ध किया है। अध्यवसाय- परिवर्तन में मुख्यतया व्यक्ति का उपादान ही कारण है, गौणरूप से कोई वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि निमित्त भी काम करता है । उपादान शुद्ध हो तो अशुद्ध स्थान में भी शुभ अध्यवसाय संभव है, अन्यथा उपादान अशुद्ध हो तो शुद्ध स्थान में भी अशुभ अध्यवसाय हो सकता है, इस विषय में दृष्टान्त देकर समझाया है। अध्यवसायों के आधार पर जीवन का उदय या अस्त यानी उत्थान और पतन संभव है। अतः अध्यवसाय-शुद्धि से ही सम्यग्दर्शनादि • रत्नत्रयरूप शुद्ध धर्म आराधना करके कर्मबन्ध से बचकर कर्मक्षय की दिशा में बढ़ना चाहिए।
• कर्मबंध के बीज : राग और द्वेष
शुभ-अशुभ कर्मबन्ध अध्यवसाय पर निर्भर है, किन्तु वह अध्यवसाय राग-द्वेप या कषाय से युक्त हो तभी कर्मबन्ध होता है। केवल प्रवृत्ति या क्रियामात्र से या एकमात्र किसी व्यक्ति या वस्तु के निमित्तमात्र से कर्मबन्ध नहीं होता। राग अपनी ओर खींचने वाली और द्वेप दूर फेंकने वाली बिजली की तरह है । किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर राग या द्वेष का या कपाय को आरोपण वह व्यक्ति या वस्तु आदि नहीं करती, अपितु व्यक्ति स्वयं ही करता है, जड़ पदार्थों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती; वह होती है। व्यक्ति की ओर से ही, क्योंकि इष्ट-अनिष्ट, प्रिय-अप्रिय, अच्छा-बुरा, मनोज्ञ-अमनोज्ञ, आसक्ति घृणा आदि या असद्भाव सद्भाव आदि सब राग या द्वेष की ही संतान हैं। पंचेन्द्रिय और मन के विषय में अत्यन्त आवश्यकता होने पर प्रवृत्त होने से बचना शक्य नहीं, उनके प्रति राग व द्वेष से बचना अनिवार्य है, यही जैन-कर्मविज्ञान का कर्मबन्ध या पापकर्मबन्ध से बचने का निर्देश है।
रागान्धता तो भयंकर है ही उससे बचना अनिवार्य है; राग होगा, वहाँ प्रायः द्वेष भी आ धमकता है। साम्प्रदायिक कट्टरता जाति-कौम, प्रान्त, राष्ट्र के प्रति अन्धता आदि अप्रशस्त रागान्धता है। इसी प्रकार कामराग, दृष्टिराग और स्नेहराग भी अप्रशस्तराग के प्रकार हैं। वैसे तो वीतरागता की प्राप्ति के लिए रागभाव सर्वथा त्याज्य है, किन्तु अगर रागभाव का सर्वथा त्याग न हो सके तो अप्रशस्त राग का तो सर्वथा त्याग करके कथंचित् प्रशस्तराग क्षम्य है। आचार्यों ने अप्रशस्तराग और प्रशस्तराग के भी दो-दो भेद बताए हैं। अशुद्ध और अशुभ, ये दोनों अप्रशस्तराग हैं। न्यून शुभ और अधिक शुभ, ये दोनों प्रशस्तराग के प्रकार हैं। परमात्म-भक्ति, गुरु-सेवा, धर्म-श्रद्धा आदि ये अधिक प्रशस्तराग के कारण हैं, जो सरागसंयमी साधुवर्ग तथा संयमासंयमी श्रावकवर्ग की भूमिका में कथंचित् उपादेय माना गया है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org