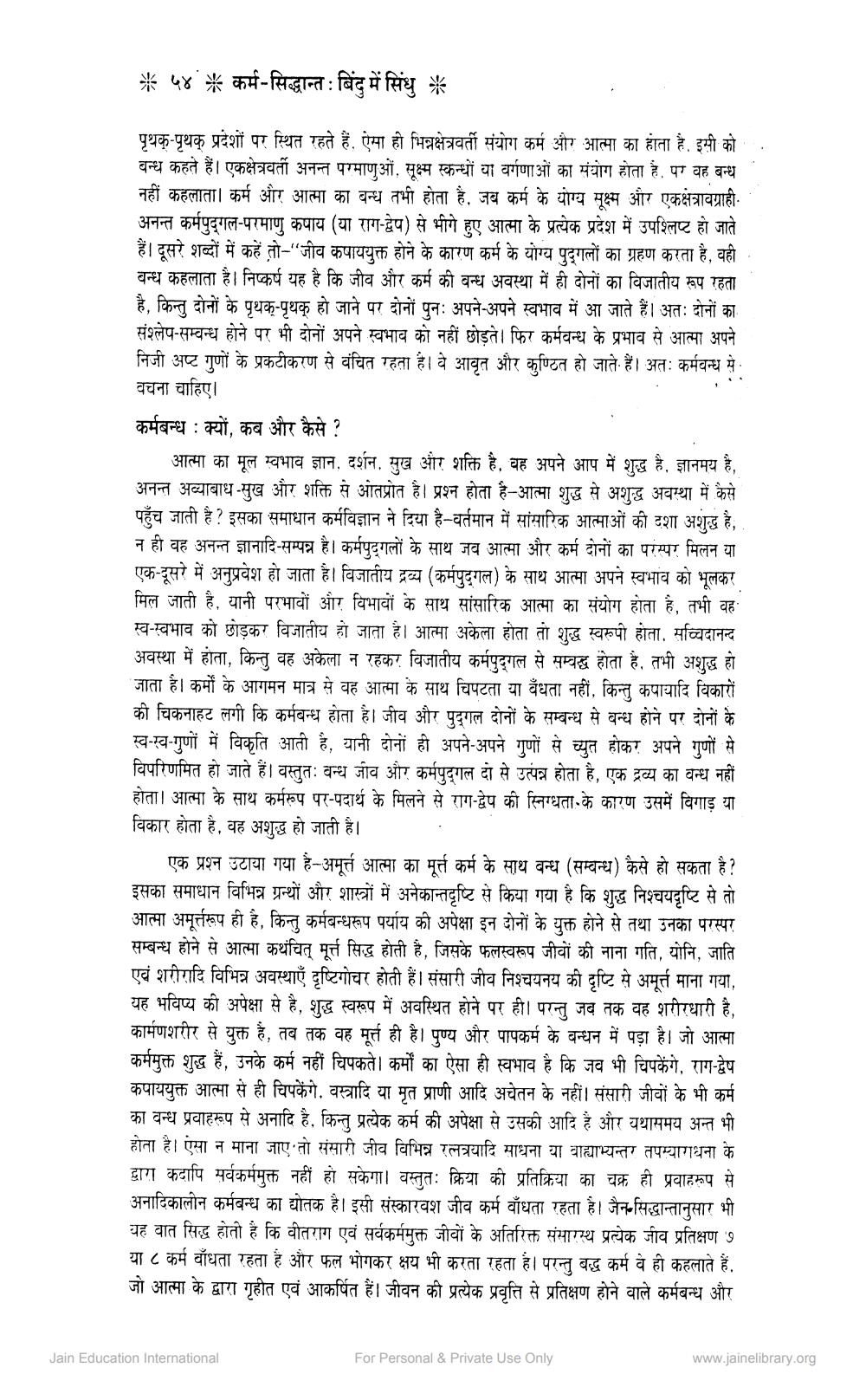________________
* ५४ * कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
पृथक्-पृथक् प्रदेशों पर स्थित रहते हैं. ऐसा ही भिन्नक्षेत्रवर्ती संयोग कर्म और आत्मा का होता है. इसी को बन्ध कहते हैं। एकक्षेत्रवर्ती अनन्त परमाणुओं, सूक्ष्म स्कन्धों या वर्गणाओं का संयोग होता है. पर वह बन्ध नहीं कहलाता। कर्म और आत्मा का बन्ध तभी होता है. जब कर्म के योग्य सूक्ष्म और एकक्षेत्रावग्राही. अनन्त कर्मपुद्गल-परमाणु कषाय (या राग-द्वेष) से भीगे हुए आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में उपश्लिष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो-“जीव कषाययुक्त होने के कारण कर्म के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करता है, वही बन्ध कहलाता है। निष्कर्ष यह है कि जीव और कर्म की बन्ध अवस्था में ही दोनों का विजातीय रूप रहता है, किन्तु दोनों के पृथक्-पृथक् हो जाने पर दोनों पुनः अपने-अपने स्वभाव में आ जाते हैं। अतः दोनों का संश्लेप-सम्बन्ध होने पर भी दोनों अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। फिर कर्मवन्ध के प्रभाव से आत्मा अपने निजी अप्ट गुणों के प्रकटीकरण से वंचित रहता है। वे आवृत और कुण्ठित हो जाते हैं। अतः कर्मबन्ध से वचना चाहिए। कर्मबन्ध : क्यों, कब और कैसे ?
आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति है. वह अपने आप में शुद्ध है, ज्ञानमय है, अनन्त अव्याबाध-सुख और शक्ति से ओतप्रोत है। प्रश्न होता है-आत्मा शुद्ध से अशुद्ध अवस्था में कैसे पहुँच जाती है ? इसका समाधान कर्मविज्ञान ने दिया है-वर्तमान में सांसारिक आत्माओं की दशा अशुद्ध है, न ही वह अनन्त ज्ञानादि-सम्पन्न है। कर्मपदगलों के साथ जब आत्मा और कर्म दोनों का परस्पर मिलन या एक-दूसरे में अनुप्रवेश हो जाता है। विजातीय द्रव्य (कर्मपुद्गल) के साथ आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर मिल जाती है, यानी परभावों और विभावों के साथ सांसारिक आत्मा का संयोग होता है, तभी वह स्व-स्वभाव को छोड़कर विजातीय हो जाता है। आत्मा अकेला होता तो शुद्ध स्वरूपी होता. सच्चिदानन्द अवस्था में होता, किन्तु वह अकेला न रहकर विजातीय कर्मपुद्गल से सम्बद्ध होता है, तभी अशुद्ध हो जाता है। कर्मों के आगमन मात्र से वह आत्मा के साथ चिपटता या वधता नहीं, किन्तु कपायादि विकारों की चिकनाहट लगी कि कर्मबन्ध होता है। जीव और पुद्गल दोनों के सम्बन्ध से बन्ध होने पर दोनों के स्व-स्व-गुणों में विकृति आती है, यानी दोनों ही अपने-अपने गुणों से च्युत होकर अपने गुणों से विपरिणमित हो जाते हैं। वस्तुतः बन्ध जीव और कर्मपुद्गल दो से उत्पन्न होता है, एक द्रव्य का बन्ध नहीं होता। आत्मा के साथ कर्मरूप पर-पदार्थ के मिलने से राग-द्वेप की स्निग्धता के कारण उसमें विगाड़ या विकार होता है, वह अशुद्ध हो जाती है।
एक प्रश्न उठाया गया है-अमूर्त आत्मा का मूर्त कर्म के साथ वन्ध (सम्वन्ध) कैसे हो सकता है ? इसका समाधान विभिन्न ग्रन्थों और शास्त्रों में अनेकान्तदृष्टि से किया गया है कि शुद्ध निश्चयदृष्टि से तो आत्मा अमूर्तरूप ही है, किन्तु कर्मबन्धरूप पर्याय की अपेक्षा इन दोनों के युक्त होने से तथा उनका परस्पर सम्बन्ध होने से आत्मा कथंचित् मूर्त सिद्ध होती है, जिसके फलस्वरूप जीवों की नाना गति, योनि, जाति एवं शरीरादि विभिन्न अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। संसारी जीव निश्चयनय की दृष्टि से अमूर्त माना गया, यह भविष्य की अपेक्षा से है, शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होने पर ही। परन्तु जब तक वह शरीरधारी है, कार्मणशरीर से युक्त है, तब तक वह मूर्त ही है। पुण्य और पापकर्म के बन्धन में पड़ा है। जो आत्मा कर्ममुक्त शुद्ध हैं, उनके कर्म नहीं चिपकते। कर्मों का ऐसा ही स्वभाव है कि जब भी चिपकेंगे, राग-द्वेष कपाययुक्त आत्मा से ही चिपकेंगे. वस्त्रादि या मृत प्राणी आदि अचेतन के नहीं। संसारी जीवों के भी कर्म का वन्ध प्रवाहरूप से अनादि है, किन्तु प्रत्येक कर्म की अपेक्षा से उसकी आदि है और यथासमय अन्त भी होता है। ऐसा न माना जाए तो संसारी जीव विभिन्न रलत्रयादि साधना या बाह्याभ्यन्तर तपम्यागधना के द्वारा कदापि सर्वकर्ममुक्त नहीं हो सकेगा। वस्तुतः क्रिया की प्रतिक्रिया का चक्र ही प्रवाहरूप से अनादिकालीन कर्मबन्ध का द्योतक है। इसी संस्कारवश जीव कर्म वाँधता रहता है। जैन सिद्धान्तानुसार भी यह वात सिद्ध होती है कि वीतराग एवं सर्वकर्ममुक्त जीवों के अतिरिक्त संसारस्थ प्रत्येक जीव प्रतिक्षण ७ या ८ कर्म बाँधता रहता है और फल भोगकर क्षय भी करता रहता है। परन्तु बद्ध कर्म वे ही कहलाते हैं. जो आत्मा के द्वारा गृहीत एवं आकर्षित हैं। जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति से प्रतिक्षण होने वाले कर्मबन्ध और
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org