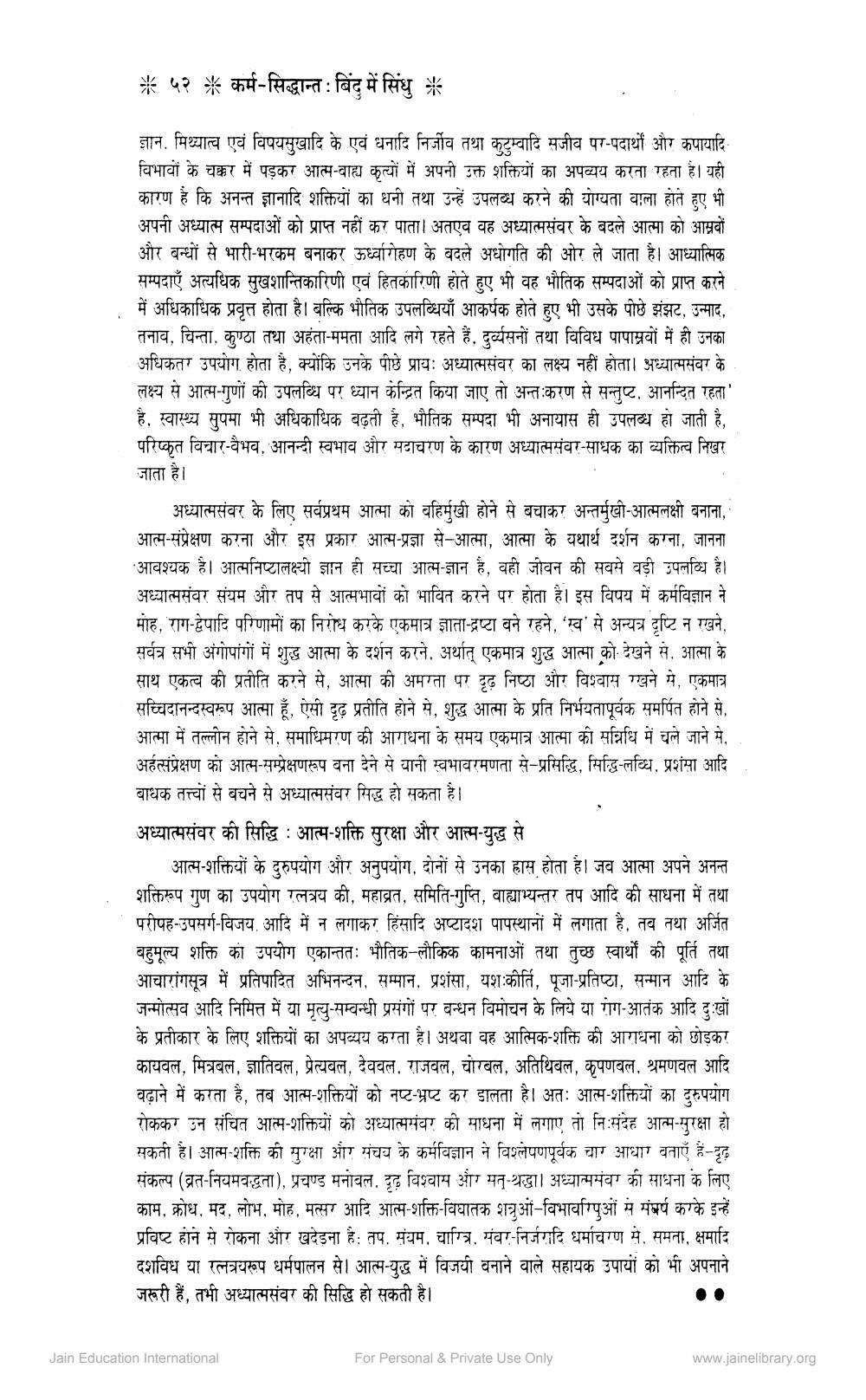________________
* ५२ * कर्म - सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
ज्ञान. मिथ्यात्व एवं विषयसुखादि के एवं धनादि निर्जीव तथा कुटुम्बादि सजीव पर पदार्थों और कपायादिविभावों के चक्कर में पड़कर आत्म- बाह्य कृत्यों में अपनी उक्त शक्तियों का अपव्यय करता रहता है। यही कारण है कि अनन्त ज्ञानादि शक्तियों का धनी तथा उन्हें उपलब्ध करने की योग्यता वाला होते हुए भी अपनी अध्यात्म सम्पदाओं को प्राप्त नहीं कर पाता । अतएव वह अध्यात्मसंवर के बदले आत्मा को आम्रवों और बन्धों से भारी-भरकम बनाकर ऊर्ध्वारोिहण के बदले अधोगति की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक सम्पदाएँ अत्यधिक सुखशान्तिकारिणी एवं हितकारिणी होते हुए भी वह भौतिक सम्पदाओं को प्राप्त करने में अधिकाधिक प्रवृत्त होता है। बल्कि भौतिक उपलब्धियाँ आकर्षक होते हुए भी उसके पीछे झंझट, उन्माद, तनाव, चिन्ता, कुण्ठा तथा अहंता-ममता आदि लगे रहते हैं, दुर्व्यसनों तथा विविध पापाम्रवों में ही उनका अधिकतर उपयोग होता है, क्योंकि उनके पीछे प्रायः अध्यात्मसंवर का लक्ष्य नहीं होता। अध्यात्मसंवर के लक्ष्य से आत्म-गुणों की उपलब्धि पर ध्यान केन्द्रित किया जाए तो अन्तःकरण से सन्तुष्ट, आनन्दित रहता' है, स्वास्थ्य सुपमा भी अधिकाधिक बढ़ती है, भौतिक सम्पदा भी अनायास ही उपलब्ध हो जाती है, परिष्कृत विचार-वैभव, आनन्दी स्वभाव और सदाचरण के कारण अध्यात्मसंवर-साधक का व्यक्तित्व निखर जाता है।
अध्यात्मसंवर के लिए सर्वप्रथम आत्मा को बहिर्मुखी होने से बचाकर अन्तर्मुखी - आत्मलक्षी बनाना, आत्म-संप्रेक्षण करना और इस प्रकार आत्म-प्रज्ञा से - आत्मा, आत्मा के यथार्थ दर्शन करना, जानना 'आवश्यक है। आत्मनिष्टालक्ष्यी ज्ञान ही सच्चा आत्म-ज्ञान है, वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अध्यात्मसंवर संयम और तप से आत्मभावों को भावित करने पर होता है। इस विषय में कर्मविज्ञान ने मोह, राग-द्वेपादि परिणामों का निरोध करके एकमात्र ज्ञाता - द्रष्टा बने रहने, 'स्व' से अन्यत्र दृष्टि न रखने, सर्वत्र सभी अंगोपांगों में शुद्ध आत्मा के दर्शन करने अर्थात् एकमात्र शुद्ध आत्मा को देखने से आत्मा के साथ एकत्व की प्रतीति करने से, आत्मा की अमरता पर दृढ़ निष्ठा और विश्वास रखने से, एकमात्र सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मा हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति होने से, शुद्ध आत्मा के प्रति निर्भयतापूर्वक समर्पित होने से, आत्मा में तल्लीन होने से, समाधिमरण की आराधना के समय एकमात्र आत्मा की सन्निधि में चले जाने से, अर्हत्संप्रेक्षण को आत्म-सम्प्रेक्षणरूप बना देने से यानी स्वभावरमणता से प्रसिद्धि, सिद्धि-लब्धि प्रशंसा आदि बाधक तत्त्वों से बचने से अध्यात्मसंवर सिद्ध हो सकता है।
अध्यात्मसंवर की सिद्धि : आत्म-शक्ति सुरक्षा और आत्म-युद्ध
से
आत्म-शक्तियों के दुरुपयोग और अनुपयोग, दोनों से उनका हास होता है। जब आत्मा अपने अनन्त शक्तिरूप गुण का उपयोग रत्नत्रय की, महाव्रत, समिति गुप्ति, बाह्याभ्यन्तर तप आदि की साधना में तथा परीपह-उपसर्ग-विजय आदि में न लगाकर हिंसादि अष्टादश पापस्थानों में लगाता है, तब तथा अर्जित बहुमूल्य शक्ति का उपयोग एकान्ततः भौतिक - लौकिक कामनाओं तथा तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति तथा आचारांगसूत्र में प्रतिपादित अभिनन्दन, सम्मान, प्रशंसा, यशःकीर्ति, पूजा-प्रतिष्ठा, सन्मान आदि के जन्मोत्सव आदि निमित्त में या मृत्यु-सम्बन्धी प्रसंगों पर बन्धन विमोचन के लिये या रोग आतंक आदि दुःखों के प्रतीकार के लिए शक्तियों का अपव्यय करता है। अथवा वह आत्मिक-शक्ति की आराधना को छोड़कर कायवल, मित्रबल, ज्ञातिवल, प्रेत्यबल, देववल, राजबल, चोरबल, अतिथिबल, कृपणबल, श्रमणवल आदि बढ़ाने में करता है, तब आत्म-शक्तियों को नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है। अतः आत्म-शक्तियों का दुरुपयोग रोककर उन संचित आत्म-शक्तियों को अध्यात्मसंबर की साधना में लगाए तो निःसंदेह आत्म-सुरक्षा हो सकती है। आत्म-शक्ति की सुरक्षा और संचय के कर्मविज्ञान ने विश्लेपणपूर्वक चार आधार बताएँ हैं दृढ़ संकल्प (व्रत-नियमबद्धता), प्रचण्ड मनोबल, दृढ़ विश्वास और सत् श्रद्धा । अध्यात्मसंवर की साधना के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि आत्म-शक्ति-विघातक शत्रुओं-विभावरिपुओं से संघर्ष करके इन्हें प्रविष्ट होने से रोकना और खदेड़ना है: तप. संयम, चारित्र, संवर-निर्जरादि धर्माचरण से, समता, क्षमादि दशविध या रत्नत्रयरूप धर्मपालन से। आत्म- युद्ध में विजयी बनाने वाले सहायक उपायों को भी अपनाने जरूरी हैं, तभी अध्यात्मसंवर की सिद्धि हो सकती है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org