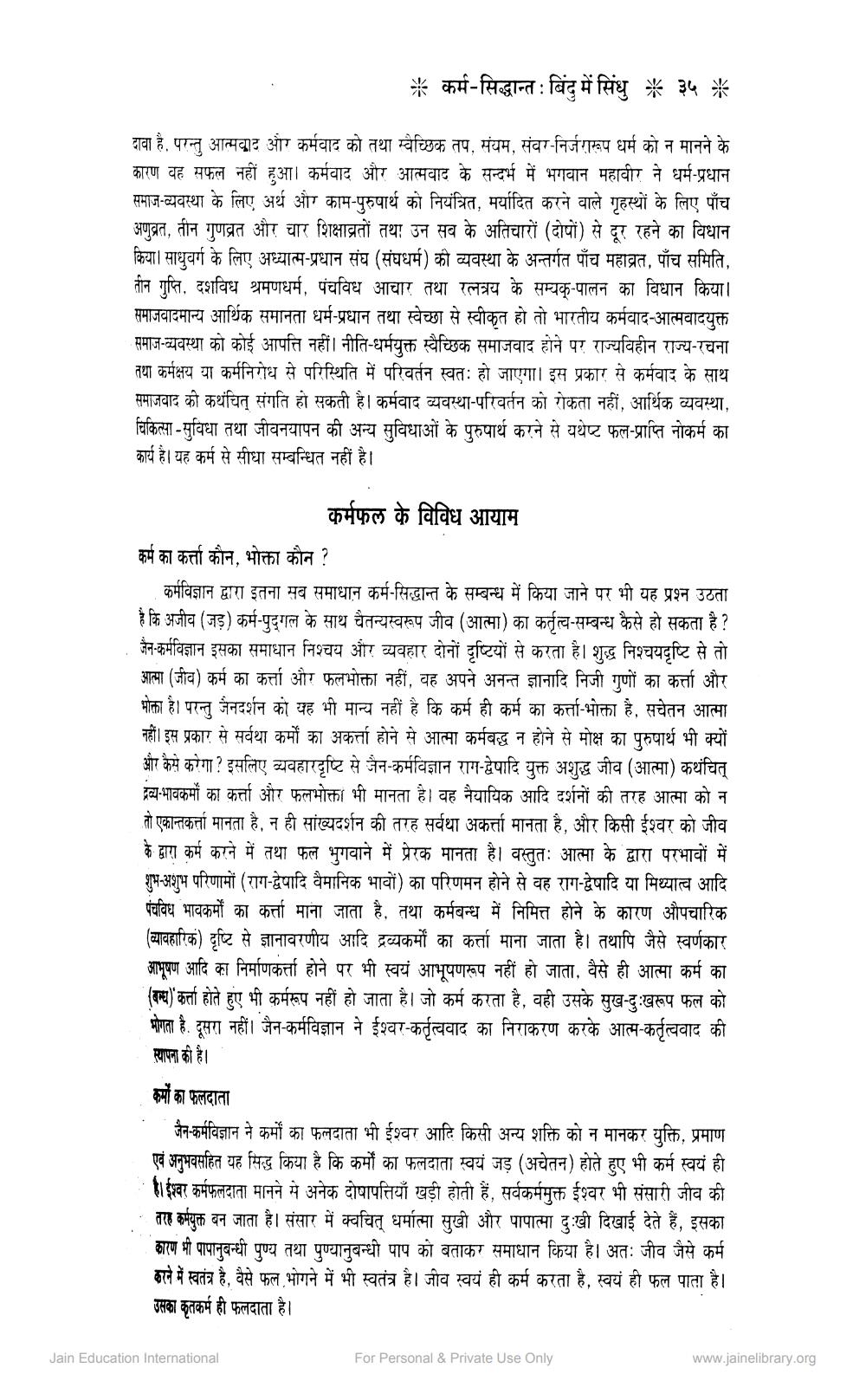________________
* कर्म - सिद्धान्त: बिंदु में सिंधु *३५ *
दावा है, परन्तु आत्मवाद और कर्मवाद को तथा स्वैच्छिक तप, संयम, संवर- निर्जरारूप धर्म को न मानने के कारण वह सफल नहीं हुआ। कर्मवाद और आत्मवाद के सन्दर्भ में भगवान महावीर ने धर्म-प्रधान समाज-व्यवस्था के लिए अर्थ और काम- पुरुषार्थ को नियंत्रित, मर्यादित करने वाले गृहस्थों के लिए पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतों तथा उन सब के अतिचारों (दोषों) से दूर रहने का विधा किया। साधुवर्ग के लिए अध्यात्म-प्रधान संघ (संघधर्म) की व्यवस्था के अन्तर्गत पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, दशविध श्रमणधर्म, पंचविध आचार तथा रत्नत्रय के सम्यक् पालन का विधान किया । समाजवादमान्य आर्थिक समानता धर्म-प्रधान तथा स्वेच्छा से स्वीकृत हो तो भारतीय कर्मवाद - आत्मवादयुक्त समाज-व्यवस्था को कोई आपत्ति नहीं। नीति-धर्मयुक्त स्वैच्छिक समाजवाद होने पर राज्यविहीन राज्य - रचना तथा कर्मक्षय या कर्मनिरोध से परिस्थिति में परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। इस प्रकार से कर्मवाद के साथ समाजवाद की कथंचित् संगति हो सकती है। कर्मवाद व्यवस्था परिवर्तन को रोकता नहीं, आर्थिक व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा तथा जीवनयापन की अन्य सुविधाओं के पुरुषार्थ करने से यथेष्ट फल प्राप्ति नोकर्म का कार्य है। यह कर्म से सीधा सम्बन्धित नहीं है ।
कर्मफल के विविध आयाम
कर्म का कर्त्ता कौन, भोक्ता कौन ?
कर्मविज्ञान द्वारा इतना सब समाधान कर्म सिद्धान्त के सम्बन्ध में किया जाने पर भी यह प्रश्न उठता है कि अजीव (जड़) कर्म-पुद्गल के साथ चैतन्यस्वरूप जीव (आत्मा) का कर्तृत्व-सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? जैन-कर्मविज्ञान इसका समाधान निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों से करता है। शुद्ध निश्चयदृष्टि से तो आत्मा (जीव ) कर्म का कर्त्ता और फलभोक्ता नहीं, वह अपने अनन्त ज्ञानादि निजी गुणों का कर्त्ता और भोक्ता है। परन्तु जैनदर्शन को यह भी मान्य नहीं है कि कर्म ही कर्म का कर्ता-भोक्ता है, सचेतन आत्मा नहीं। इस प्रकार से सर्वथा कर्मों का अकर्त्ता होने से आत्मा कर्मबद्ध न होने से मोक्ष का पुरुषार्थ भी क्यों और कैसे करेगा? इसलिए व्यवहारदृष्टि से जैन-कर्मविज्ञान राग-द्वेषादि युक्त अशुद्ध जीव (आत्मा) कथंचित् द्रव्य-भावकर्मों का कर्त्ता और फलभोक्ता भी मानता है। वह नैयायिक आदि दर्शनों की तरह आत्मा को न तो एकान्तकर्त्ता मानता है, न ही सांख्यदर्शन की तरह सर्वथा अकर्त्ता मानता है, और किसी ईश्वर को जीव के.
5 द्वारा कर्म करने में तथा फल भुगवाने में प्रेरक मानता है। वस्तुतः आत्मा के द्वारा परभावों में शुभ-अशुभ परिणामों (राग-द्वेषादि वैमानिक भावों) का परिणमन होने से वह राग-द्वेषादि या मिथ्यात्व आदि पंचविध भावकर्मों का कर्त्ता माना जाता है, तथा कर्मबन्ध में निमित्त होने के कारण औपचारिक ( व्यावहारिक) दृष्टि से ज्ञानावरणीय आदि द्रव्यकर्मों का कर्त्ता माना जाता है। तथापि जैसे स्वर्णकार आभूषण आदि का निर्माणकर्ता होने पर भी स्वयं आभूषणरूप नहीं हो जाता, वैसे ही आत्मा कर्म का (बन्ध) कर्ता होते हुए भी कर्मरूप नहीं हो जाता है। जो कर्म करता है, वही उसके सुख-दुःखरूप फल को भोगता है. दूसरा नहीं। जैन-कर्मविज्ञान ने ईश्वर-कर्तृत्ववाद का निराकरण करके आत्म-कर्तृत्ववाद की स्थापना की है।
कर्मों का फलदाता
जैन-कर्मविज्ञान ने कर्मों का फलदाता भी ईश्वर आदि किसी अन्य शक्ति को न मानकर युक्ति, प्रमाण एवं अनुभवसहित यह सिद्ध किया है कि कर्मों का फलदाता स्वयं जड़ (अचेतन) होते हुए भी कर्म स्वयं ही है। ईश्वर कर्मफलदाता मानने से अनेक दोषापत्तियाँ खड़ी होती हैं, सर्वकर्ममुक्त ईश्वर भी संसारी जीव की तरह कर्मयुक्त बन जाता है। संसार में क्वचित् धर्मात्मा सुखी और पापात्मा दुःखी दिखाई देते हैं, इसका कारण भी पापानुबन्धी पुण्य तथा पुण्यानुबन्धी पाप को बताकर समाधान किया है। अतः जीव जैसे कर्म करने में स्वतंत्र है, वैसे फल भोगने में भी स्वतंत्र है। जीव स्वयं ही कर्म करता है, स्वयं ही फल पाता है। उसका कृतकर्म ही फलदाता है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org